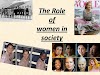डॉ. अंजना सिंह राजपूत (PhD)
जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
सारांश
भारत की सांस्कृतिक विविधता में जनजातियाँ एक अभिन्न अंग के
रूप में स्थापित हैं, जिनमें सहरिया
जनजाति का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत सरकार द्वारा 'विशेष रूप से दुर्लभ जनजातीय समूह' (PVTGs) के रूप में
चिन्हित सहरिया समुदाय मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और
राजस्थान के वन क्षेत्रों में निवास करता है। यह जनजाति पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों,
लोक-ज्ञान आधारित औषधीय प्रयोगों तथा वनस्पति-आधारित उपचारों के लिए जानी जाती है। पीढ़ियों से अर्जित इस ज्ञान का प्रयोग
वे न केवल स्वास्थ्य देखभाल में करते हैं, बल्कि यह उनके जीविकोपार्जन
का भी एक महत्त्वपूर्ण साधन है। तथापि, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, शिक्षा की कमी, और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता ने इस समुदाय को आज भी अंधविश्वास,
देवी-देवताओं पर निर्भरता, एवं घरेलू उपचारों तक सीमित कर रखा है। यह शोध सहरिया जनजाति की पारंपरिक औषधीय
संस्कृति का विश्लेषण करते हुए, उनके स्वास्थ्य व्यवहार,
सांस्कृतिक विश्वासों तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से दूरी के अंतःसंबंधों
को समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन इस पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता तथा
जनजातीय स्वास्थ्य में संस्कृति की भूमिका को उजागर करता है।
मुख्य शब्द: सहरिया जनजाति, परंपरागत औषधियाँ, घरेलू उपचार, धार्मिक निवारण
प्रस्तावना
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ललितपुर जनपद, एक ऐसा भू-भाग है जो एक ओर समृद्ध
सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किए हुए है, वहीं दूसरी ओर आज
भी सूखा, भुखमरी, जल संकट और कुपोषण
जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग परंपराओं, रीति-रिवाजों और लोकदेवताओं के प्रति गहरी आस्था रखता है। स्वास्थ्य,
शिक्षा और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में व्यापक अभाव यहाँ की
ग्राम्य संरचना में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, जिसके
कारण जनसमूह विकास की मुख्यधारा से कटकर आध्यात्मिक विश्वासों और अंधविश्वास की ओर
प्रवृत्त होता चला गया है।
यह स्थिति तब और अधिक जटिल हो जाती है जब हम अनुसूचित
जनजातियों, विशेषकर
सहरिया जनजाति की बात करते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य की स्थिति को सामान्यतः पोषण
स्तर, जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर,
शिशु मृत्यु दर, आत्महत्या, विकलांगता, नशीली पदार्थों की लत, किशोर अपराध एवं सामाजिक हिंसा जैसे मानकों के माध्यम से आँका जाता है।
इसके साथ ही शिक्षा का स्तर, आवास की गुणवत्ता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा पर्यावरणीय कारक भी स्वास्थ्य निर्धारण में
निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
सहरिया जनजाति, जो ललितपुर में निवास करने वाली एक प्रमुख आदिवासी आबादी है, अपने पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान और धार्मिक आस्थाओं के माध्यम से रोगों के
उपचार को परिभाषित करती है। यह समुदाय बीमारियों के कारणों को केवल जैविक न मानकर,
सामाजिक-धार्मिक और आध्यात्मिक कारकों से भी जोड़ता है। बीमारी की
स्थिति को अक्सर दैवी कोप, अथवा पूर्वजों की अप्रसन्नता से
जोड़कर देखा जाता है, और इसके समाधान हेतु झाड़-फूंक,
ताबीज, पशुबलि तथा अनुष्ठानों का सहारा लिया
जाता है।
सहरिया समुदाय की स्वास्थ्य संस्कृति में धार्मिक और
आध्यात्मिक धारणाएँ इतनी गहराई से अंतर्निहित हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ
इनके विश्वास तंत्र में समावेश नहीं पा सकीं। ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी समाज
में आज भी यह धारणा प्रचलित है कि रोग का मूल कारण किसी बुरी आत्मा अथवा दुष्ट
शक्ति द्वारा उत्पन्न होता है (मिश्रा एवं मांझी, 2004)। इस कारणवश, समुदाय के लोग आधुनिक
स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा करते हुए, धार्मिक एवं पारंपरिक
उपचारों को प्राथमिकता देते हैं।
ललितपुर की सहरिया जनजाति अन्य क्षेत्रों की सहरिया आबादी
से इस अर्थ में भिन्न है कि यह समुदाय उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित होकर आया है
और वर्ष 2003 तक इसे अनुसूचित जाति के
अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। 2003 के उपरांत ही इसे
अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने इनके
सामाजिक-आर्थिक संघर्षों को और जटिल बनाया है, जिसका सीधा
प्रभाव इनके स्वास्थ्य व्यवहार और जीवनशैली पर पड़ा है।
वनवासी जीवन शैली के कारण इस जनजाति ने प्रकृति के साथ
सहजीविता स्थापित करते हुए अनेक पारंपरिक औषधीय पद्धतियाँ विकसित की हैं, जिनमें से अनेक धार्मिक विश्वासों से
प्रेरित हैं। इनके उपचार पद्धति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है; निवारक (Preventive) और उपचारात्मक (Curative)। निवारक उपायों में तावीज, धार्मिक अनुष्ठान,
पशु बलि एवं पूर्वज पूजा शामिल हैं, जबकि
उपचारात्मक विधियों में वनस्पति आधारित औषधियों एवं लोकजड़ी-बूटियों का उपयोग होता
है।
सहरिया समुदाय की मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएँ परिवार
की समृद्धि, शारीरिक
स्वास्थ्य और मानसिक शांति की संरक्षक होती हैं। इस विश्वास के आधार पर वे शारीरिक
अस्वस्थता को भी आध्यात्मिक असंतुलन से जोड़ते हैं।
यह लेख ललितपुर जनपद में निवासरत सहरिया जनजाति के पारंपरिक
चिकित्सा ज्ञान, धार्मिक
विश्वासों और स्वास्थ्य संस्कृति का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। साथ ही यह भी
स्पष्ट करता है कि किस प्रकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, सामाजिक बहिष्करण और सांस्कृतिक धारणाएँ मिलकर इस समुदाय को वैज्ञानिक
चिकित्सा पद्धतियों से दूर रखती हैं। यह शोध इस बात पर बल देता है कि जनजातीय
स्वास्थ्य को समझने और सुधारने के लिए उनके सांस्कृतिक ढांचे, धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक ज्ञान को समावेशी दृष्टिकोण से समझा जाना
आवश्यक है।
धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक संरचना
सहरिया जनजाति, जो भारत के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है, एक
ऐसी पारंपरिक समुदाय है जिसके जीवन में धर्म न केवल एक आस्था है, बल्कि दैनिक जीवन की हर गतिविधि का अभिन्न अंग भी है। इस जनजाति का यह
दृढ़ विश्वास है कि धार्मिक अनुष्ठानों के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है,
और सम्पूर्ण ब्रह्मांड की रचना ईश्वर की इच्छा का प्रतिफल है।
सहरिया समुदाय में बेहरान, ठाकुर, भूमिज,
नाहरसिंह, और
घटोइया जैसे स्थानीय देवताओं की आराधना विभिन्न सामाजिक और चिकित्सकीय
प्रयोजनों हेतु की जाती है। ‘माता’ की अवधारणा इस समुदाय में विशेष महत्व रखती है:
सीतला देवी और शारदा माई जैसे
स्वरूपों में उनकी पूजा की जाती है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई
व्यक्ति चेचक से ग्रस्त होता है, तो समुदाय इसे ‘माता के
प्रकोप’ के रूप में देखता है और तदनुसार फल, मिठाई, एवं पकवान चढ़ाकर पूजा करता है।
धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में सहरिया जनजाति पारंपरिक
पुजारियों को प्राथमिकता देती है, किंतु समय-समय पर हिंदू ब्राह्मणों को भी बुलाया जाता है, यद्यपि जातीय भेदभाव के कारण कई बार वे आमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं। यह
समुदाय हिंदू पर्वों जैसे होली, दिवाली, दशहरा, और रक्षा बंधन को भी उत्साह से
मनाता है, हालांकि कई गांवों में उन्हें मंदिर प्रवेश से
वंचित रखा जाता है। फिर भी वे सामुदायिक स्तर पर सतही धार्मिक आयोजन में सहभागिता
करते हैं।
मौनी बाबा नृत्य, जो दिवाली के पश्चात श्रवण नक्षत्र में आयोजित होता है, इस जनजाति की सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का जीवंत उदाहरण है, जिसमें सहरिया समुदाय की भागीदारी विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है।
सहरिया जनजाति न केवल धार्मिक आस्थाओं को बीमारी और उपचार
से जोड़ती है, बल्कि
आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों की तुलना में पारंपरिक गुनिया, ओझा, भोपा, और देवज्ञों
पर अधिक भरोसा करती है। इन चिकित्सकों द्वारा झाड़-फूंक, ताबीज,
बलि, और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से रोग
निवारण किया जाता है।
सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से, यह समुदाय हाड़ौती बोली से प्रभावित
भाषा बोलता है। विवाह सामान्यतः 15 वर्ष की आयु के बाद
वर-वधू की आपसी सहमति से संपन्न होता है। गोत्र-व्यवस्था विवाह में निर्णायक होती
है, जिसमें सोहारा, गोरचिया,
दोतिया, चौहान, सेलिया,
और बख प्रमुख गोत्र हैं।
स्वास्थ्य संस्कृति: एक सैद्धांतिक और नृविज्ञान-आधारित
परिप्रेक्ष्य
स्वास्थ्य संस्कृति की अवधारणा को बनर्जी (1982) द्वारा चिकित्सा नृविज्ञान के क्षेत्र में प्रवर्तित किया
गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों की स्वास्थ्य संबंधी
अवधारणाओं, व्यवहारों और प्रतीकों को उनके सांस्कृतिक
सन्दर्भ में समझना है। इस अवधारणा के अनुसार, स्वास्थ्य और
बीमारी के अनुभवों को केवल जैविक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि
सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे में विश्लेषित करना अधिक उपयुक्त है।
मैरियट (1955) और कारस्टेयर्स (1955) जैसे विद्वानों के केस
स्टडीज़ यह इंगित करते हैं कि भारतीय समाज में स्वास्थ्य प्रथाओं को अक्सर 'अवैज्ञानिक' या 'अंधविश्वासी'
के रूप में देखा जाता है, जबकि वे समुदाय के
लिए गहन सांस्कृतिक अर्थ वहन करते हैं। हसन (1967), गोल्ड (1967),
खरे (1963) आदि ने यह रेखांकित किया है कि
आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को 'वैज्ञानिक' और जनजातीय स्वास्थ्य पद्धतियों को 'पिछड़ा' कहना एक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है, जो सांस्कृतिक
उपेक्षा को बढ़ावा देता है।
उड़ीसा के राउरकेला में उरांव जनजाति पर साहू (1991) द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ
कि स्वास्थ्य संस्थानों तक भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक
अवरोधों के कारण इन समुदायों की आवश्यकताएँ अधूरी रह जाती हैं। रेड्डी (2008)
का कार्य भी इस अवरोधात्मक संरचना की पुष्टि करता है।
सहरिया जनजाति की स्वास्थ्य अवधारणा में भी प्रमुख रूप से अलौकिक
कारणों का प्रभाव है। उनका विश्वास है कि रोग आत्माओं, भूत-प्रेत, या दैवी
प्रकोप के कारण होते हैं और इन्हें दूर करने हेतु झाड़-फूंक, ताबीज, देवता की आराधना, तथा पारंपरिक जड़ी-बूटियों का सहारा लिया जाता है। वे आधुनिक
चिकित्सालयों, दवाओं और डॉक्टरों
की अपेक्षा अपने पारंपरिक ज्ञान और धार्मिक चिकित्सकों पर अधिक विश्वास रखते हैं।
बेक (2020) के अनुसार, जनजातीय स्वास्थ्य प्रणाली में वैज्ञानिक
चिकित्सा के स्थान पर लोक आधारित, धार्मिक और सांस्कृतिक
उपचार विधियों का वर्चस्व है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली उनके विश्वासों और सामाजिक
ताने-बाने में सहजता से समाहित नहीं हो पाती।
पारंपरिक चिकित्सा: एक सांस्कृतिक-सामाजिक उपचार तंत्र
पारंपरिक या स्वदेशी चिकित्सा उन चिकित्सा प्रणालियों को
संदर्भित करती है, जो आधुनिक
जैव-चिकित्सा पद्धतियों के आगमन से पूर्व विभिन्न समाजों में विकसित हुईं और आज भी
जीवित हैं। ये पद्धतियाँ केवल औषधीय उपचार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे स्थानीय विश्वासों, सांस्कृतिक प्रतीकों,
और सामुदायिक अनुभवों से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। इनमें
आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, अफ्रीकी मुटी, योरूबा इफ़ा, और अन्य विश्व-प्रसिद्ध स्वदेशी
पद्धतियाँ सम्मिलित हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पारंपरिक चिकित्सा को एक ऐसी समग्र स्वास्थ्य प्रणाली के
रूप में परिभाषित करता है, जिसमें पौधों, खनिजों और पशु-आधारित औषधियों के साथ-साथ आध्यात्मिक उपचार, मैनुअल तकनीकें, और व्यायाम शामिल होते हैं, जिन्हें अकेले या संयुक्त रूप से निदान, उपचार,
और रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है (Beck, 2020)। यह पद्धति रोग की केवल जैविक व्याख्या ही नहीं देती, बल्कि उसके सामाजिक, आध्यात्मिक, और सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझने की चेष्टा करती है।
ललितपुर जिले की सहरिया जनजाति के संदर्भ में पारंपरिक
चिकित्सा पद्धति न केवल व्यवहारिक चिकित्सकीय प्रणाली है, बल्कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक विश्वासों की
भी अभिव्यक्ति है। यहाँ उपचार की प्रक्रिया अक्सर स्थानीय देवताओं की आराधना से
प्रारंभ होती है, और यह दर्शाता है कि चिकित्सा इनके लिए
केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है।
उदाहरणस्वरूप, अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न रोगों के निवारण
हेतु विशिष्ट देवताओं की पूजा की जाती है:
- भैंसासुर: पशुओं से संबंधित बीमारियों के निवारण
में विशेष रूप से पूजनीय।
- खांच के
बाबा: साँप
के काटने पर उपचार हेतु श्रद्धा का केंद्र।
- जमुनाया के
बाबाजू: बिच्छू
के विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए विख्यात।
- अताई के
बाबाजू: अग्नि-दग्ध
व्यक्ति के उपचार में सहायक माने जाते हैं।
- नट बाबाजू: वर्षा के लिए पूजा की जाती है,
विशेषतः फसल सुरक्षा के उद्देश्य से।
इस समुदाय का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि व्यक्ति किसी पीड़ा
या रोग से ग्रस्त है, तो वह
देवताओं की अप्रसन्नता का परिणाम है। अतः उपचार से पूर्व या समानांतर रूप से
देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक समझा जाता है। दूसरी ओर, जब
सामुदायिक जीवन में समृद्धि और प्रसन्नता व्याप्त होती है, तब
यह देवताओं की कृपा के रूप में देखा जाता है और उन्हें धन्यवाद स्वरूप भोग,
फल, प्रसाद आदि अर्पित किए जाते हैं।
यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि सहरिया जनजाति में चिकित्सा और
धर्म का संबंध गहन और अपरिवर्तनीय है। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति उनके सामाजिक
जीवन की संरचना, पर्यावरणीय
ज्ञान, और सामूहिक स्मृति से निर्मित होती है। यह केवल जैविक
उपचार नहीं, बल्कि सामुदायिक और आध्यात्मिक पुनर्स्थापन का
माध्यम भी है।
सहरिया जनजाति की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और औषधीय ज्ञान
सहरिया जनजाति, जिन्हें ‘वनवासी’ भी कहा जाता है, पारंपरिक औषधीय
ज्ञान के एक समृद्ध स्रोत के रूप में पहचानी जाती है। इनकी जीवन-शैली, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचना में चिकित्सा केवल भौतिक उपचार न
होकर, एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। यह
समुदाय पर्यावरण के साथ गहरे संबंध के माध्यम से प्राप्त जैव-सांस्कृतिक ज्ञान को
पीढ़ियों से संरक्षित करता आया है। यह चिकित्सा परंपरा मुख्यतः मौखिक परंपरा और
अनुभवजन्य प्रयोगों के माध्यम से संप्रेषित होती रही है।
इस समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औषधीय पौधों
और उनके पारंपरिक उपयोगों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:
1. स्त्री स्वास्थ्य एवं प्रसव पश्चात देखभाल
- रयोंझा: पौधे का गोंद प्रसव के बाद 15 दिनों तक महिलाओं को टॉनिक के रूप में दिया जाता है।
- सियोनला: फूलों से प्राप्त गोंद बवासीर के
उपचार में तथा महिलाओं को प्रसव पश्चात "कमरकास" के रूप में दिया
जाता है।
2. श्वसन और बाल चिकित्सा विकार
- मोर्शिखा: बच्चों के निमोनिया और सांस की तकलीफ
में उपयोगी।
- उमर, मगवा-मुसरी: निमोनिया,
बुखार और सर्दी के इलाज में प्रयुक्त।
- आंथ: बच्चों के पेट दर्द और मांसपेशीय दर्द
पर बाहरी प्रयोग।
3. त्वचा एवं चर्मरोग
- बाबर, पुआन, चिरोई,
कटाई, कस्तरुगा: चर्म
रोगों, खुजली, और फोड़े-फुंसियों
के उपचार हेतु प्रयुक्त।
- दतुआ, जल धनिया: बाह्य
लेप के रूप में प्रभावी।
4. यकृत, जठरांत्र एवं
दंत विकार
- पाथर-चट्टा, गटन, नियागर,
करार: पेट दर्द, पेचिश,
दंत रोग और मासिक धर्म के उपचार में।
- कसाई: मसूढ़ों और दांतों के दर्द में गरारे
हेतु प्रयोग।
5. अस्थि, संधि और
मांसपेशीय विकार
- इनगोटा, मलकवानी, सेमालू,
धामिन: आमवाती दर्द, सूजन, हड्डी टूटने और जोड़ों की समस्याओं में।
- घमेरा, मासिन: बाहरी
घावों के उपचार में।
6. पशु चिकित्सा और विषहरण
- इमलुआ, अमलतास, अपु:
पशुओं की बीमारियों और आंखों की समस्याओं में।
- बेल, कुमी, चिरोई:
मछली के ज़हर और सर्पदंश के उपचार में।
- अचार: सर्पदंश घावों पर लेप रूप में।
7. आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उपयोग
- डाब, चकेरी: धार्मिक
अनुष्ठानों में प्रयुक्त और प्रतीकात्मक चिकित्सा रूप में।
- कारा: पशुओं की सुरक्षा हेतु गले में बाँधा
जाता है।
सांस्कृतिक दृष्टिकोण
सहरिया जनजाति का पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान केवल उपचारात्मक
नहीं, बल्कि गहन सांस्कृतिक मान्यताओं,
विश्वासों और पर्यावरणीय समझ से जुड़ा हुआ है। इनके लिए रोग केवल
शारीरिक विकृति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक असंतुलन का द्योतक
है। इसीलिए उपचार की प्रक्रिया में औषधीय पौधों के साथ-साथ धार्मिक अनुष्ठानों और
स्थानीय देवताओं की भी केंद्रीय भूमिका होती है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि इन उपचार पद्धतियों में स्थानीय
महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती है, विशेष रूप से प्रसव-पूर्व और पश्चात देखभाल तथा बच्चों की सामान्य
बीमारियों में। पारंपरिक उपचारकों जैसे गुनिया, ओझा, भोपा आदि, समुदाय में सम्मानित सामाजिक भूमिका
निभाते हैं।
पारंपरिक चिकित्सा की उपादेयता और मूल्यांकन: सहरिया जनजाति
के मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य अनुभव पर एक दृष्टि
सहरिया जनजाति की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली न केवल एक
उपचार विधि है, बल्कि यह
उनके सांस्कृतिक विश्वास, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक संगठन
का अभिन्न अंग है। गर्भधारण, प्रसव और प्रसवोत्तर काल जैसे
जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में महिलाएं जिन जैविक और सामाजिक चुनौतियों से गुजरती
हैं, उनके समाधान में यह चिकित्सा पद्धति निर्णायक भूमिका
निभाती है। यह खंड सहरिया समुदाय में मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के पारंपरिक
चिकित्सकीय दृष्टिकोण, व्यवहार और धार्मिक आयामों को
प्रस्तुत करता है।
1. गर्भावस्था और
प्रसव के दौरान पारंपरिक देखभाल
प्रसवपूर्व देखभाल
गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर उल्टी, सूजन (एडिमा), अपच,
कमजोरी और शरीर दर्द जैसे लक्षण देखे जाते हैं। सहरिया जनजाति इन
लक्षणों के इलाज हेतु घरेलू उपचार अपनाती है, जैसे:
- जले हुए मकई के दाने — उल्टी और शरीर दर्द से राहत हेतु दिया जाता है।
प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल
प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, कमजोरी और शारीरिक थकावट से राहत हेतु
परंपरागत रूप से प्रयुक्त तत्व:
- बबूल का गोंद, गुड़ का पानी, दूध में हल्दी का मिश्रण
— शरीर को शक्ति देने वाले टॉनिक के रूप में।
- मासिक धर्म
विकार, बांझपन,
गर्भाशय का बाहर आना (प्रोलैप्स), ऐंठन व
गर्भपात जैसी समस्याओं का उपचार भी जड़ी-बूटियों और घरेलू पद्धतियों से किया
जाता है।
प्रसव सुरक्षा हेतु टोटके
बुरी आत्माओं से बचाव के लिए नींबू, लाल मिर्च और धातु
के टुकड़ों का उपयोग गर्भवती महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो उन्हें शरीर पर बाँधने की परंपरा से जुड़ा है।
2. गर्भपात और प्रजनन व्यवहार
विवाहेतर या अवांछित गर्भधारण के मामलों में सहरिया महिलाएं
पारंपरिक गर्भपात पद्धतियों का सहारा लेती हैं:
- स्थानीय जड़ी-बूटी को गर्भाशय में रखना — जिससे भ्रूण नष्ट हो जाता है।
- गैंस्की नामक पौधे की जड़ + गुड़ व काली मिर्च का मिश्रण — गर्भपात के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने हेतु।
गर्भपात को सामान्य सामाजिक रिश्तों में स्वीकार नहीं किया
जाता, इसलिए यह प्रक्रिया गुप्त रूप
से की जाती है।
3. शिशु रोगों एवं
श्वसन संबंधी विकारों का उपचार
खांसी-जुकाम और शारीरिक ताप
- तुलसी + शहद, अदरक + नमक, काली मिर्च की चाय
— सामान्य संक्रमणों में प्रमुख घरेलू उपचार।
- सरसों का तेल + अदरक — बच्चों की नाभि पर मालिश करके सर्दियों में सर्दी से
बचाव हेतु।
पेट संबंधी समस्याएं
- नींबू + बेल का रस — छोटे बच्चों के पेट दर्द के लिए।
- ओआरएस — गंभीर मामलों में सीमित रूप से आधुनिक उपायों का सहारा।
निमोनिया और एआरआई
- जयफल, केसर, लौंग — बच्चों व खदानों में काम करने वाले
वयस्कों में सांस की बीमारियों में प्रयोग।
- गर्म लोहे की छड़ से झाड़-फूंक — अंधविश्वास से जुड़ा एक धार्मिक उपचारात्मक प्रयास।
4. धार्मिक उपचार पद्धति
सहरिया जनजाति में रोगों को केवल शारीरिक विकृति नहीं बल्कि
आध्यात्मिक असंतुलन के रूप में देखा जाता है। अतः निम्न रूपों में धार्मिक
उपचार प्रचलित हैं:
- झाड़-फूंक: पुजारी द्वारा रोगी पर राख फेंक कर
बीमारी दूर करने की प्रक्रिया।
- विषहरण
पूजा: सांप,
बिच्छू आदि के काटने पर रोगी को स्थानीय देवता के मंदिर ले
जाया जाता है।
5. पारंपरिक
उपचारों की प्रासंगिकता के कारक
पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की स्थिरता और लोक-आस्था
निम्नलिखित कारणों पर आधारित है:
- उपचारकों
पर विश्वास और उनका सहज उपलब्ध होना
- उपचार की
किफायती प्रकृति और स्थानीय पहुंच
- सांस्कृतिक
जुड़ाव और धार्मिक महत्व
- सरकारी
स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था, भेदभाव और स्वच्छता की कमी
- जनजातीय और
गैर-जनजातीय समुदायों के बीच सांस्कृतिक दूरी और संवेदनहीन स्वास्थ्य कर्मी
सहरिया जनजाति में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली केवल एक विकल्प
नहीं, बल्कि एक संवेदनशील सामाजिक और
सांस्कृतिक तंत्र है, जो न केवल बीमारियों से निपटने बल्कि
समुदाय की आत्मा और पहचान को भी संरक्षित करता है। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा तक सीमित
पहुँच और संस्थागत असंवेदनशीलता इसकी आवश्यकता को बनाए रखती है, फिर भी यह आवश्यक है कि जनजातीय स्वास्थ्य संस्कृति को 'अवैज्ञानिक' या 'पिछड़ा'
कहकर खारिज करने की बजाय, इसे सामाजिक संदर्भ में
समझा जाए और सशक्तिकरण तथा समावेशी स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत समाहित किया जाए।
निष्कर्ष
सहरिया जनजाति का धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक मूल्य और स्वास्थ्य संस्कृति एक
परस्पर गुंथे हुए तंत्र का निर्माण करते हैं। इनकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ
केवल रोग निवारण नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान, आध्यात्मिक विश्वास और सामुदायिक एकता का भी प्रतीक हैं। जनजातीय
स्वास्थ्य नीतियों और हस्तक्षेपों को सफल बनाने के लिए, उनके
स्थानीय ज्ञान, सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक संरचनाओं को
सम्मिलित दृष्टिकोण से समझना और सम्मान देना आवश्यक है।
उपसंहार
उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सहरिया जनजाति की
स्वास्थ्य संस्कृति गहराई से उनकी धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और सामाजिक
संरचना से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य की अवधारणा उनके लिए केवल शारीरिक अवस्था नहीं,
बल्कि एक आध्यात्मिक और सामुदायिक अनुभव भी है। ईश्वर, देवी-देवताओं और पारंपरिक उपचारकों में गहरी आस्था के चलते वे आधुनिक
चिकित्सा पद्धति की अपेक्षा पारंपरिक एवं धार्मिक उपचारों को प्राथमिकता देते हैं।
यद्यपि सहरिया जनजाति आज भी अनेक स्तरों पर सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का
सामना कर रही है, किन्तु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि
उनके पास औषधीय पौधों और परंपरागत चिकित्सा ज्ञान का समृद्ध भंडार है, जिसे यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नीति समर्थन मिले, तो
यह व्यापक रूप से मानवता के हित में प्रयोग हो सकता है।
इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक समावेशी पहुंच, और पारंपरिक
ज्ञान का वैज्ञानिक मूल्यांकन—इन तीनों की संयुक्त भूमिका अत्यंत आवश्यक है।
शिक्षा न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि
यह धार्मिक विश्वास और आधुनिक चिकित्सा के बीच संतुलन बनाने में भी सहायता करेगी।
अतः जनजातीय समुदायों को केवल "पिछड़ा" कहकर नहीं, बल्कि संस्कृति-संवेदनशील नीतियों के माध्यम से सशक्त बनाकर ही
समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।
नीतिगत सुझाव (Recommendations)
1.
संवेदनशील और
समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं का विकास: सहरिया समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सांस्कृतिक रूप से अनुकूल
बनाया जाना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को स्थानीय
भाषा, विश्वासों और उपचार पद्धतियों के प्रति संवेदनशील
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
2.
पारंपरिक
चिकित्सा ज्ञान का दस्तावेजीकरण और वैज्ञानिक मूल्यांकन: सहरिया
जनजाति के पारंपरिक औषधीय ज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति से प्रलेखित,
संरक्षित और प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता
है ताकि उनका सतत उपयोग किया जा सके और लाभकारी तत्वों को मुख्यधारा में लाया जा
सके।
3.
जनजातीय महिलाओं
के लिए मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम: गर्भवती और नवप्रसूता महिलाओं के लिए विशेष
रूप से मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और स्थानीय महिला स्वास्थ्य
कार्यकर्ताओं (ASHA आदि) के
माध्यम से पोषण, टीकाकरण, प्रसवपूर्व
और प्रसवोत्तर सेवाएं पहुंचाई जाएं।
4.
लोक-चिकित्सकों
(Traditional Healers) का एकीकरण: पारंपरिक उपचारकों को "सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शक" के रूप
में प्रशिक्षित कर उनकी भूमिका को पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच पुल
की तरह प्रयोग किया जा सकता है।
5.
स्वास्थ्य
शिक्षा और जन-जागरूकता अभियान: बाल्यावस्था बीमारियों, टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता,
पोषण और उचित दवा प्रयोग से जुड़ी जानकारी को स्थानीय बोली और
परंपरा के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए।
6.
भेदभाव रहित
स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थापना: स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जाने वाले
भेदभाव को खत्म करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाया जाए और जनजातीय
अधिकारों पर केंद्रित प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।
7.
हर्बल बागवानी
और स्थानीय औषधीय पौधों को बढ़ावा देना: जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों की
खेती और प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देकर न केवल स्वास्थ्य बल्कि आजीविका के
अवसर भी उत्पन्न किए जा सकते हैं।
8.
नीति निर्माण
में जनजातीय प्रतिनिधित्व: जनजातीय समुदायों की जरूरतों को बेहतर तरीके
से समझने के लिए नीति निर्माण में सहरिया समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल
किया जाना चाहिए।
संदर्भ ग्रंथ
1.
अलेक्जेंडर, के.सी., प्रसाद आर.आर और
जहांगीरदार, एम.पी. (1984).
जनजातीय शिक्षा और जनजातीय विकास, भारत में जनजातीय
संस्कृति. रावत प्रकाशन, नई
दिल्ली.
2.
आचार्य, डी., और श्रीवास्तव,
ए. (2008). स्वदेशी हर्बल मेडिसिन्स:
ट्राइबल फॉर्म्युलेशन्स एंड ट्रेडिशनल हर्बल प्रैक्टिसेज, जयपुर: आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर.
3.
जनगणना
(2011), भारत सरकार
4.
त्यागी
बी.आर. (2012). शिक्षा का
अधिकार: औचित्य, परिभाषा और दिशानिर्देश, नई दिल्ली: एराइज पब्लिशर्स.
5.
दास, आर. चंद्रा (2013). हैजा
को ठीक करने के लिए उड़ीसा की पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मा एंड बायो-साइंस.
6.
दोशी, एस.एल., और व्यास,
एन. (1992). आदिवासी राजस्थान: अरावली
पर धूप, उदयपुर: हिमांशु प्रकाशन. मल्होत्रा, रमेश (2011). शिक्षा का अधिकार: सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, नई दिल्ली: पीडीएस पब्लिशिंग हाउस.
7.
पांडे
एस.के.(1988). सहरिया: चंबल
की एक पिचड़ी जंजती, मध्य प्रदेश संदेश अगस्त, भोपाल.
8.
बनर्जी,
देबाबर (2004). द पीपल एण्ड हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट इन इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ
हेल्थ सर्विसेज़.
9.
बसु, सलिल (1994). भारत में जनजातीय स्वास्थ्य, दिल्ली:
मानक प्रकाशन.
10. बालगीर, आर.एस. (2006). जनजातीय स्वास्थ्य समस्याएं,
रोग भार और जनजातीय में सुधारात्मक चुनौतियाँ उड़ीसा की
जनजातियों पर विशेष जोर देने वाले समुदाय, राष्ट्रीय
संगोष्ठी की कार्यवाही पर जनजातीय स्वास्थ्य
11. भटनागर, के.एस.(1961). गढेर: ए विलेज सर्वे, सेंसस ऑफ इंडिया.
12. भटनागर, के.एस.(1961). गढेर: ए विलेज सर्वे, सेंसस ऑफ इंडिया.
13. भारत सरकार (2009-10),
वार्षिक रिपोर्ट, आदिवासी कल्याण
मंत्रालय, नई दिल्ली.
14. मंडल, देवव्रत, (1988). मध्य प्रदेश में एक आदिम
जनजाति का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य, स्वरूप एंड संस
प्रकाशन, नई दिल्ली
15. मंडल, देवव्रत, (1988). मध्य प्रदेश में एक आदिम
जनजाति का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य, स्वरूप एंड संस
प्रकाशन, नई दिल्ली.
16. माहेश्वरी, जे. के और सिंह, हरी (1988).
एथनोबोटिकल आब्ज़र्वैशन ऑन द सहरिया ट्राइब ऑफ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश,
एथनोबोटिकल डेसीप्लिन, नैशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, लखनऊ.
17. रानी, मिदताला (2009). भारत में जनजातीय शिक्षा
की समस्याएं: मुद्दे और संभावनाएं, नई दिल्ली: कनिष्क
प्रकाशक और वितरक.
18. व्यास, एन., और भानावत, एम. (2008).
आदिवासी जीवनधारा, उदयपुर: हिमांशु
प्रकाशन.
19. शंकर, वी. (2014). सहरिया समाज एवं संस्कृति,
जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.
20. शर्मा, हरिओम और सिकंदरार, आर.एल.एस. (2001). मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वरूप एंड संस प्रकाशन, नई दिल्ली.
21. शर्मा, हरिओम और सिकंदरार, आर.एल.एस. (2001). मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वरूप एंड संस प्रकाशन, नई दिल्ली.
.png)