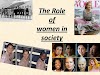डॉ० निधि शर्मा सहायक आचार्या (हिंदी विभाग)
राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नगरोटा बगवां
जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश-176047
nidhieera@gmail.com
शोध-सार- साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे आकर्षक
एवं सशक्त माध्यम रही है। लघु कलेवर में होने के बावजूद भी कहानी के माध्यम से
हमारा व्यक्तित्व हमारे समक्ष दर्पण की भांति स्पष्ट झलकता है। आधुनिक हिंदी
साहित्य में प्रेमचंद एक प्रतिभाशाली एवं प्रभावशाली लेखक रहे हैं,
जिन्होंने
उपन्यास, कहानी,
नाटक आदि में
अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रेमचंद महान् पत्रकार एवं संपादक भी रहे हैं।
इन्होंने हंस, मर्यादा,
जागरण आदि पत्र-
पत्रिकाओं का संपादन कार्य संभाला। इन्होंने पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से राजनीतिक,
सामाजिक,
साहित्यिक चेतना
जगाने का भरसक प्रयास किया। उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद ने
कहानियों में
अपनी लेखनी का जादू बिखेरा है। इनकी कहानियां न केवल पाठकों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों,
कुरीतियों
पर भी करारी चोट
करती हैं। इन्होंने 300 के लगभग कहानियां लिखी हैं,जो मानसरोवर के आठ खंडों में संकलित हैं।
इन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। इनकी
कहानियां समाज के विभिन्न वर्गों की ज्वलंत समस्याओं से हमें रूबरू करवाती हैं।
मूल शब्द- यथार्थ,
प्रासंगिक,
संस्कार,
सामाजिक सुधार,
बदलाव,
समाधान।
युग स्रष्टा एवं
युग दृष्टा साहित्यकार प्रेमचंद की कहानियां साहित्य को नई दिशा देने में सहायक
रही हैं। मुंशी प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य ही मानव संस्कार का प्रभावशाली,
सशक्त एवं
प्रेरणादायक माध्यम है। इनका अपना जीवन अभावों,
कष्टों में
गुज़रा इसलिए इन्होंने मानवीय जीवन के दुख-दर्द को अनुभव किया और पूरी ईमानदारी से
उसका चित्रण अपनी कहानियों में किया । "प्रेमचंद
साहित्य का महत्त्व केवल समाजशास्त्रीय नहीं है,
उसका बहुत बड़ा
कलात्मक महत्त्व भी है। किसानों पर बहुत लोगों ने लिखा है। प्रेमचंद अब भी उनसे
अलग और ऊंचे ही दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है,
हर पात्र के मन
में वह पैठ जाते हैं। उसके भीतर की दुनिया की कोई बात उनसे छिपी नहीं रहती। उसके
बाहर की दुनिया तो वह देखते ही हैं। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार उनकी कला का एक
आधारभूत तत्त्व है।"1 इसी कारण इनकी कालजयी कहानियां आज भी
साहित्यकारों का मार्ग प्रशस्त करती आ रही हैं। प्रेमचंद
अपनी कहानियों
के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविकताओं,
सामाजिक चिंताओं,
आर्थिक समस्याओं,
शोषण,
नारी की दुर्दशा,
किसान व दलित
वर्ग की जो जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करते हैं,
उसके मुख्य पहलू
निम्नलिखित हैं –
1- मानवीय चेतना को जगाती कहानियां-
इनकी कहानियां
सामाजिक परिवर्तन लाकर मानवीय चेतना को जगाने में सहायक रही
हैं। प्रेमचंद की कहानियां एक ऐसी धरोहर है जो भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं
को सुलझाने में भारतीयों का मार्ग प्रशस्त करती रही हैं और करती रहेंगी। "जिस
तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी,
चाहे वह कैसा ही
क्रूर और कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान
की आंखें भर आईं।..........तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया,
मानो मेरे कानों
में शंखनाद कर मुझे कर्म-पथ में प्रवेश का उपदेश दिया हो।"2
प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से मनुष्य
को उत्तरदायित्व का ज्ञान करवाना चाहते थे ताकि इस ज्ञान को शक्ति बना वह अपने
जीवन को सही राह दे सके।
"किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम किया
जाता है, उसी का नाम ज़िंदगी है। हमें कामयाबी वहीं
होती है, जहां हम अपने पूरे हौंसले से काम में लगे हों,
वही लक्ष्य
हमारा स्वप्न हो, हमारा प्रेम हो,
हमारे जीवन का
केंद्र हो। हममें और इस लक्ष्य के बीच में और कोई इच्छा,
कोई आरजू दीवार की तरह न खड़ी हो.... मुल्क में आप जैसे
हज़ारों नौजवान हैं, जो अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीना और
मरना सीख जाएं तो चमत्कार कर दिखाएं....जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। सच्ची
ज़िंदगी वहीं है जहां हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते हैं। "मुंशी
प्रेमचंद की कहानियां मानवीय चेतना को जगा कर
अपने कर्त्तव्य
पर अडिग रहते हुए मनुष्य के मन में सही निर्णय शक्ति का भाव जगाने में सक्षम हैं।
2. देशप्रेम/देशसेवा का भाव जगाती कहानियां-
प्रेमचंद एक
सच्चे देशभक्त थे। इन्होंने अपनी कहानियों में देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले
पात्रों का चित्रण किया है - "चिंता ने गंभीरता से कहा- इसकी तुम कुछ चिंता न
करो, दादा! मैं अपने बाप की बेटी हूं। जो कुछ उन्होंने किया,
वही मैं भी
करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिए।
मेरे सामने भी वही आदर्श है। जा कर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और
हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा,
तो आप लोग मुझे
किसी से पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना,
तो तलवार के एक
हाथ से इस जीवन का अंत कर देना।"4 प्रेमचंद देशसेवा को प्रत्येक मनुष्य का परम कर्त्तव्य समझते हैं।
"प्रेमचंद उन महान् आत्माओं में थे जिनका जन्म
स्वदेश के कल्याण के लिए होता है, जिनके रग-रग में स्वदेश-प्रेम की लहर दौड़ा
करती है, जिनके हृदय की प्रत्येक धड़कन में देश-कल्याण
की चिंता व्याप्त रहती है।"5 इन्होंने अपनी कलम के बल पर साधारण जन में
देशभक्ति जगाने और अपना सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा देकर एक सच्चे देशभक्त का
परिचय दिया है।
3. प्रकृति और मानव के अटूट संबंध को सहेजती
कहानियां –
महान्
साहित्यकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से प्रकृति और मानव के अटूट संबंध
को स्पष्ट किया है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इनकी
कहानियां 'जुगनू की चमक'
और 'घर जमाई'
के उदाहरण
प्रस्तुत हैं - "कहीं ऊंचे -ऊंचे साखू और महुए के जंगल
थे और कहीं हरे-भरे जामुन के वन। उनकी गोद में हाथियों और हिरणों के झुंड किलोलें
कर रहे थे। धान की क्यारियां पानी से भरी हुई थीं। किसानों
की स्त्रियां
धान रोपती थीं और सुहावने गीत गाती थीं।"6
"जब वह आमों के बाग में पहुंचा,
जहां डालियों पर
बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरों और लिसोड़ों में एक
स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुका कर रोने
लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति-कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में,
वहां के प्रकाश
में, मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी वहां की अंगुल-अंगुल भूमि माता
के पद चिन्हों से पवित्र थी, माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक आकाश
में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन-सी संजीवनी थी जिसने उसके
शोकार्त्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया।"7
प्रेमचंद की कहानियां प्रत्येक मनुष्य के मन
में प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव जगाने का
प्रयास करती
नज़र आ रही हैं। इनकी बहुत सी कहानियों में पर्यावरण और ग्रामीण जीवन की समकालीन
चिंताओं को उजागर किया गया है। इनकी कहानियां वर्तमान समय में भयंकर रूप धारण किए
हुए पर्यावरणीय संकट से उभरने की प्रेरणा भी देती हैं।
4 सामाजिक असमानताओं की विरोधी एवं सामाजिक
बदलाव से प्रेरित कहानियां –
इनकी कहानियां
समाज सुधार एवं समाज कल्याण की प्रेरणा देती हैं। अपनी कहानियों के माध्यम से
सामाजिक सुधार एवं बदलाव लाना चाहते थे। इनका मानना था कि आत्मबल व
दृढ़संकल्प से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इनकी कहानी 'लाग डांट'
का एक उदाहरण
प्रस्तुत है- "स्वराज लेने का केवल एक ही उपाय है और वह आत्म संयम है। यही
महौषधि तुम्हारे समस्त रोगों को समूल नष्ट करेगी। आत्मा को बलवान बनाओ,
इंद्रियों को
साधो, मन को वश में करो,
तुममें
भ्रातृभाव पैदा होगा,
तभी वैमनस्य
मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा,
तभी भोग विलास
से मन हटेगा, तभी नशेबाजी का दमन होगा। आत्मबल के बिना
स्वराज्य कभी उपलब्ध न होगा।" 8 मुंशी प्रेमचंद साम्यवाद व गांधीवादी
विचारधारा के लेखक रहे हैं। वे अमीर-गरीब के बीच की खाई को पाटना चाहते थे। इस
संदर्भ में कहानी की निम्न पंक्तियां देखिए- "सोचता,
मनुष्य क्यों
पाप करता है? इसलिए न कि संसार में इतनी विषमता है। कोई तो
विशाल भवनों में रहता है और किसी को पेड़ की छांह भी मयस्सर नहीं। कोई रेशम और
रत्नों से मढ़ा हुआ है, किसी को फटा वस्त्र भी नहीं। ऐसे न्यायविहीन
संसार में यदि चोरी, हत्या और अधर्म है तो यह किसका दोष?
वह एक ऐसी समिति
खोलने का स्वप्न देखा करता, जिसका काम संसार से इस विषमता को मिटा देना
हो। संसार सबके लिए है और उसमें सबको सुख भोगने का समान अधिकार है।"9
प्रेमचंद
रूढ़िवादी सोच के विरोधी थे। वे अपनी कहानियों में पारंपरिक सोच और सामाजिक
असमानताओं का विरोध कर सामाजिक सुधार लाने में प्रयासरत रहे हैं। दो उदाहरण
प्रस्तुत हैं-
"पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि
दहेज के नाम पर कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन क्वांरी बैठी रहे। यहां भी
आपका आदर्शवाद आ कूदा। समाज के नेताओं का छल- प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं,
फिर भी आपकी
आंखें नहीं खुलतीं। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित
रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। दो- चार ऐसे
व्यक्ति भले ही निकल आवें जो दहेज के लिए हाथ न फैलावें; लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी
हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं;
लेकिन मिलते हुए
दहेज को छोड़ देनेवाला मैंने आज तक न देखा। अब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा
और जीविका की सुविधाएं निकल आयेंगी, तो यह प्रथा
भी विदा हो
जाएगी।"10
"पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है,
तो स्त्री उसे
क्यों नहीं ठुकरा सकती? वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को
उसका गुलाम बना दिया। वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे ,कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता,
कोई
चूं भी नहीं कर
सकता। पुरुष अपनी दूसरी,
तीसरी,
चौथी शादी कर
सकता है, स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसी
कठोरता से शासन कर सकता है। वह जानता है कि स्त्री कुल-मर्यादा के बंधनों में
जकड़ी हुई है, उसे रो-रोकर मर जाने के सिवा और कोई उपाय
नहीं है। अगर उसे भय होता है कि औरत भी उसकी ईंट
का जवाब पत्थर
नहीं, ईंट से भी नहीं;
केवल थप्पड़ से
दे सकती है, तो उसे कभी इस बदमिजाजी का साहस न होता
है।"11 इनकी कहानियों में न केवल सामाजिक असमानताओं,
कुप्रथाओं का
विरोध है बल्कि उनके निदान का रास्ता भी सुझाया गया है। इनकी पत्नी शिवरानी देवी
अपनी कृति 'प्रेमचंद घर में'
में स्त्रियों
के अधिकारों को लेकर मुंशी प्रेमचंद के विचारों को प्रकट करते हुए लिखती हैं-
"जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी और सब कानूनी अधिकार उनको बराबर न मिल
जाएंगे तब तक महज काम करने से काम नहीं चलेगा।"12
मुंशी प्रेमचंद
कुप्रथाओं, विसंगतियों का कड़ा विरोध करते हैं। प्रेमचंद
ताउम्र कहानियों के माध्यम से जन-जन में क्रांति का भाव जगाने में काफ़ी हद तक
कामयाब रहे। लेखक शंभूनाथ जी लिखते हैं- "प्रायः सभी उपन्यासों और कहानियों
में प्रेमचंद ने सामाजिक कुप्रथाओं पर चोट की और नारी मुक्ति की आवाज़ उठाई वे सिर्फ सुधार में विश्वास नहीं करते बल्कि
सामाजिक क्रांति भी चाहते हैं।" 13
5. सामाजिक समस्याओं का चित्रण-
प्रेमचंद ने
अपनी कहानियों में छुआछूत, जात-पात,
अनमेल विवाह,
दहेज-प्रथा,
धर्म के
ठेकेदारों द्वारा लोगों को भयभीत करना, नारी की दुर्दशा,
दलित/मज़दूर
वर्ग का शोषण, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को उठाकर लोगों को
सोचने पर मजबूर कर दिया है। तत्कालीन समय में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते
हुए वे लिखते हैं- "किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित
आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे अधिकारी वर्ग उनके भक्त,
अमले उनके सेवक, वकील-मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अरदली,
चपरासी तथा
चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि
अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया बल्कि इसलिए कि वह कानून के
पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्नय
वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में
आए।...... न्याय
के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप
खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था,
न स्पष्ट भाषण
के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे,
किंतु लोभ से
डावांडोल।यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दीख पड़ता
था।वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था
किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो,
वहां न्याय की
कल्पना भी नहीं की जा सकती।...….....आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव
हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां,
बड़ी-बड़ी
दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं।"14
जात-पात के नाम
पर गांवों में साहूकार, जमींदार,
ब्राह्मण,
धनी वर्ग
भोली-भाली जनता से पशुओं से भी बुरा व्यवहार कर रहे थे। इसका दिल दहलाने वाला
वर्णन इनकी कहानी 'ठाकुर का कुआं'
व 'सदगति'
में मिलता है। 'ठाकुर का कुआं'
कहानी का एक
उदाहरण प्रस्तुत है- "ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं। क्या एक लोटा पानी न
भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ
चुपके से। ब्रह्म-देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे,
साहू जी एक के
पांच लेंगे। गरीबों के दर्द कौन समझता है! हम तो मर भी जाते हैं,
तो कोई दुआर पर
झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से
पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़ुवा सत्य था। गंगी क्या
जवाब देती; किंतु उसने वह बदवूदार पानी पीने को न
दिया।"15
धर्म के ठेकेदार
भोली- भाली जनता को धर्म का डर दिखाकर किस तरह लूटते हैं और उनका शोषण करते हैं
इसका सजीव चित्रण इनकी कहानी 'सवा सेर गेहूं'
में किया गया है
- "शंकर ने चकित होकर कहा- मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो साढ़े पांच मन हो
गए। तुम भूलते हो,
मेरे यहां किसी
का छटांक भर न अनाज है, न एक पैसा उधार।विप्र-इसी नीयत का तो यह फल भोग
रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता।यह कहकर विप्र ने उस सवा सेर गेहूं का जिक्र किया,
जो आज के सात
वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर मैंने इन्हें कितनी बार
खेलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन- सा काम किया?
जब पोथी- पत्रा
देखने, साइत-सगुन विचारने,
द्वार पर आते थे,
कुछ-न-कुछ 'दक्षिणा'
ले ही जाते थे।
इतना स्वार्थ! सवा सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया,
जो मुझे निगल ही
जाएगा।
शंकर- पांडे,
क्यों एक गरीब
को सताते हो, मेरे खाने का ठिकाना नहीं,
इतना गेहूं
किसके घर से लाऊंगा?
विप्र- जिसके घर
से चाहे लाओ, मैं छटांक- भर भी न छोडूंगा,
यहां न दोगे,
भगवान् के घर तो
दोगे।
शंकर कांप उठा।
......... एक तो ऋण-वह भी ब्राह्मण का- बही में नाम रह
गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से उसे रोमांच हो गया। ........उसी
घड़ी तगादा करके
ले लिया होता, तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों
पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान् के यहां जवाब देना
पड़ेगा।
विप्र- वहां का
डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। वहां तो सब अपने ही
भाई- बंधु हैं।ऋषि- मुनि, सब तो ब्राह्मण ही हैं;देवता ब्राह्मण हैं जो कुछ बने बिगड़ेगी,
संभाल
लेंगे।"16
7. किसान/मज़दूरों की दुर्दशा को दर्शाती
कहानियां -
इनकी कहानियों
में भारतीय किसानों की दुर्दशा का जो चित्रण मिलता है,
वह आज भी उतना
ही प्रासंगिक है। आज भी किसान आर्थिक तंगी,फसल का
उचित मूल्य न
मिलने और अधिक कर्ज़ा हो जाने के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए विवश हो
जाते हैं। "क्या आश्चर्य की देश की दुर्दशा,
देश के प्राण
किसानों की भयंकर दशा देखकर उनकी आत्मा द्रवीभूत हो उठी।
वह कर्मण्य थे।
देशोद्वार के लिए-पीड़ित किसानों का दुःख दूर करने के लिए-क्रमशः कर्मरत हो
गए।.... अपनी जादू भरी लेखनी द्वारा वह जनता को देश की-देहातों की- दरिद्रता से परिचित कराते थे,
बताते थे कि
किसान जो देश के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं,
स्वयं मुट्ठीभर
अन्न के लिए तरसते हैं, भूखे मरते हैं। विधाता के क्रूर व्यंग्य का
वह सत्य एवं संजीव चित्र खींचते थे।"17
भारत का किसान
कितना गरीब, बेबस और लाचार है। इसका यथार्थ
चित्रण 'पूस की रात'
कहानी में मिलता
है-"पूस की
अंधेरी रात! आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे ।हल्कू अपने खेत के किनारे
ऊंख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर
ओढ़ कांप रहा था।खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से
कूं-कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी।"18
अतः प्रेमचंद
अपने समय के प्रथम सर्वश्रेष्ठ मौलिक लेखक रहे हैं,जिन्होंने यथार्थ की धरती पर अपना साहित्य
रचा। "अतःयहां इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रेमचंद
मूलतः मानववादी,
राष्ट्रवादी एवं
भौतिकवादी थे। यद्यपि उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने क्रमबद्ध रूप
में न तो मार्क्सवादी का ही अध्ययन किया था और न उस पर विचार ही। परंतु यह भी सत्य
है कि न्याय और अन्याय के संघर्ष में प्रेमचंद न्याय के साथ तथा पूंजीपति एवं निर्धन
के संघर्ष में निर्धन के साथ दिखाई पड़ते हैं। यदि साहूकार और किसान के बीच संघर्ष
है, तो वह किसान के साथ हैं। ज़मींदार और कारिंदे निर्धन कृषक का शोषण करते हैं,
तो प्रेमचंद उस
शोषण के विरुद्ध किसान से लाठी उठाने को कहते हैं। यदि शासक वर्ग अत्याचार करता है,
तो प्रेमचंद
जनता के साथ दिखाई पड़ते हैं।“19
इनकी कहानियां
समाज के हर वर्ग और उसके संघर्ष को दर्शाती हैं। अपनी
कहानियों के माध्यम से वे सामाजिक सुधार व बदलाव लाना चाहते थे। वर्तमान समय में
भी इनकी कहानियां उतनी ही प्रासंगिक हैं,
जितनी तत्कालीन
समय में थी। इन्होंने अपनी कहानियों में समाज में व्याप्त समस्याओं का सिर्फ
चित्रण ही नहीं किया बल्कि समाधान का रास्ता भी सुझाया है।
संदर्भ सूची -
1. डॉ० रामविलास शर्मा (भूमिका एवं मार्गदर्शन): प्रेमचंद रचनावली (खंड-एक):,
जनवाणी प्रकाशन
प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली,
द्वितीय सं० 2006,पृ०45
।
2. प्रेमचंद: प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियां,
विद्यापीठ
पब्लिकेशन हाउस,
दिल्ली,
सं० 2006,
पृ०157 ।
3. प्रेमचंद: प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां,
प्रतिभा
प्रतिष्ठान, नई दिल्ली,
सं० 2015,
पृ० 69-70
।
4. प्रेमचंद: प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियां,पृ०30
।
5. डॉ० रामविलास शर्मा
(भूमिका एवं मार्गदर्शन): प्रेमचंद रचनावली (खंड-बीस),
जनवाणी प्रकाशन
प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली,
द्वितीय सं० 2006,
पृ० 182
।
6. प्रेमचंद: प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां,
प्रतिभा
प्रतिष्ठान, नई दिल्ली,
सं० 2015,
पृ०111
।
7. प्रेमचंद: प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियां,
पृ०177
।
8. प्रेमचंद: प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां,
पृ०99-100
9. वही,पृ०15 ।
10. डॉ० रामविलास शर्मा (भूमिका एवं मार्गदर्शन) : प्रेमचंद रचनावली( खंड:पन्द्रह), जनवाणी प्रकाशन दिल्ली,
द्वितीय सं० 2006,
पृ० 28
।
11. वही,
पृ०60 ।
12. शिवरानी देवी : प्रेमचंद घर में,
आत्माराम एंड
संस, दिल्ली, सं० 1956,
पृ०113
।
13. शंभूनाथ : प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन,
नेशनल पब्लिशिंग
हाउस, दिल्ली,
सं०1988,
पृ०26।
14. कमलेश पांडेय(सं०): प्रेमचंद की अमर कहानियां,
सुहानी बुक्स,पांडव नगर काम्प्लेक्स,
दिल्ली,
सं० 2013,पृ० 9 ।
15. डॉ० रामविलास शर्मा(भूमिका एवं मार्गदर्शन):
प्रेमचंद
रचनावली (खंड-पन्द्रह),जनवाणी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,
दिल्ली,
द्वितीय सं० 2006,
पृ०55
।
16. कमलेश पांडेय(सं०):प्रेमचंद की अमर कहानियां,
पृ० 35-36 ।
17. डॉ० रामविलास शर्मा (भूमिका एवं मार्गदर्शन): प्रेमचंद रचनावली (खंड-बीस), पृ०182
18. प्रेमचंद : प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियां,
पृ० 242
।
19. डॉ० जाफ़र रज़ा:प्रेमचंद उर्दू-हिंदी कथाकार, लोक भारती प्रकाशन,
इलाहाबाद, सं० 2014,
पृ०296
।
.png)