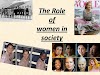डॉ. चिलुका पूष्पलता
एम.ए,एम.फिल,पी.एच.डी,अनुवाद में डिप्लोमा,एम.बी.ए।
अध्यक्षा हिन्दी विभाग
दयानंदा सागर कला, विज्ञान और
वणिजय महाविद्यालय
बैगलुरू
सारः
राधावल्लभ
सम्प्रदाय उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख सम्प्रदाय है,
जिसकी
स्थापना 16वीं
शताब्दी में श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा वृंदावन में की गई थी। यह
सम्प्रदाय मुख्यतः राधा के परमत्व को स्वीकार करता है और उन्हें ही परब्रह्म
मानकर भक्ति करता है। जबकि अधिकांश वैष्णव सम्प्रदायों में भगवान श्रीकृष्ण को
परब्रह्म माना जाता है, वहीं
राधावल्लभ सम्प्रदाय इस धारणा को उलट कर राधा को सर्वोच्च सत्ता घोषित करता है।
इस
सम्प्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि में वेदान्त, भक्ति
और रस सिद्धान्त का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। राधा को इस सम्प्रदाय में सगुण
तथा निर्गुण दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। वे मूल रूप में निर्गुण
परब्रह्म हैं,
किन्तु
भक्तों की भावना के कारण सगुण रूप में लीलाएं करती हैं। राधा-कृष्ण के मधुर प्रेम
को इस सम्प्रदाय ने आध्यात्मिक प्रेम का आदर्श बताया है।
इस
सम्प्रदाय का मुख्य आधार रसात्मक भक्ति है, जिसमें
भक्त और भगवान के मध्य प्रेम के माधुर्य रस की प्रधानता होती है। यहाँ ज्ञान,
योग
या कर्म के स्थान पर प्रेम और अनुभूति को साधना का माध्यम माना गया है।
राधावल्लभ सम्प्रदाय सहज, सरल,
औपचारिकताओं
से रहित भक्ति मार्ग को अपनाता है, जो
भाव और समर्पण पर आधारित है।
भूमिका
धर्म के क्षेत्र में भारतीयजन सदैव से स्वतन्त्र रहे
है। यही कारण है कि जितने दार्श-निक वाद और धार्मिक मत-पथ इस देश में प्रचलित हुए उतने अन्य किसी देश में नहीं हुए। बौद्धधर्म के
वैराग्य और ज्ञान-प्रधान
तथा तात्रिक क्रियाओ के अवशेष प्रभावो को लेकर यहाँ शैव और शाक्त-मतो का अनेक शाखा प्रशाखाओ में प्रचलन हुमा जैसे शैव, पाशुपत, कालादमन, कापालिक, कौल आदि। इन सम्प्रदायो मे बाहरी आचारो तथा वाह्य साधन क्रियाओ पर अधिक बल
दिया गया था। शैव और शाक्त मतो की प्रभाव-परम्परा में ईसा की तेरहवी शताब्दी में नाथ सम्प्रदाय
के अनेक पंथ प्रचलित हो गये थे जैसे- सिद्धमार्ग, योगमार्ग, अवधूतमत आदि। मत्स्येन्द्रनाथ (मछन्दरनाथ) और गोरखनाथ के द्वारा हठयोग की साघन क्रियाओ को इस युग में अधिक प्रचार
मिला । ईसा की ग्यारहवी शताब्दी मे, जो हिन्दी का शैशव काल था, वौद्धधर्म के निर्वासन के बाद शंकराचार्य के मायावाद, सन्यास, ज्ञान और योग के मागों का देश के धार्मिक क्षेत्र में इतना प्रचार हुआ कि
जनता लोक-जीवन
से उदासीन होने लगी। धर्म ने सामूहिक लोक-धर्म का रूप छोडकर व्यक्तिगत साधन का रूप धारण कर
लिया। संसार के व्यावहारिक पक्ष को छोडकर लोग परोक्ष के चिन्तन की ओर अग्रसर हुए।
अधिकारी साघको की देखा-देखी साधारण पुरुषार्थ और बुद्धि वाले लोग भी, जो बुद्धि के परिष्कार और ज्ञानयोग के साधन के लिए
बहुत अंश में अयोग्य थे, अपने को 'ब्रह्म' समझने लगे और परमतत्त्व को पहचानने का ढोग करने लगे।
इस प्रवृत्ति ने समाज में एक ओर तो दम्भ को जन्म दिया और दूसरी ओर देश में
अकर्मण्यता फैली। ईसा की ग्यारहवी शताब्दी से देश पर विदेशी आक्रमण भी आरम्भ हो
गये थे, जो आगे की कई शताब्दियों तक चलते रहे। उस समय देश छोटे-छोटे राज्यो में बँटा हुना था, कोई सगठित शक्ति न रह गई थी। आपस की फूट और व्यक्तिगत
मिथ्याभिमान में डूबे हुए भारतीयों को मुट्ठी भर बाहरी लोग रौंदते रहे। ऐसे समय
में बुद्धि की प्रखरता कुंठित हो गई। धर्म के दार्शनिक तत्त्व को समझने की क्षमता
भी कम हो गई और चित्त के निरोध के लिए लोगो में मानसिक वल भी क्षीण हो गया। उस समय
बुद्धि-प्रधान
और शारीरिक तथा मानसिक पुरुपायं के कष्टसाध्य धर्मों का प्रचार अपेक्षाकृत कठिन हो
गया। इसीलिए लोग उपासना के सरल और सहज मार्ग सगुण भक्ति की ओर उन्मुख हुए। देशी
राजसत्ता धीरे-धीरे
समाप्त होती जा रही थी, विदेशी धर्म का बलात् प्रसार होने लगा था। फलतः चारो ओर निराशा का
साम्राज्य छा गया था। लोग राज्य छिनने पर स्वधर्म और स्वसस्कृति के बचाने में लीन
थे। देवा में यातायात और विद्याप्रसार की कोई समुचित व्यवस्था न थी। स्थान-स्थान पर नये आचार्यों ने अपनी-अपनी विद्या-बुद्धि के अनुसार नये-नये धार्मिक पथों में लोगों को आश्रय देकर मानो समाज
के टूटते हुए बाँध को जगह-जगह रोका । विदेशी आक्रमण बहुधा पश्चिम की ओर से हुए थे इसलिए देश के
पच्छिमी भूभाग में धर्म-परिवर्तन के साथ राजनीतिक परिवर्तन अधिक हुए और पूर्वी भूभाग में धार्मिक
आन्दो लनो की प्रचुरता रही, क्योकि वहाँ बौद्धधर्म के हास के बाद अनेक धार्मिक मतवादो का प्रसार पहले
से ही चला आ रहा था। विदेशी धर्म के प्रहारो से बचने के लिए और भी बहुलता के साथ
धार्मिक मत खडे हो गए। चौदहवी तथा उसके बाद की दो शताब्दियों में भाकर तो पूरे
उत्तरी भारत में धार्मिक आन्दोलनो का प्रबल वेग हो गया ।
उपासना
मार्ग
भारतवर्ष में निवृत्ति के मुख्यत तीन मार्ग प्राचीन
काल से ही प्रचलित रहे है, ज्ञान-मार्ग, योगमार्ग तथा भक्ति-उपासना मार्ग । सास्य और योग के वैराग्य पूर्ण साधन
तथा हठयोग के कृच्छ-साध्य
अभ्यास एव निर्गुणोपासना का चिन्तन जब लोगो को अनुकूल न रह गए तब उन्होंने भक्ति
के सरल मार्ग को अपनाना आरम्भ किया। भक्ति का मार्ग इस देश के लिये नया नहीं था।
भागवत-धर्म-रूप में इसका प्रचलन उत्तरी भारत में बहुत प्राचीनकाल
से ही था। दक्षिणी भारत में भागवत धर्म की विद्यमानता आडवार भक्तो के तामिल गीतो
के रूप में मिलती है। यह मक्तिधारा ईसा की चौथी शताब्दी से दसवी शताब्दी तक
प्रवाहित होती रही । दक्षिण भारत के कुछ श्राचायों ने विष्णु-भक्ति की प्रेरणा उक्त आडवार गीतो से ली और वे भागवत
धर्म के प्रचार को उत्तरी भारत में ले आये और उसे उन्होने वहाँ पुनर्जीवित किया ।
इन आचार्यों ने आडवारो की उपासना भक्ति को शास्त्रीय रूप दिया। उन्होंने आडवार
भक्तो के गीत 'प्रवन्धम्' और ब्रह्म-सूत्र के मन्तव्य का समन्वय करने का प्रयास किया। उक्त आचार्यों में मुख्यत
चार प्राचार्य प्रसिद्ध है, श्रीरामानुजाचार्य, श्री विष्णुस्वामी, श्री निम्बार्काचार्य तथा श्री मध्वाचार्य। इन्होने शकराचार्य के मायावाद
का खंडन किया और जीव तथा जगत् की सत्यता तथा ईश्वर-भक्ति को पुन स्थापित किया। बारहवी शताब्दी से आगे की
तीन शता-ब्दियो
में उत्तरी भारत में भक्ति के भी अनेक पथ प्रचलित हुए। कुछ तो वैष्णव धान्दोलन के
फलस्वरूप पहले से ही चले था रहे थे और कुछ विदेशी धर्म के आघातो से बचने और कुछ
निराश्रित जनो की पीर हरने वाले भक्तवत्सल भगवान् हरि के आश्रय ग्रहण करने की
मनोवृत्ति से बने । इन चार वैष्णव सम्प्रदायो के अतिरिक्त प्रमुख भक्ति सम्प्रदाय
जिनका प्रचलन उत्तरी भारत में ईसा की सोलहवी शताब्दी के अन्त तक हो चुका था, ये थे-रामानन्दी सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय, चैतन्य अथवा गौडीय सम्प्रदाय, राधावल्लभीय सम्प्रदाय और हरिदासी सम्प्रदाय । उपासना का मार्ग मुख्यत दो
रूपो में प्रचलित हुआ, निर्गुण-ब्रह्मोपासना
तथा सगुण-ब्रह्मोपासना
। नाम, रूप और गुण के अभ्यस्त आर्त मनुष्यो को सगुण ब्रह्मोपासना में अधिक
सान्त्वना मिली। महात्मा सूरदास ने इस भाव को बड़े सुन्दर शब्दो में प्रगट किया है
कि "जिस
ब्रह्म की रूपरेखा और गुण नहीं है उसको मन का आलम्बन बनाना बढ़ा कठिन है। चंचल मन
अव्यक्त पर कही टिकता नही, चक्र की तरह भटकता है इसलिए मैं सगुण ब्रह्म की लीला का गान कर उसी की
उपासना करता हूँ।" 'रूप रेख गुन जाति जुगति विनु निरालम्ब मन चक्रित घावं, सव विधि अगम विचार्राह तातै सूर सगुण लीला पद गावै ।' महात्मा तुलसीदास ने भी यही भाव प्रगट किया है कि "जो व्यक्ति अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते
हैं वे करें, हम तो, हे प्रभु तुम्हारे सगुण रूप को जानते है और उसी का नित्य गान करते हैं।" सगुणोपासना के अन्तर्गत पाँच देवताओ की उपासना (पचोपासना) अधिक प्रसारित हुई-शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणेश । वैष्णव भाचार्यों ने विष्णु और उनके अवतारो की भक्ति को
अपनाया था ।वैष्णव धर्म के विभिन्न मतो में जहाँ दार्शनिकवाद का वैपम्य है वहाँ
आचार क्रियाश्रों में भी पार्थक्य है। परन्तु समान रूप से सब वैष्णव मतो ने सगुण
भक्ति को साधन रूप में अपनाया है। उनके सामान्य सिद्धान्तो को हम संक्षेप में इस
प्रकार व्यक्त कर सकते हैं-
१. ब्रह्म के सगुण रूप की ही विशेप मान्यता समान रूप से सभी वैष्णव सम्प्रदायो
में है, तथा विष्णु के अनेक अवतारो को मानते हुए भी राम और कृष्ण तथा उनकी परम
शक्तियो को सबने विशेष महत्त्व दिया है।
२. समान रूप से सब ने जीव और जगत् की सत्यता स्थापित की है और शंकराचार्य के
मायावाद का खंडन किया है।जीव और जगत् की सत्यता को उन्होने प्रकार-भेद से स्थापित किया है, इस दार्शनिक विभिन्नता के सूचक विभिन्न सम्प्रदायो के
नाम भी प्रचलित हुए हैं। जैसे विशिष्टाईत,शुद्धाद्वंत,द्वैताद्वत, द्व'त, अचिन्त्य भेदाभेद आदि ।
३. समान रूप से समस्त वैष्णव सम्प्रदायो मे भक्ति को साधन का मार्ग अंगीकार
किया गया है।
४. समन्वय की भावना वैष्णव धर्म की एक मुख्य विशेषता है।
वेद-संहिताएँ, उपनिषद्, ब्राह्मण, ब्रह्मसूत्र, गीता और भागवत पुराण वैष्णव धर्म में प्रमुख प्रमाण माने जाते हैं। परन्तु इतिहास-पुराण और लोक-प्रचलित विश्वासो का भी समावेश वैष्णवो ने अपनी-अपनी पद्धति में कर लिया है। उक्त प्रमाणो के
अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, हरिवश और ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मसूत्र और भागवत पर लिखे भाष्य, नारद भक्तिसूत्र, शाण्डिल्य भक्ति सूत्र तथा महाभारत का
नारायणीयोपाख्यान भक्ति-आन्दोलन के मुख्य आधार ग्रथ है। वैष्णव भक्ति-मार्ग ने शैव और शाक्त मतो के विभिन्न साम्प्रदायिक
विश्वास और उपासना-उपचारो
को रूपान्तरित कर अपने-अपने ढंग से अपना लिया है। ज्ञात होता है कि भोग-सुख को 'महासुख' का प्रतीक मानने की प्रवृत्ति वौद्ध तान्त्रिक मतो में पहले आई थी। कुछ समम
बाद, उन्ही मतो में लौकिक
स्त्री-पुरुप
की रति-क्रियाओ
के ऐन्द्रिय सुखों में मन की धान्तरिक तटस्थता और उसमे चित्त की चचल वृत्ति का
निरोध ढूंढा जाने लगा। धीरे-धीरे रति-भोग
को ही 'परम
सुख' का पूर्वरूप भौर उसका
माध्यम बना लिया गया और इस प्रकार काम-वासना आध्यात्मिक आनन्द का प्रतीक न रह कर परमानन्द-साधन की एक सीडी बना ली गई। तान्त्रिक बौद्ध मतो से
यह प्रवृत्ति शैव और शाक्तों में थाई और वहाँ भी धर्म की आड में काम-क्रीडा का रस-प्रसार खूब हुआ। वैष्णव भक्तो ने भी इस व्यापक भाव को
अपनाया परन्तु उसका परिष्कार करके उन्होने इसको ग्रहण किया। रतिमाव की भक्ति जिसे 'मधुर-भक्ति' कहा गया है वैष्णव भक्ति-साधन का एक मुख्य अग बन गई। भगवान आनन्द-स्वरूप हैं और सब प्रकार के मायो से वे भजनीय है, इस दृढ विश्वास को लेकर भक्ति-साधना के अनेक रूप प्रतित हो गये।
५. भक्ति-साधन
में मन के लोक-लिप्त-भाव और सम्बन्ध ही लोक से हटाकर ईश्वर में लगाने का
विधान है। इस साधन में ऐहिक सम्वन्धो को छोडना नहीं होता, उन्हें केवल ईश्वर की ओर मोडना होता है। इसी से भक्ति
का साधन सरल और सहज कहा गया है।
६ एक विशिष्टता वैष्णव धर्म की यह भी कही गई है कि
भक्ति के साधन में भक्त की जाति-पाति और कुल का कोई भेदभाव नही है। अनेक भक्त समाज की निम्न श्रेणी के हुए
हैं और अपनी साधना और सिद्धि से परम पूजनीय हो गए है। भक्ति-साधन का द्वार सव के लिये समान रूप से खुला है।
७. विश्वास, श्रद्धा, दैन्य, अकिंचनता और उपास्य ईश्वर की महत्ता तथा उसकी भक्त-वत्सलता भक्ति के ये आलम्बन तत्त्व सभी सम्प्रदायो
में समान रूप से मान्य रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि भत्ति-धर्म एक श्राशावादी धर्म के रूप में प्रवत्तित हुआ
था। इस साधन में मन के कोमल भावों के अतिरिक्त क्रूर भावो का भी समावेश है।
क्रूरकर्मा व्यक्ति भी क्रूर-भाव को ही भगवान को अर्पित कर मन का परिष्कार और नित्यसुख प्राप्त कर सकता
है। वैसे भगवान के प्रति प्रीति के चार भाव ही बहुधा भारतीयजनों ने अपनाये हैं।
दास्य प्रीतिभाव, सख्य प्रीतिभाव, वात्सल्य प्रीतिभाव तथा माधुर्यभाव अथवा कान्ताभाव । ईसवी चौदहवी शताब्दी
में स्वामी रामानन्द ने श्री रामानुजाचार्य के तात्त्विक सिद्धान्तो का अनुकरण कर
रामोपासना का एक स्वतन्त्र भक्ति मार्ग स्थापित किया। स्वामी रामानन्द जी के अनेक
शिष्य हुए परन्तु उनमें से लगभग सभी ने अपने अलग-अलग पथ स्थापित किये। इनमें कई शिष्यो ने स्वामी
रामानन्द की प्रेम-भक्ति
का रूपान्तरण कर उसमें नाथपथ की ज्ञान-योग की साधना सम्मिलित करली। उन्होंने भक्ति और ज्ञानयोग के सम्मिश्रण से
अध्यात्म्य के नवीन मार्ग चलाये। इन मार्गों में प्रेम-भक्ति का वह रूप नही है जो वैष्णव-भक्ति के विभिन्न सम्प्रदायो में है, फिर भी साधन-रूप में इन्होंने भी कुछ अश में भक्ति का स्वीकार
किया है। रामानन्द जी के शिष्यो में हिन्दी-भाषी ऐसे अनेक साधक हो गये हैं जिन्होने अव्यक्त और
निर्गुण ब्रह्म की उपासना मे ज्ञान और योग के साथ प्रेम-भक्ति का समावेश किया है। निर्गुण ब्रह्मोपासना के ये
नये पथ 'संतमत' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन सन्तो मे महात्मा कवीर, नानक और रैदास अधिक विख्यात है। इन्होने आध्यात्मिक
साधन के साथ व्यावहारिक जीवन के पारस्परिक सम्बन्ध और सदाचार की ओर भी ध्यान दिया
है और उस क्षेत्र में जनता को इन्होने नैतिक मर्यादा के उपदेश भी दिये हैं। आत्म-कल्याण के साथ समाज कल्याण भी इनका ध्येय रहा है।
रामानन्द की शिष्य-परम्परा
मे सगुण-भक्त
भी हुए है जिन्होने लोक-भाषा हिन्दी के द्वारा अपने विचार और भाव प्रकट किये हैं। भक्त-शिरोमणि तुलसीदास इसी परम्परा के रामोपासक महात्मा
थे। अयोध्या मे इस प्रकार के विभिन्न भावो को लेकर चलने वाले अनेक राम-भक्त महात्मा रहे हैं। विष्णु स्वामी, निम्बार्क, मध्त्र, वल्लभ, चैतन्य, हितहरिवश और हरिदास इन आचार्य और भक्तो के नाम से जो सम्प्रदाय उत्तरभारत
में प्रचलित हुए वे सब सगुणोपासक है तथा कृष्ण-भक्ति से सम्बद्ध है। विष्णुस्वामी म्प्रदाय की
परम्परा में श्री वल्लभाचार्य हुए जिन्होने ईसवी १६वी शताब्दी में माधुर्य-भक्ति का प्रचार किया। महाराष्ट्र में प्रचार पाने
वाला भागवतधर्म, जो पीछे वारकरी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का ही रूपान्तर बताया जाता
है। ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलोचन, एकनाथ, आदि महाराष्ट्र संत-भक्त वारकरी सम्प्रदाय से सम्बद्ध रहे थे। इन सभी महाराष्ट्र सतो ने हिन्दी
मे भी अपने भाव प्रकट किये हैं। सूरदास, परमानन्ददास, नन्ददास, नागरीदास श्रादि परममवत विष्णुस्वामी की वल्लभ-शाखा के अनुगामी थे। इनकी विविध भावमयी भक्ति-पूर्ण रचनाओ से हिन्दी-साहित्य सम्पन्न बना है। वल्लभ सम्प्रदाय का प्रसार
राजस्थान और गुजरात में अधिक हुआ। वहाँ के भक्तो ने भी अपने भाव हिन्दी मे प्रकट
किये हैं। प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई परम कृष्णभक्ता थी जिसकी रचनाओं में
सगुणभक्ति का निखरा हुआ रूप परिलक्षित होता है।
श्री वल्लभाचार्य के समकालीन भक्त चैतन्य महाप्रभु
थे। उनके द्वारा प्रवत्तित सम्प्रदाय 'गौडीय सम्प्रदाय अथवा चैतन्य सम्प्रदाय' कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के साधन में
कीर्तन प्रणाली को अधिक प्रश्रय दिया। इस सम्प्रदाय ने वगाल में विशेष प्रचार
पाया। वहा के अनेक बंगाली भक्त प्रसिद्ध हो गये हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी इस
सम्प्रदाय के प्रमुख प्रचारक थे जो अकबर बादशाह के शासनकाल मे वृन्दावन में वास
करते थे। श्री रूप गोस्वामीजी के तीन ग्रन्थ 'हरिभक्ति-रसामृत सिधु,' 'उज्जवल नीलमणि,' और 'लगुभागवतामृत' भक्ति-शास्त्र के प्रसिद्ध सस्कृत-ग्रन्थ है। गदाधर भट्ट और विठ्ठल रसिक इसी सम्प्रदाय के हिन्दी कवि और भक्त
थे। हरिदासी सम्प्रदाय के सस्थापक स्वामी हरिदास जी भी श्री वल्लभाचार्य और
सम्राट् अकबर के समकालीन परमभक्त थे। इनकी वाणी भक्ति-रस से सिक्त है। इन्होने आराध्य कृष्ण की सखीभाव से
उपासना की थी। विट्ठलविपुल और विहारिदेव सखी भाव के प्रसिद्ध भक्त कवि हुए है।
उक्त सम्प्रदायो का समकालीन राधाकृष्णभक्ति परक एक सम्प्रदाय राधावल्लभीय भी था
जिसके सस्थापक थी गोस्वामी हितहरिवशजी थे
जो स्वय एक सिद्ध भक्त और उच्च-कोटि के रससिद्ध कवि थे। भक्तप्रवर व्यासदेव और ध्रुवदास इस सम्प्रदाय के
प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं। राधावल्लभीय भक्तो ने भी ज्ञान और योग-मागों की अनुपयुक्तता बताकर, प्रेम-भक्ति का प्रसार किया। इस सम्प्रदाय में राधा-कृष्ण युगल की प्रेम और श्रानन्दमयी लीलाओ के ध्यान
और मनन को परमानन्द प्राप्ति का साघन बताया गया है। गोस्वामी हितहरिवश ने भी
माधुर्यभाव की प्रेम-भक्ति
का प्रचार किया, परन्तु इन्होने मधुरभाव को एक नवीन और विशेष उग से अपनाया। इस सम्प्रदाय
में आनन्द स्वरूप कृष्ण की रसशक्ति राधा की विशेष मान्यता है। भक्तमाल में
नाभादासजी ने इनके सिद्धात को स्पष्ट किया है भौर इस सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति को वडा कठिन बताया है। वे कहते हैं- “श्री राधाचरण प्रधान हुदै अति सुदृढ़ उपासी कुंज केलि
दम्पति तहां की फरत खवासी ।।“ “व्यास सुवन पथ अनुसर सोई भलि पहिचानि है, हरिवश गुसाई भजन की रोति सकृत कोई जानि है ।“ भक्तमाल राधा-कृष्ण दम्पति की माधुर्यभाव (पृगार) की भानन्द केलि का मनन करते हुए मानसिक वृत्ति को लौकिक कामभावना से बचाए
रखना वास्तव में वहा कठिन योग है। प्रियादास जी ने तो यहा तक कहा है कि 'हितू जू की प्रेम पद्धति को लाखो व्यक्तियो में से
कोई एक समझ सकता है।' नाभादास जी ने इस सम्प्रदाय का परिचय देते हुए कहा है कि इस पन्थ में
राधाचरण की भक्ति प्रधान है। राधा कृष्ण की भी आराध्या है। राधाकृष्ण के नित्य-विहार को सहचरी के रूप में देखना इस सम्प्रदाय का परम
लक्ष्य है। यद्यपि इस सम्प्रदाय में सयोग की भावना सदैव रहती है, क्षणभर को भी वियोग की स्वीकृति नही है फिर भी भक्त
अपने हृदय में सस्तीभाव से युगल के नित्य नूतन विग्रह और क्रीडाओं के दर्शन में
सदा अतृप्ति के भाव का अनुभव करता है। अन्य भक्ति-सम्प्रदायो के समान इस सम्प्रदाय में भी नवधाभक्ति को
साधन रूप में अपनाया गया है। सहचरी-भाव अन्य कृष्णभक्ति सम्प्रदायो में भी है परन्तु अन्य सम्प्रदायो में
भक्तात्मा सहचरी से उठकर भगवान् की कृपा द्वारा प्रियापद को प्राप्त करती है, जो भगवान् से भिन्न रहते हुए भी अभिन्न है। राधावल्लभ
सम्प्रदाय में आत्मा, सहचरी भाव से श्रागे, प्रियाभाव में जाने की अभिलाषा नही करती। उसे युगल केलि दर्शन में ही
परमानन्द प्राप्त होता है। भारतीय भक्ति-उपासना पद्धति के महत्त्वपूर्ण सम्प्रदायो में राधावल्लभ सम्प्रदाय की गणना
है। सूरदास, परमानन्द दास, नन्ददास, मीरा, हितहरिवश, सेवक, ध्रुवदास, व्यास विहारिनदास, विठ्ठलविपुल आदि कृष्णभक्तो ने भक्ति का कोई शास्त्रीय विवेचन नहीं किया ।
इन्होने, एक न एक सम्प्रदाय से बद्ध होते हुए भी, समान रूप से, भगवान् के प्रति अनन्य 'प्रेम' का प्रस्फुटन ही अपनी वाणी में किया है। उस वाणी में प्रेमानुभूति की विभोर
दशा का स्वाभाविक और सजीव चित्रण है। इनकी रचनाओ में सरसता, सरलता, भाषा-लालित्य
प्रौर स्वाभाबिक कलात्मकता है। काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से भी इन सम्प्रदायो का साहित्य अत्यधिक समृद्ध और
सम्पन्न है। लगभग १५ वर्ष पूर्व, जब मैंने हिन्दी के वल्लभ सम्प्रदायी वैष्णव-कवियो का अध्ययन किया था, और 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ लिखा था, उस समय मुझे अन्य वैष्णव सम्प्रदायो के हिन्दी कवियो के भी अध्ययन का अवसर
प्राप्त हुआ । 'अष्ट-छाप और वल्लभ सम्प्रदाय' नामक अपने ग्रन्थ मे मैंने विभिन्न कृष्ण-भक्ति परक वैष्णव सम्प्रदायो का सक्षिप्त विवरण उक्त
अध्ययन के फलस्वरूप दिया है। उसी समय से मेरी हार्दिक कामना थी कि में अथवा अन्य
कोई व्यक्ति वल्लभ सम्प्रदायी हिन्दी कवियो के समान ही, अन्य वैष्णव सम्प्रदायो के पृथक् पृथक् गम्भीर और
गवेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। अनेक कारणो से में इस कार्य को पूरा नही कर
पाया। मुझे अत्यधिक हर्ष है कि डा० विजयेन्द्र प्रेम' का प्रस्फुटन ही अपनी वाणी में किया है। उस वाणी में
प्रेमानुभूति की विभोर दशा का स्वाभाविक और सजीव चित्रण है।
इनकी रचनाओ में सरसता, सरलता, भापा-लालित्य
और स्वाभाविक कलात्मकता है। काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से भी इन सम्प्रदायो का साहित्य अत्यधिक समृद्ध और
सम्पन्न है। लगभग १५ वर्ष पूर्व, जब मैंने हिन्दी के वल्लभ सम्प्रदायी वैष्णव-कवियो का अध्ययन किया था, और 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ लिखा था, उस समय मुझे अन्य वैष्णव सम्प्रदायो के हिन्दी कवियो के भी अध्ययन का अवसर
प्राप्त हुआ । 'अष्ट-छाप और वल्लभ सम्प्रदाय' नामक अपने ग्रन्थ मे मैंने विभिन्न कृष्ण-भक्ति परक वैष्णव सम्प्रदायो का सक्षिप्त विवरण उक्त
अध्ययन के फलस्वरूप दिया है। उसी समय से मेरी हार्दिक कामना थी कि में अथवा अन्य
कोई व्यक्ति वल्लभ सम्प्रदायी हिन्दी कवियो के समान ही, अन्य वैष्णव सम्प्रदायो के पृथक् पृथक् गम्भीर और
गवेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। अनेक कारणो से में इस कार्य को पूरा नही कर
पाया। मुझे अत्यधिक हर्ष है कि डा० विजयेन्द्र स्नातक ने 'राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य' नामक प्रवन्ध मे, वैष्णव सम्प्रदायो में से एक सम्प्रदाय 'राधावल्लभीय' और उसके हिन्दी कवियो का सुन्दर अव्ययन प्रस्तुत कर
महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इस कार्य मे विद्वान् लेखक ने अपनी गहन विद्वत्ता, अध्ययनशीलता और गम्भीर परिश्रम का परिचय दिया है। 'राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य' ग्रन्थ दो भागो में विभक्त है। पूर्वाद्ध मे
सिद्धान्त पक्ष का विवेचन है और उत्तराद्ध मे उक्त सम्प्रदाय के प्रमुख कवियो और
उनके साहित्य का समीक्षात्मक मूल्याकन है। माधुर्य-भक्ति-निष्ठ इस वैष्णव सम्प्रदाय की सैद्धान्तिक तथा साहित्यिक दृष्टि से विवेचना
प्रस्तुत करने वाला यह पहला शोध-ग्रन्थ है। साम्प्रदायिक सिद्धान्तो के अध्ययम मे लेखक ने युक्ति, तर्क और प्रमाणो के साथ-साथ सम्प्रदाय की भावना का भी ध्यान रखा है। आरम्भ
में पृष्ठभूमि के रूप में विष्णु-भक्ति के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अध्याय मे
लेखक ने विविध सम्प्रदायो का जो वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत किया है वह, वास्तव मे, गहन अध्ययन और मौलिक चिन्तन का प्रतिफल है। लेखक का विचार है कि वैष्णव-भक्ति का प्रसार केवल चतु. सम्प्रदायो में ही आवद्ध नहीं है वरन् विष्णु के किसी
भी रूप की उपासना करने वाला भक्त वैष्णव है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, राधावल्लभ सम्प्रदाय माधुर्य भक्ति का पोपक सम्प्रदाय
है जिसकी साधना में प्रेम या हित तत्त्व की प्रधानता है। वल्लभाचार्य और गोस्वामी
विठ्ठलनाथ जी की भाँति गोस्वामी हितहरिवश ने भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही मधुर-भक्ति की साघन-प्रणाली चलाई थी। निष्काम कर्म और भगवत्त-हित की भावनाओ से पूर्ण इस रसिक सम्प्रदाय की साधन
प्रणाली ने, कठिन होते हुए भी, बहुत मान पाया। इसमे परम सुख की कल्पना 'नित्यविहार' के रूप में की गई है। डा० स्नातक ने 'नित्यविहार' के दार्शनिक रूप को समझा है और उसका गम्भीर विवेचन किया है। नित्यविहार के
विधायक अग राधा, कृष्ण, सहचरी और वृन्दावन का पहली बार विशद-व्यापक वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। कुछ विद्वानो ने
इस सम्प्रदाय की दार्शनिक विचार प्रणाली को, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि वादो के समान 'सिद्धाद्वैत' नाम दिया है। वस्तुतः आचार्य हितहरिवंश जी ने न तो
किसी प्रकार के दार्शनिक मतवाद की स्थापना की थी और न उसका नामकरण ही किया था। इस
विषय का भी विद्वान् लेखक ने प्रस्तुत ग्रन्थ में गम्भीर एव प्रामाणिक विवेचन किया
है। ग्रथ का उत्तरार्द्ध, जैसा कि पीछे कहा गया है, साहित्यिक आलोचना की दृष्टि से लिखा गया है। लेखक ने राधावल्लभ सम्प्रदाय
के केवल दस प्रमुख कवियो का विवरण दिया है। इस दिशा में भी लेखक की मौलिक देन है।
खोज के साथ कवियो का सम्पूर्ण चारित्रिक परिचय और उनके काव्य का सर्वांगीण विवेचन
है। अनेक कवि ऐसे भी प्रकाश में लाये गये हैं जिनका उल्लेख हिन्दी के इतिहास-प्रथो में नहीं है। प्रस्तुत ग्रथ पर श्री स्नातक जी
को पी-एच०
डी० की उपाधि मिली है, जिसके वे सर्वथा अधिकारी है। सफलता के लिए वे मेरी बधाई के पात्र हैं। डा०
स्नातक की लेखनी से इसी प्रकार के अन्य महत्त्वपूर्ण और गवेषणात्मक ग्रन्थों का
सृजन होगा, यह मेरी शुभ कामना है।
भक्ति का उद्भव
भक्ति का उद्भव भगवद् भक्ति वैष्णव धर्म की आधार शिला
है। ब्रह्म-साक्षात्कार, ईश्वर-प्राप्ति, विष्णु-सान्निध्य
तथा परम-पुरुपार्थ-सिद्धि आदि विभिन्न नामो से व्यवहृत 'साध्यतत्व' का भवन वैष्णव धर्म मे भक्ति की नीव पर ही प्रतिष्ठित है। वैदिक ऋचाओ से
लेकर मध्ययुगीन भक्त महानुभावो द्वारा रचित 'वाणी ग्रन्थो' तक भक्ति के क्रमिक विकास का अनुशीलन करने पर यही
निष्कर्ष निकलता है कि कर्म, ज्ञान और उपासना नाम से जिन तीन मार्गो का निर्देश वैदिक वाड्मय मे हुआ है, उनका पर्यवसान वैष्णव धर्म मे भक्ति-मार्ग में हुआ। मानव जीवन के चरम लक्ष्य 'परम पुरुषार्थ-सिद्धि' के लिए उपर्युक्त तीनो मार्गो के समन्वय पर वैदिक साहित्य मे पर्याप्त वल
दिया गया है। यह समन्वय बुद्धि ही वाद मे भक्ति-पथ को प्रशस्त करने में सहायक हुई। पुराण तथा भक्ति
सूत्रो के प्रणयन काल में तो 'परम पुरुषार्थ-सिद्धि' का तात्पर्य 'भगवत्-कृपा-प्राप्ति' ही समझा जाने लगा और इसीलिए भगवद् भक्ति को पुरुषार्थ
के भीतर परिगणित किया गया। ज्ञान, कर्म और उपासना मार्ग की दुरूह एव कष्टसाध्य साधना को त्यागकर श्रवण, कीर्तन, दैन्य, आत्मनिवेदन आदि के सुगम माध्यम से वैष्णव भक्त ने भगवान् के समीप पहुँचने
का पथ खोज निकाला, फलत भक्ति का सोपान मध्ययुग में अपेक्षाकृत अधिक आदरणीय समझा जाने लगा।
प्रेमलक्षणा भक्ति को स्वीकार करने वाले सम्प्रदायो में तो प्रेम को ही साध्य एव
साधन समझ लिया गया। भक्ति का यह चरम उत्कर्ष जिस क्रमिक विकास-परम्परा में हुआ उसका अनुशीलन इस तथ्य का द्योतक है
कि उपासना मार्ग ही परवर्ती युग में भक्ति मार्ग बना । भक्ति के उद्भव और विकास-क्रम के सम्वन्ध में पर्याप्त मतभेद होने पर भी यह
प्रामा-णिक
रूप से कहा जा सकता है कि आस्तिक भाव से ईश्वरोपासना करने वाले आर्यों मे भक्ति के
मूल बीज विद्यमान थे और आशिक रूप से भक्ति के विविध रूपो का आभास उन्हे वैदिक काल
में ही मिल गया था।
राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य
ऋचाओ का सामजस्य स्वीकार न करने वाले अनेक पाश्चात्य
विद्वानो ने भक्ति को अभार-तीय तत्व सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। पाश्चात्य विद्वान् वेवर, कीथ और ग्रियर्सन ने इसे ईसाई धर्म की देन कहा है।
वेवर महोदय कृष्ण की भगवान् के रूप में कल्पना का श्रेय क्राइस्ट को देते हैं और
ग्रियर्सन महाशय का मत है कि प्राचीन काल में ईसाइयो की एक बस्ती मद्रास प्रान्त
मे थी, उन्ही के प्रभाव से हिन्दुथो मे भक्ति-मार्ग आया और बाद में दक्षिण भारत से समस्त भारतवर्ष
में फैल गया। इसी प्रकार प्रो० विलसन ने भक्ति को अर्वाचीन युग की उपज कहकर यह
सिद्ध करना चाहा है कि त्रिभिन्न सम्प्रदायो के गुरुयो ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए
इसका प्रचार किया। उक्त मान्यताओ के पीछे भारतीय भक्ति-परम्परा के क्रमिक विकास को न समझना तया स्वधर्म (ईसाई) का उत्कर्ष सिद्ध करने का आग्रह मात्र है। यह सत्य है कि वैदिक काल में
अनुराग-परक
भक्ति का वह रूप प्रकाश मे नही झाया था जो मध्ययुग मे अथवा पौराणिक काल में व्यापक
रूप से स्वीकार किया गया, किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि उस युग में भक्ति की कल्पना तक नही
हुई थी। विभिन्न देवताओ की स्तुति-प्रार्थना के लिए जो मार्मिक अभिव्यक्तियाँ उस काल में प्रस्तुत की गई
उनमें भक्ति के लिए अनिवार्य राग-तत्व का अभाव नही कहा जा सकता । वेवर महोदय ने तो कृष्ण जन्माष्टमी पर्व और
महाभारत में वर्णित श्वेत-द्वीप वर्णन को भी ईसाई धर्म की देन ठहराया है। वे द्वीप शब्द से समुद्र
पार स्थित योरोप देश समझते है। श्री राय चौधरी ने अपने ग्रथ 'अर्ली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट' में इन भ्रान्तियो का निराकरण किया है। इसके सिवा
वेसनगर (भेलसा) के शिलालेख द्वारा भी भक्ति का ईसा से दो शताब्दी
पूर्व होना सिद्ध होता है। जिन कल्पित तथ्यो के आधार पर भक्ति को अभारतीय और
अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया उनका परवर्ती विद्वानो ने खडन किया है।
इस निमूल भ्रान्त धारणा का कारण वैदिक साहित्य का एकागी अध्ययन या अज्ञान ही कहा
जा सकता है। भारतीय विद्वान् श्री बालगगाधर तिलक तथा श्री कृष्ण स्वामी आयगर ने
उक्त मान्यता का सप्रमाण खडन करते हुए भक्ति को वैदिक युग से ही वीज रूप में
स्वीकार किया है। भक्ति एव भागवत धर्म के सम्बन्ध मे इतने पुष्कल प्रमाण उपलब्ध
होते हैं कि उनकी अवहेलना करके भक्ति को अभारतीय तत्व बताने का साहस आज कोई निष्पक्ष
विद्वान् नही करेगा। हम यहाँ इस विवाद मे न उलझकर विष्णु-भक्ति के क्रमिक विकास का सकेत मात्र प्रस्तुत करना
चाहते हैं। विष्णु-भक्ति
के विविध रूप ही वैष्णव-भक्ति-सम्प्रदायो
के आधार हैं अत: उनके प्रारम्भिक रूप का यदि यत्किचित् भी सधान हो
सके तो परवर्ती भक्ति-पद्धति
का वैज्ञानिक अनुशीलन सम्भव होगा ।
वेद में भक्ति
वेद सहिता और ब्राह्मण ग्रथो मे प्रत्यक्ष रूप से
अनुराग-सूचक
भक्ति शब्द का प्रयोग नही हुआ और भक्ति शब्द द्वारा साक्षात् उपासना का लक्ष्य भी
नही कराया गया, किन्तु उस काल में भक्ति की कल्पना भी नही हुई थी यह मानना भक्ति-परक अभिव्यक्तियो की अवहेलना करना है। वेद और
ब्राह्मण ग्रन्थो मे कर्मकाण्ड की प्रधानता होने पर भी जिस प्रकार ज्ञान-काड का विकास स्पष्ट परिलक्षित होता है वैसे ही ज्ञान
के बाद भक्ति की परम्परा का भी सधान ऋचाओ के आधार पर सम्भव है। यदि वैदिक साहित्य
मे भक्ति-तत्त्व
के बीज सन्निहित न होते तो उनके श्रकुरित होकर पल्लवित और पुष्पित होने का सुयोग
परवर्ती काल मे कैसे सम्भव होता। भक्ति के शास्त्रीय रूप के स्थिर होने पर जिस
नवधा-भक्ति
की स्थापना हुई उसके श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आत्मनिवेदन आदि अगो के सकेत हमें वेदमत्रो में अनेक स्वलो पर मिलते हैं।
वेद प्रतिपादित भक्ति भावना को वैष्णवीय भक्ति से किस प्रकार सयुक्त किया जाय और
वेद को वैष्णवधर्म का आधार किस प्रकार माना जाय यही इस प्रसग में विवेच्य है।
हमारी यह मान्यता है कि वैदिक देवता इन्द्र के प्रति उस काल में अवश्य ही स्निग्ध
और राग पूर्ण धारणा रही थी जिसके परिणाम स्वरूप इन्द्र को माता पिता आदि के
सम्बोधनो से व्यवहृत करके भक्ति के मूल तत्व को वेद में स्वीकार किया गया ।
वेदमत्रो में भक्ति के अवयवो को खोज निकालने का जैसा प्रयत्न वर्त्तमान युग में हो
रहा है उसे सर्वतोभावेन स्वीकार न करते हुए भी मूल रूप से श्रवण, कीर्तन आदि की भावना को हमें मत्रो मे स्वीकार करना
ही होगा। शाडिल्य ने अपने भक्ति सूत्र में 'भक्ति' प्रमेया श्रुतिम्य' (१-२-६) द्वारा वेदो की ओर स्पष्ट सकेत किया है। "भारतीय भक्ति सम्प्रदाय का आदि स्रोत ऋग्वेद है। यहाँ
कुछ मत्रो में आदमी और देवता के बीच गाढे प्रेम और मित्रता की कल्पना की गई है।" विविध देवी-देवताओ की पूजा-अर्चा का विधान भी एक ही देवता अर्थात् ईश्वर की भक्ति का ही विधान है ऐसा
आज सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। एक ही ईश्वर या सत् को विद्वान् लोग इन्द्र, मित्र, वरुण या अग्नि के नाम से पुकारते हैं, वही सुन्दर पखो वाला दिव्य गरुड भी है। उसी एक पदार्थ
का वर्णन वे अनेक प्रकार से करते हैं इसलिए वही एकमात्र सत् (सृष्टि को आविर्भाव करने के कारण, अग्नि (ससृत्ति एव परिवर्तन का मूल कारण होने पर कारण) यम (अखिल विश्व का आधारभूत होने से) तथा मातरिश्वा भी कहलाता है। भक्ति-भावना के द्धमूल होने के लिए भक्त की एक ही ओर गति
होना आवश्यक है। अनेक मे भी एक को खोज लेना भक्त की स्वाभाविक विशेषता है। अत वेद
में ऐसे अनेक मंत्र उपलब्ध होते हैं जिनमें एक ही देवता मे अपनी भावना को लीन करने
का वर्णन किया गया है। वैदिक उपासना मार्ग मे भक्ति-तत्वो का विकास हुआ था और इसीलिए भक्ति का सबसे पहला
रूप सहिता भाग की उन ऋचाओ मे है जिनमे ईश्वर का श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 'व्यानयोग' के लिए विधान किया गया है। प्रसिद्ध सस्कृतज्ञ पाश्चात्य विद्वान् कीथ के
अनुसार भक्ति की वैष्णवानुमोदित भावना का आविर्भाव आर्यो के आध्यात्मिक एव
दार्शनिक विचारो में अधिक गभीरता आने पर बाद मे हुआ और तभी वह प्रारम्भिक श्रद्धा
वा उपासना से विकसित होती हुई क्रमश उपास्य भगवान् के ऐश्वर्य वा मूलतत्व मे भाग
लेना (भज्
भाग लेना) आदि व्यक्त करने वाले अधिक व्यापक भाव मे परिणत हुई। कीथ का यह विचार केवल
अनुमानाश्रित है। इसके लिए उन्होने अकाट्य तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नही किया ।२ अत. भक्ति के मूल बीज का पता हमें वेद से ही मानना चाहिए
। वैदिक काल में उपास्य देवताओ के नामो की इयत्ता नही है। अनेक नामो से एक ही
ईश्वर की पूजा-अर्चा
का विधान है ऐमा ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध मत्र 'एकमद्विप्रा बहुधा' आदि द्वारा हमने सकेतित किया है। किन्तु वैष्णव धर्म
की दृष्टि से हमे श्रनेक देवताओ के होने पर भी विष्णु पदवाच्य देवता पर विचार करना
है। उपासना क्षेत्र मे विष्णु शब्द देवता के अर्थ में कब से प्रयुक्त होना
प्रारम्भ हुआ और किस प्रकार यह वैदिक विष्णु देवता ही परवर्ती पुराण तथा भक्ति
साहित्य मे लीलावतारी विष्णु बन गया। वैदिक विष्णु और पौराणिक कृष्ण के
श्रृखलावद्ध क्रमिक रूप का संधान कठिन है किन्तु जितनी कडियाँ उपलब्ध है हम उनका
सकेत प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे ।
वेद में विष्णु
ऋग्वेद में विष्णु शब्द का प्रयोग अनेकार्थ और विपुल
है किन्तु उसकी एक विशेषता यह है कि वह सर्वत्र एक दिव्य, महान् और व्यापक शक्ति का प्रतीक है। यदि उसे
ग्रादित्य वाचक मानकर प्रयोग में लाया गया है तब भी वह तीन पगो में अखिल ब्रह्माड
को लाघ जाता है। उसके दो पग जो पृथ्वी और अन्तरिक्ष मे पडते हैं मनुष्य देख पाता
है, शेष तीसरे पग का
पराक्रम उसे भी विदित नही होता। तृतीय पग विष्णु का परम पद है जिसे विद्वान् लोग
आकाश की ओर सदा ऊँची दृष्टि लगाकर देखा करते हैं। इस प्रकार विष्णु को कही 'ऋतस्य गर्भम्' कहा है तो कही 'यज्ञोहर्वं विष्णु' कहकर स्वय यज्ञ ही स्थिर किया है उपासना के प्रसग के
आये हुए वेदमन्त्रो में विष्णु को लोकरक्षक के रूप में समस्त ईश्वरीय गुणो से
समन्वित कहा है। विष्णु का वर्णन वेद में इन्द्र के सहायक देवता के रूप में भहुआ
है और इन दोनो के पराक्रम का वर्णन एक साथ समान भाव से भी किया गया है विष्णु के
विविध रूपो का वर्णन जे० गोडा नामक विद्वान् ने अपने शोध ग्रंथ 'एस्पैक्टस् ऑब् अर्ली विष्णुइज्म' में विस्तारपूर्वक किया है। इस ग्रंथ की मान्यताओ को
यदि विष्णु विकास का आधार स्वीकार कर लिया जाय तो वैदिक विष्णु ही परवर्ती काल का
देवता विष्णु सिद्ध हो सकता है। सहिता के वाद ब्राह्मणकाल में विष्णु का वर्णन
बढता हुआ दृष्टिगत होता है और विष्णु की शक्ति का भी उत्तरोत्तर विकास ब्राह्मण
ग्रन्थो में वर्णित किया गया है। शतपथ् ब्राह्मण मे यज्ञ-निष्ठा की दृष्टि से विष्णु को अग्रणी ठहराया गया है
और विष्णु के अलौकिक दिव्य शक्तिपूर्ण चमत्कारो का भी कथा के रूप में वर्णन मिलता
है। ब्राह्मण ग्रथो में विष्ण की व्यापकता इस बात का निदर्शन है कि देवताओ में
इन्द्र की जैसी प्रधानता ऋचाओ में थी वैसी ही प्रधानता शनै शनै विष्णु को प्राप्त
होना प्रारम्भ हो गई थी एक प्रकार से इन्द्र का स्थान विष्णु ने ग्रहण करना
प्रारम्भ कर दिया था। विष्णु शब्द के देवता अभिधान का यह क्रमिक विकास ही समझता
चाहिए। कुछ विद्वानो ने तो विष्णु के अवतारो की सूचना भी ब्राह्मण ग्रथो में ढूंढ
निकाली है।
उपनिषद् और भक्ति
वैदिक ऋचाओ मे किसी एक मार्ग की वरेण्यता न होकर
ज्ञान, कर्म और उपासना तीनो के सामंजस्य पर वल देने का स्पष्ट कारण ऋपियों की
समन्वय-बुद्धि
है। सासारिक कार्य-कलाप
को ध्यान में रखकर जिस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति का पारस्परिक तारतम्य
निर्धारित करके उनके त्याग और ग्रहण का विधान है, उसी प्रकार इन तीनो मार्गों के सापेक्षिक महत्व को
हृदयगम करके, स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है। ब्राह्मणकाल मे याज्ञिक अनुष्ठानो का
प्राधान्य होने से कर्मकाड का अपेक्षाकृत अधिक विकास और विस्तार हुआ । ज्ञान और
उपासना की उपेक्षा होने से उपनिषद् एव आरण्यको मे ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई और ज्ञान-मार्ग से ब्रह्म के समीप बैठने (उपनिषद्) का उपक्रम किया गया। ब्रह्म-सान्निध्य के लिए ज्ञान की उपादेयता स्वीकार करते हुए भी ऋषियो को भक्ति की
अनिवार्यता प्रतीत हुई और श्वेताश्वतर उपनिषद् में सर्वप्रथम देव (प्रभु) और गुरु की भक्ति का महत्व बताते हुए उन्होने कहा-
“यस्य वेवे परा भक्ति र्यथा देवे तथा गुरो ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः ॥
“ श्वेताश्वतरोपनिषद् ६-२३ ।
उपनिपकालीन ऋषियो को ज्ञान-मार्ग का अनुसरण करते हुए भी यह विदित हो गया था कि मानव जीवन का उद्देश्य
ऐसी ज्ञान-प्राप्ति
नही जो केवल गहन दार्शनिक अनुभूति पर आश्रित रहकर जीवन को राग के स्पन्दन से
नितान्त विहीन बना दे। उत्कट प्रेम और ज्ञान के द्वारा ही दिव्य आनन्द की प्राप्ति
सम्भव है। इसीलिए कदाचित् वृहदारण्यक के 'मधु-विज्ञान' प्रकरण मे तथा छान्दोग्य उपनिषद् मे उपासना के अगो मे भक्ति तत्व को स्थान
देकर उन्होने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। यथार्थ में, ब्रह्म की सूक्ष्म और निर्गुण कल्पना को सगुण-व्यक्त-प्रतीक के रूप प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न में ही विष्णु, श्रीकृष्ण, वासुदेव, नारायण आदि की भक्ति या पासना-पद्धति प्रतित हुई। काल-क्रम की दृष्टि से वाद में निर्मित हुई उपनिषदो मे इस पासना (भक्ति) का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है।
वैदिक वाङ्मय में विष्णु के विविध रूप
वैदिक काल
में जिस रूप में भक्ति का विकास हो रहा था उसमें हृदय-पक्ष को शनै-नि प्रधानता मिलनी प्रारम्भ हुई और बुद्धिवादी ज्ञान-प्रधान तार्किक उपासना को गौणता मलने लगी। हृदय-पक्ष की प्रधानता होने पर विष्णु नामक देवता की पूजा-अर्चा वढी और ही प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित
हुआ। उपनिषद् काल में विष्णु के परमधाम को विर्वोच्च स्थान माना गया और जगत्-पालक के रूप मे विष्णु की कल्पना की गई। विष्णु ज
वर्णन जिस रूप मे सहिताओ में हुया था उसे और अधिक तेजस्वी, उर्जस्वी एव भास्वर नाकर प्रस्तुत किया जाने लगा। जो
विशेषण पहले इन्द्र के लिये प्रयुक्त होते थे वे ही प्रमन विष्णु की प्रगना में
काम आने लगे। 'विष्णु
के निःशय, बानुदेव, युष्मी पति, वृषण, प्रषभ, वैनु छ, यूहब्स प्रादि नाम जैने पट्ने इन्द्र के लिए प्रपूरन होने थे प्रथवा इन्द्र-नम्बन्धी रिसी यत्तु को गृमृचिन ने थे, धीरे-धीरे विष्णु के पर्ने नामी एत्र उपाधियों का प्राधार बन गये। विष्णु या
यत्र माहात्म्य एस यात या प्रमाण है कि भविन की दृष्टि ने अन्य देवी-देवताषो पी अपेक्षा विष्णु के नाम घोर्गिक और
परिपूर्ण नमभा गया था। धिग्णु शब्दको निक्ति घोर निर्वनन करने ममय विष्णु की
व्यापाना का ध्यान गतत बना गगहा । यानाने प्ररने मे विष्णु शब्द की निरविन इन
प्रशार कोरे प्रथ यद गिविनो भनि भनिदिनेोनेर्दा ।' श्री दुर्गाचार्य श निर्देचन इम प्रयमभिविना व्यालो
भनि न्यानोनि वा रश्मि-भिन्चनयंम् । तश विष्णुदिन्यो भनि। गाने मे जो नमन्न गरावर जगत् वो व्याप्न
पन्ना है वही दिले 'मेदेरिटप्नोनिगर
जगत् विष्णु सुगत्ति विष्णु-माहात्म्य प्रतिपादन रे लिए पर्यान्न। वैष्णव धर्म के मूल में निष्कामना
प्रधानजना व्यापक विग्नार निदियो में भलित क्षेत्र हावा अधिगमान्निम्मी सामना ने, उगे प्रथिरुश दश्यापिंग में पान जाने ही रात्रमा मे
दिए नगवार भावना नागयगण (विष्णु) यको रुप में हुई। उन रिपनको घोर प्राचार्य रामनन्द्र गुग्न ने ग्राने 'भरित या नितास' नीदा निरंध में नदिया। मागमण के ग्प में भी विष्णु की
उनना का विधान वैश्मगाव धर्म में है। नर के घयन ता घन्निम नध्य नागया है। मेद में
सुष्टि निर्माण की कया के प्रमग में नारायण कामोन मित्रता। मनुग्मृति मे नागयगण
शब्द की व्युत्पत्ति करने हुए बताया गया
'आपो नग इति प्रोक्ता श्रापो वै नर मूनय. ।
ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायण स्मृत ।।'
- मनुस्मृति ८० १ ब्लोक १०
महाभाग्न
में नारायण रूप में विष्णुरा वर्णन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना है। नारायण और
विष्णु दोनों का अदात्म्य म्प ने यहाँ नामोर नेय हुआ है। नारायण की मलाह ने ही
गमुद्र-मंथन
किया गया ऐमा भी वर्गान है।" विष्णु के विविध रूपो का युग है कि उमती रचना महाभारत और पुराणो के चाद
हुई। भक्ति-मार्ग
के प्रतिशदक नारद भक्तिनून एवं माटिल्य भक्तिभूय तो बाद की रचना है। यह गीना के
श्लोको ने विद्ध होना है जो उन नक्ति-मूयो में उदाहन किये गये हैं। अतएव भागवत धर्म का विशद उल्लेन हमें महाभारत
के नागयणीयोपारयान में ही मानना होगा । ने यानुदेव-भक्ति वा तान्विक निरुपण महाभारत हसन में ही न्वीतार
चौर वामुदेव का ऐवत्र भी महाभारन के गान्नि पर्व में बड़े व्यक्त शब्दों में
म्बोवार किया गया है। विष्णु को ही वामुदेव ताम्प मानते हुए गहने हैं-
'सर्वेषाम। श्रयो विष्णश्वर्य विधिमास्थितः ।
सर्वभूनकृनानामो वासुदेवेति चोच्यते ॥
महाभारत, गान्तिपर्व २० २४७ दलो० ६४
पुराणों में भक्ति तत्त्व
वैष्णव धर्म का वर्तमान म्प पुराणो द्वारा प्रतिपादित
और ममर्पित होकर ही सार्व जनीन बना है। पुराणो तो रचना ने पूर्ण वैष्णय धर्म का
मूक्ष्म म्प ही प्राग में आया पा जिने पौराणिक कथानक, धान्यान, घरंशद, विनियोग और व्याम्या द्वारा स्पष्ट बोर व्यापतन्य प्राप्त हुया। महाभारत
में पुराण महिमा वर्णन करते हुए एरु दचोक श्राना है जिनमें पहा गया है कि
श्रष्टादग पुराणों में धत्रण में जो फन होना है यह वैष्णव को हो प्राप्त होता है।
यहाँ वैष्णव शब्द म्पष्ट रूप मे व्यवहृन हूया है। यह श्लोक पुराणो की रनना के
पश्चान् महाभारत में बाद में जोडा गया समभा जाता है निन्नु वैष्णवो के लिये
पुराग्ण माहात्म्य बाद वे प्रायः सभी ग्रत्रो में वर्णिन हुया है। आज के पौराणिक
जगत् में तो श्री मद्भागवत यो वेद के नमका आप्त प्रमाण समभ्न जाना है। पुराणो के
तत्वार्थ पर ही विकमिन होटर वैष्णय भक्ति अपनी प्रौटावस्था तक पहुँची। महाभारत और
गीता की रचना के बाद भी भगवान् की महिमा या आम्यान शेप रह गया था जिसे पुराणो
द्वारा पूर्ण किया गया । देर्वाप नान्द ने महाभारत के विपय मे अपने विचार व्यक्त
करते हुये यही कहा है कि धर्मादि चनुष्टय की व्याग्या हो जाने पर भी भगवद्-महिमा का निरूपण दरोप रहता है। यह महिमा ही वैष्णव
धर्म या भागवत धर्म का प्राण है अत व्यासजी को नारद ने पुराण प्रणयन में प्रवृत्त
किया। इस पौराणिक श्राख्यान का तात्पर्य पुराणो का महत्व प्रदर्शन मात्र है। मानव-धर्म के धारयान की दृष्टि में महाभारत की महत्ता
सर्वविदित है। राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य सात्वत विधिमास्याय
प्राक्सूर्यमुख नि सूतम् ।
' पूजयामास देवेश तच्छेषेण पितामहान् ।।'
'नारायण पर सत्यमृत नारायणात्मकम् ।
नारायणपरो धर्म पुनरावृत्ति दुर्लभः ।।'
प्रवृत्ति लक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मकः
नारायणात्मको गधो भूमौ श्रेष्ठतम स्मृतः ।"२
पाचरात्रविदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मन ।
प्रायण भगवत्प्रोक्त भुञ्जते वाऽप्रभोजनम् ॥"3
भागवत धर्म के विषय में महाभारत मे कया थाती है कि
इसे धर्म को नारद ने स्वय नारायण से ग्रहण किया था। वासुदेव शब्द का भक्ति के
क्षेत्र में प्रामाणिक रूप से प्रयोग बताने के लिए श्री भडारकर, लोकमान्य तिलक, डा० राय चौधरी आदि विद्वानो ने पाणिनि के व्याकरण
सूत्रो का प्रमाण प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर ईसा से सात शताब्दी पहले
वासुदेव पूजा प्रचलित थी यह स्थिर किया है। किन्तु वासुदेव भक्ति का विकसित रूप
हमें महाभारत से ही मानना चाहिये। भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के विषय में
भागवत पुराण के प्रारम्भ मे एक कथा आती है जिसमें कहा गया है कि जब व्यासजी ने
देखा कि महाभारत और गीता में नैष्कर्म्य प्रधान भागवत धर्म का जो प्रति-पादन किया गया है उसमें भक्ति का यथार्थ रूप नहीं
निखर पाया और भक्ति के बिना कोरा नैष्कर्म्य शोभा नहीं देता तब उन्होने नारद को
बुलाकर अपने मन का उद्वेग कहा तथा उसी की पूति के निमित्त भक्ति-प्रधान भागवत पुराण की रचना की। इस कथा से यह ध्वनि
स्पष्ट निकलती है कि भागवत पुराण से पहले वैष्णव धर्म में गृहीत उपासना मार्ग
नैष्कम्यं प्रधान था, उसमें भक्ति पक्ष की स्थिति सन्तोपजनक न होने से परवर्ती काल में भक्ति-प्रधान पुराण का निर्माण किया गया। वैष्णव धर्म में
समादत नारद पंचरात्र ग्रन्थ भी भक्ति-मार्ग की स्थापना के लिए बाद में ही लिखा गया। पचरात्र मे गीता, महाभारत, भागवत तया ब्रह्मवैवर्त, पुराण आदि का स्थान-स्थान पर उल्लेख भी इस बात का प्रमाण है कि उसकी रचना महाभारत और पुराणो के
बाद हुई। भक्ति-मार्ग
के प्रतिपादक नारद भक्तिसूत्र एवं शाडिल्य भक्तिसूत्र तो वाद की रचना है। यह गीता
के श्लोको से सिद्ध होता है जो उन भक्ति-मूत्रो मे उदाहृत किये गये हैं। अतएव भागवत धर्म का विशद उल्लेख हमे
महाभारत के नारायणीयोपाख्यान मे ही मानना होगा। प० रामचन्द्र शुक्ल ने वासुदेव-भक्ति का तात्विक निरूपण महाभारत काल से ही स्वीकार
किया है। विष्णु और वासुदेव का ऐक्य भी महाभारत के शान्ति पर्व मे वडे व्यक्त
शब्दो मे स्वीकार किया गया है। विप्णु को ही वासुदेव का रूप मानते हुए कहते हैं-
'सर्वेषामाश्रयो विष्णरैश्वर्य वित्रिमास्थितः ।
सर्वभूनकृतावासो वासुदेवेति चोच्यते ॥
महाभारत, शान्तिपर्व श्र० ३४७ श्लो० ६४
पुराणों में भक्ति तत्त्व
वैष्णव धर्म का वर्तमान रूप पुराणो द्वारा प्रतिपादित
और सर्मार्थत होकर ही सार्व-जनीन वना है। पुराणों की रचना से पूर्ण वैष्णव धर्म का सूक्ष्म रूप ही
प्रकाश में आया था जिसे पौराणिक कथानक, आख्यान, धयंवाद, विनियोग और व्याख्या द्वारा स्पष्ट और व्यापक रूप प्राप्त हुआ। महाभारत में
पुराण महिमा वर्णन करते हुए एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि श्रष्टादश
पुराणो मे श्रवण से जो फल होता है वह वैष्णव को ही प्राप्त होता है। यहाँ वैष्णव
शब्द स्पष्ट रूप से व्यवहृत हुआ है। यह श्लोक पुराणो की रचना के पश्चात् महाभारत
में वाद में जोडा गया समझा जाता है किन्तु वैष्णवो के लिये पुराण माहात्म्य बाद के
प्राय सभी ग्रथो में वणित हुआ है। आज के पौराणिक जगत् मे तो श्री मद्भागवत को वेद
के समकक्ष श्राप्त प्रमाण समझा जाता है। पुराणो के तत्वार्थ पर ही विकसित होकर
वैष्णव भक्ति अपनी प्रौढावस्था तक पहुँची। महाभारत और गीता की रचना के बाद भी
भगवान् की महिमा का आख्यान शेप रह गया था जिसे पुराणो द्वारा पूर्ण किया गया।
देवर्षि नारद ने महाभारत के विषय मे अपने विचार व्यक्त करते हुये यही कहा है कि
धर्मादि चतुष्टय की व्याख्या हो जाने पर भी भगवद्-महिमा का निरूपण शेष रहता है। यह महिमा ही वैष्णव
धर्म या भागवत धर्म का प्राण है अत व्यासजी को नारद ने पुराण प्रणयन मे प्रवृत्त
किया। इस पौराणिक आख्यान का तात्पर्य पुराणो का महत्व प्रदर्शन मात्र है। मानव-धर्म के आख्यान की दृष्टि से महाभारत की महत्ता
सर्वविदित है ।
सात्त्वतं विधिमास्थाय प्राश्सूर्यमुख नि सूतम् ।'
पूजयामास देवेश तच्छेषेण पितामहान् ।।१
'नारायण पर सत्यमृत नारायणात्मकम् ।
नारायणपरो धर्म पुनरावृत्ति दुर्लभ ।।'
प्रवृत्ति लक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मक'
नारायणात्मको गधो भूमौ श्रेष्ठतम स्मृतः ।"
पांचरात्रविदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मन ।
प्रायण भगवत्प्रोक्त भुञ्जते वाऽग्रभोजनम् ॥"3
भागवत धर्म के विषय में महाभारत में कया आती है कि इस
धर्म को नारद ने स्वय नारायण से ग्रहण किया था। वासुदेव शब्द का भक्ति के क्षेत्र
में प्रामाणिक रूप से प्रयोग बताने के लिए श्री भडारकर, लोकमान्य तिलक, डा० राय चौधरी आदि विद्वानो ने पाणिनि के व्याकरण
सूत्रो का प्रमाण प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर ईसा से सात शताब्दी पहले
वासुदेव पूजा प्रचलित थी यह स्थिर किया है। किन्तु वासुदेव भक्ति का विकसित रूप
हमें महाभारत से ही मानना चाहिये। भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के विषय में
भागवत पुराण के प्रारम्भ में एक कथा आती है जिसमें कहा गया है कि जब व्यासजी ने
देखा कि महाभारत और गीता मे नैष्कर्म्स प्रधान भागवत धर्म का जो प्रति-पादन किया गया है उसमें भक्ति का यथार्थ रूप नही निखर
पाया और भक्ति के बिना कोरा नैष्कर्म्य शोभा नही देता तब उन्होने नारद को बुलाकर
अपने मन का उद्वेग कहा तथा उसी की पूति के निमित्त भक्ति-प्रधान भागवत पुराण की रचना की। इस कथा से यह ध्वनि
स्पष्ट निकलती है कि भागवत पुराण से पहले वैष्णव धर्म मे गृहीत उपासना मार्ग
नैष्कर्म्य प्रधान था, उसमें भक्ति पक्ष की स्थिति सन्तोपजनक न होने से परवर्ती काल मे भक्ति-प्रधान पुराण का निर्माण किया गया। वैष्णव धर्म में
समादूत नारद पचरात्र ग्रन्य भी भक्ति-मार्ग की स्थापना के लिए वाद में ही लिखा गया। पचरात्र में गीता, महाभारत, भागवत तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि का स्थान-स्थान पर उल्लेख भी इस बात का प्रमाण इसी पुराण मे
राधा शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ दिया गया है। राधा के स्वरूप के विषय में हमने
आगे पंचम अध्याय में विस्तार से लिखा है। भागवत पुराण तो भक्ति-शास्त्र का सबसे वडा भडार है जहाँ वैष्णव धर्म में
स्वीकृत भक्ति का शास्त्रीय रूप उपलब्ध होता है। साहित्य की दृष्टि से भी भागवत
पुराण की प्रतिष्ठा अत्यधिक है। भागवत पुराण का रचना-काल से ही जो सम्मान हुआ वह इस बात का प्रमाण है कि
भक्ति मार्ग का उन्मेप हो जाने पर भी वह इस पुराण के प्रकाश मे ही प्रशस्त हो सका।
प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करने वाले आचार्यों मे से कुछ ने भागवत पुराण पर भी टीका
लिखी और भक्ति सम्प्रदाय मे इस ग्रन्थ का श्रुति के समान सम्मान किया। आज तो
वर्तमान वैष्णव-धर्म
की स्थापना का इसे आधार ही माना जाने लगा है। भागवत पुराण की टीकायो की भी सवसे
लवी व खला है जो इसके महत्व को प्रदर्शित करती है। मत्स्य कूर्म, वराह तया वामन पुराण का तो नाम ही विष्णु के अवतारो
से सयुक्त है यत यह स्पष्ट सिद्ध है कि विप्णु के अवतार की भावना का सर्वांगीण
विकास पुराण काल मे ही हुआ और उसके अवतारी रूप में लौकिक-अलौकिक, सव प्रकार के शक्ति, शील और सौन्दर्य आदि गुणो की प्रतिष्ठा हुई ।
पुराणो मे कृष्णभक्ति
श्रीकृष्ण-चरित्र के माधुर्य-पक्ष का सविस्तर वर्णन प्रस्तुत करके पुराण साहित्य ने भक्ति-क्षेत्र में कृष्णावतार को इतना अधिक व्यापक और
आकर्षक बना दिया कि भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में जहाँ भक्ति की लहर पहुँची कृष्ण
के माधुर्य परिपूर्ण चरित्र की पूजा-अर्चा प्रारम्भ हुई। श्रीकृष्ण लीलामो का वर्णन भी पुराणो द्वारा ही अधिक
प्रचारित हो सका । महाभारत में वर्णित श्रीकृष्ण-चरित्र मे ऐश्वयं-पक्ष का ही प्राधान्य था, पुराणो ने उसे माधुर्य मडित करके भक्तजनो के लिए
आस्वाद्य बनाया। नवधा भक्ति के समस्त रूपो का सोदा-हरण वर्णन करके भक्ति को सर्वसाधारण के लिए सुलभ
वनाने में भी पुराणो का अभित योग है। सख्य और वात्सल्य के साथ शृङ्गार को भक्ति के
क्षेत्र में, पुराणो मे उन्नयन करके रखा गया। शृगार का माधुर्य के योग से जो उन्नयन हुआ
वह परवर्ती भक्ति-सम्प्रदायो
का मेरुदड बना। भागवत पुराण में रति-भाव की प्रतिष्ठा करके तथा लौकिक कालुष्य का परिहार करके जो रसमयी भूमिका
तैयार की गई वही भक्ति-सम्प्रदायो की भाघार-भूमि मानी गई। श्रीकृष्ण की विभिन्न रसमयी लीलाओ का भौतिक और श्राध्यात्मिक
स्वरूप भी पुराणो ने ही स्थिर किया और श्रीकृष्ण को इतना दिव्य और साथ ही साथ
लीलावतारी परमेश्वर बनाया कि लौकिक प्रेम का उसकी लीलाओ में स्वाभाविक रूप से
अन्तर्भाव हो सका । राधा और कृष्ण के स्वरूप, लोला तथा पारस्परिक सम्वन्ध के विषय में वैष्णव
सम्प्रदायो में जो मान्यताएँ प्रचलित हैं उनका आधार प्राय ब्रह्म वैवर्त, हरिवश तथा भागवत पुराण है। राधा और कृष्ण के वैवाहिक
सम्वन्ध का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है और इसी पुराण मे राधा शब्द की
व्युत्पत्ति एवं अर्थ दिया गया है। राधा के स्वरूप के विषय में हमने आगे पचम
अध्याय में विस्तार से लिखा है। भागवत पुराण तो भक्ति-शास्त्र का सबसे वडा भडार है जहाँ वैष्णव धर्म मे
स्वीकृत भक्ति का शास्त्रीय रूप उपलब्ध होता है। साहित्य की दृष्टि से भी भागवत
पुराण की प्रतिष्ठा अत्यधिक है। भागवत पुराण का रचना-काल से ही जो सम्मान हुआ वह इस वात का प्रमाण है कि
भक्ति-मार्ग
का उन्मेप हो जाने पर भी वह इस पुराण के प्रकाण में ही प्रशस्त हो सका। प्रस्थान
त्रयी पर भाष्य करने वाले आचार्यों मे से कुछ ने भागवत पुराण पर भी टीका लिखी और
भक्ति सम्प्रदाय मे इस गन्थ का श्रुति के समान सम्मान किया। आज तो वर्तमान वैष्णव-धर्म की स्थापना का इसे आधार ही माना जाने लगा है।
भागवत पुराण की टीकाओ की भी सवसे लवी पृ खला है जो इसके महत्त्व को प्रदर्शित करती
है। मत्स्य कूर्म, वराह तथा वामन पुराण का तो नाम ही विष्णु के अवतारो से सयुक्त है अत यह
स्पष्ट सिद्ध है कि विप्णु के अवतार की भावना का सर्वागीण विकास पुराण काल में ही
हुआ और उसके अवतारी रूप में लौकिक-प्रलौकिक,सब
प्रकार के शक्ति,शील
और सौन्दर्य आदि गुणो की प्रतिष्ठा हुई । वैष्णव धर्म के विकास और प्रसार में
पुराणो का सर्वाधिक योगदान रहा है। वैष्णव सम्प्रदायो के प्रवर्तन में जिन
सिद्धान्तो को स्वीकार किया गया उनमे से अधिकाश का आधार पुराण साहित्य ही है।
उदाहरणार्थ चतु सम्प्रदाय के अतिरिक्त श्रीकृष्ण चैतन्य का गौडीय सम्प्रदाय, श्री वल्लभाचार्य का वल्लभ सम्प्रदाय या पुष्टिमार्ग, और श्री हितहरिवश का राधावल्लभ सम्प्रदाय मुख्यत
श्रीमद्भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण मे प्रतिपादित भक्ति पद्धति और राधा-कृष्ण स्वरूप को लेकर आगे बढे है। अत. वैष्णव सम्प्रदायो के विभिन्न रूपो की सीम-मर्यादा की परीक्षा के लिए भी पुराणो का अवगाहन
नितान्त आवश्यक हो जाता है। भागवत पुराण मे भक्ति का प्रतिपादन करते हुए जिन
आधारभूत तत्वो का उल्लेख हुआ है वे ही वैष्णव धर्म के भी आधार है। इस पुराण में
व्यवहार पक्ष मे भक्ति को ही स्वीकार किया गया है। भगवान् को सगुण और साकार सिद्ध
करते हुए उसके चार रूप स्थिर किये गये हैं। पहला स्वरूप तो पुरुप नाम से व्यवहृत
होता है। उसके तीन रूप विशिष्ट गुणो के धारण करने पर होते हैं जिन्हे विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र नाम से पुकारा जाता है। विष्णु का
वर्णन पुराणो में विस्तार से हुआ है। इसी प्रकार भगवान् की शक्ति का वर्णन है, तथा सृष्टि वर्णन के साथ जीव और माया का स्वरूप बताया
गया है। दार्शनिक दृष्टि से भागवत पुराण इतना प्रौढ है कि उसके आध्यात्मिक पक्ष को
अद्वैतादि मतवादो की कसौटी पर भली भाति कसा जा सकता है। साधन पक्ष मे पुराणो में
भक्ति का प्रतिपादन है और उसे ज्ञान, कर्म, उपासना आदि से भी वढकर बताया गया है। भक्ति में भी प्रेमाभक्ति की
उत्कृष्टता कही गई है और यही वैष्णव धर्म की व्यापकता का कारण है। भक्ति की
उत्कृष्टता बताते हुए यहाँ तक कह दिया है कि सच्चे भक्त भगवान् द्वारा प्रदत्त
मुक्ति की भी भक्ति की तुलना में कामना नहीं करते क्योकि भक्ति का आनन्द मुक्ति से
कही बढकर है-
'न किचित् साधवो धीरा झक्ता ह्य कान्तिनो मम ।
वांछन्त्यपि मया दत्त कैवल्यमपुनर्भवम् ।।'
भागवतपुराण ११ । २० । ३४
सक्षेप में, वैष्णव धर्म के स्वरूपाख्यान मे पुराणो का अत्यधिक महत्व है अत यह मानना
असगत न होगा कि वैष्णव धर्म का परवर्ती विधान पुराण साहित्य पर ही भाघृत है धौर
इसी कारण प्रस्थानत्रयी से भी अधिक पुराणो का सम्मान होता है। राधा-कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करने वाले सम्प्रदायो मे
तो पुराणो में स्वीकृत लीलावतारी कृष्ण थौर ह्लादिनी शक्ति राधा की स्थापना है।
पुराणो के भक्ति-क्षेत्र
में इतने महत्वपूर्ण होने पर यह तात्पर्य कदापि नही निकालना चाहिए कि पुराण काल
में भक्ति का उदय और विकास हुआ। यथार्थ में भक्ति की प्राचीन परम्परा को पुराणो
द्वारा व्यापक रूप मिला।
भक्तिसूत्रों में भक्ति-तत्व
मुनिवर शाडिल्य और देवर्षि नारद विरचित भक्ति-सूत्रो का वैष्णव भक्ति के स्वरूप निरूपण में बडा
महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय मनीषा की अभिव्यक्ति मे सक्षिप्तता, गहनता और प्रौढता की दृष्टि से सूत्र-पद्धति को उस समय स्थान मिला होगा जब विस्तारपूर्वक
व्या-ख्यात्मक
शैली से प्रतिपाद्य वस्तु की विवेचना हो चुकी होगी। दार्शनिक क्षेत्र मे सूत्र
पद्धति की उपयोगिता सर्वविदित है। गृह्य सूत्र और व्याकरण सूत्रो की महत्ता तो
उनके व्यापक उपयोग से ही लक्षित होती है। भक्ति-क्षेत्र में शाडिल्य ने जब सूत्र निर्मित किये तव
भक्ति का व्याख्यात्मक प्रतिपादन अवश्य हो चुका था। गीता, महाभारत और पुराण इसके प्रमाण है। इन ग्रन्थो के सार
को सूत्रो में समाविष्ट करने के निमित्त यह सूत्र रचना हुई या स्वतन्त्र रूप से
भक्ति-सिद्धान्त
की स्थापना के लिए नूतन शैली को स्वीकार किया गया, यह प्रश्न विचारणीय है। भक्ति सिद्धान्त की स्थापना
मे शाडिल्य के सूत्र परम्परानुगत मर्यादा का अनुसरण करने पर भी कुछ नवीन तत्त्वो
की ओर भी इगित कराते हैं। उदाहरणार्थ गीता मे प्रतिपादित कर्ममार्ग की अपेक्षा तथा
दार्शनिक ग्रन्थो में स्थापित ज्ञानमार्ग की अपेक्षा इन सूत्रो में भक्ति का अधिक
महत्व बताया गया। सबसे बडी बात शाडिल्य ने यह बताई कि भक्तिपथ सभी भक्तो के लिए
समान रूप से प्रशस्त है। निम्न वर्ण (जाति) के साधक भी इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। दूसरी बात ज्ञान और कर्म मार्ग
से बढकर यह कही कि जब तक भक्ति का उदय नही होता तव तक आत्मा जन्म-मरण के चक्र मे घूमती रहती है, भवित का उदय होने के बाद पूर्णता के साथ उसमे
निमज्जित होने पर ही भवचक्र का वधन कटता है। शाडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध
रागात्मिका वृत्ति है। शुद्ध राग के अन्तर्गत हरि स्मरण, कीर्तन आदि को नही गिना जाता। शाडिल्य ने भवित के
स्पष्ट दो भेद किये हैं-प्रथम अपरा भक्ति है जो साधनावस्था में रहती है, दूसरी शुद्ध भावभूमिज पराभक्ति है।२ जव साधक आनन्द की
अन्तिम स्थिति में होता है तब वह पराभक्ति की स्थिति में पहुँचता है। नारद-भक्ति-सूत्रो में जो भक्ति उपदिष्ट की गई है वह भावुकता तथा भावोद्रेक की दृष्टि
से शाडिल्य से अधिक परिपूर्ण है। नारद ने भी अन्य साधना-मार्गों की अपेक्षा भक्ति की उत्कृष्टता स्पष्ट रूप
से स्थापित की है। हार्दिक पक्ष की प्रधानता और प्रेम पर आश्रित होने से इस भक्ति
को प्रेमाभक्ति सज्ञा भी दी गई है। नारद के भक्तिसूत्रों ने प्रचार की दृष्टि से
अधिक सम्मान पाया और ये सूत्र भक्तजन की श्रद्धा के कारण 'सप्तम दर्शन' माने गये। चौरासी सूत्रो के लघु कलेवर में भक्ति सागर
को नावद्ध करना नारद-ऋषि
के लिये ही सम्भव था। दक्षिण भारत के आलवार भक्तो की भक्ति-पद्धति से नारद की भक्ति में बहुत कुछ साम्य है।
इसलिए कुछ विद्वानो ने भक्ति का प्राचीन उत्स दक्षिण में ही स्वीकार किया है।
वैष्णवधर्म के विविध रूप और
विष्णु-भक्ति
जैसा
कि हम पहले लिख चुके है कि वैष्णव घर्म का प्रारम्भिक रूप हमें विष्णु-पूजा
के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक नारायणीय,
सात्वत
एव पचरात्र घर्म की शाखाओ में दृष्टिगत होता है। इनमें भक्ति का स्पष्ट उल्लेख होने
से भक्ति मार्ग का यथाविधि प्रवर्त्तन इन्हीं से मानना उचित होगा। काल निर्धारण के
लिए हम डाक्टर कूलर का अभिमत स्वीकार कर सकते हैं जिसमें उन्होने भागवत,
सात्वत
और पचरात्र सम्प्रदाय को नारायण उपासना या देवकी पुत्र कृष्ण की उपासना का सम्प्रदाय
कहा है और जिसका काल जैन धर्म के प्रारम्भ होने से बहुत पहले ईसा पूर्व आठवी शताब्दी
ठहराया है। पालि साहित्य के प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् सेनार्ट ने भी यह मत प्रकट किया
है कि विष्णु-भक्ति
के तत्वो तथा कथानको को बौद्ध साहित्य में ग्रहण किया गया है। भागवत धर्म की स्थापना
बुद्ध जन्म के बहुत पहले हो चुकी थी। विष्णु पूजा के सम्वन्ध में अंग्रेज लेखक वार्थ
का अभिमत है कि यह बहुत प्राचीन है। बुद्ध के पूर्व यह विद्यमान थी किन्तु वे इसके
उद्भव के सम्बन्ध में स्पष्ट सकेत प्रस्तुत नही कर सके। वृक्ष,
सर्पादि
पूजा से बहुत पहले विष्णु-भक्ति
की स्थापना हो चुकी थी, इस
तथ्य को स्वीकार करने के बाद विष्णुपूजा का सीथियन मूल उद्भव स्वीकार करना सर्वथा भ्रममूलक
है। भागवत धर्म मे नारायणीय सम्प्रदाय का वर्णन महाभारत के शान्तिपर्व मे है जहाँ लम्वे
कथानक की अवतारणा करके इस धर्म को दिव्य धर्म के रूप में वर्णित किया है। उसके बाद
श्वेत द्वीप में नारद को भगवान का दर्शन होता है और वे नारद को अपने
'वासुदेव-धर्म'
का
रूप समझाते हैं। शाति पर्व का यह प्रकरण आध्यात्मिक दृष्टि से भी मननीय है।
3 इसका हमने संकेत भी किया है। इस अध्याय मे परमात्मा
को वासुदेव, जीवन
को सकर्षण, मन
को प्रद्युम्न तथा अहकार को अनिरुद्ध वताया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से वासुदेव स्वयं
श्रीकृष्ण है। संकर्षण उनके ज्येष्ठ भ्राता वलराम है,
प्रद्युम्न
और अनिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र हैं। वासुदेव शब्द का प्रयोग सहिता या ब्राह्मण भाग
में नही है। हाँ, तैत्तरीय
आरण्यक के दसवें प्रपाठक मे यह शब्द एक स्थल पर विष्णु के पर्यायवाची के रूप मे ही
आया है। किन्तु इस आरण्यक को कई विद्वानो ने वाद की रचना ठहराया है। डाक्टर कीथ के
अनुसार यह थारण्यक ईसा-पूर्व
तीसरी शताब्दी में लिखा गया, तब
तक विष्णु और वासुदेव की एकता स्वीकृत हो चुकी थी । वासुदेव शब्द का महाभारत में सूर्य-परक
अर्थ किया गया है और "वृष्णियो
मे वासुदेव हूँ" ऐसा
भी कहा गया है। वासुदेव शब्द वौद्ध-साहित्य
के घटजातक में भी आया है और उसे मथुरा प्रदेश के उत्तरी भाग में रहने वाले किसी राजवश
की सतति कहा गया है। ...
विष्णु और वासुदेव
वासुदेव पूजा को स्वीकार करने वाला द्वितीय सात्त्वत
धर्म वैष्णव भावना का सम-र्थक और संस्थापक धर्म है। इस धर्म के मुख्य उपास्यदेव वासुदेव (कृष्ण) थे। कहते है वासुदेव ही इस धर्म के प्रवर्त्तक भी है। डा० भाडारकर का
अनुमान है कि 'वासुदेव' भक्ति-सम्प्रदाय के प्रवत्तक का नाम था और उनके प्रसग का अभिप्राय यही जान पडता
है कि वह अन्य तीनो (संकर्पण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध) के साथ किसी पहले युग मे भी वर्तमान रहा माधुर्यभाव
की भक्ति को स्वीकार करने वाले मध्ययुगीन सम्प्रदायो में व्रजमडल के चार प्रमुख
सम्प्रदाय थे जो प्राय. समकालीन है। किन्तु उन सबकी माधुर्य भावना मे थोडा-बहुत अन्तर अवश्य है। श्री वल्लभाचार्य ने अपने
सम्प्रदाय के प्रवर्तन के समय माधुर्य भाव के वात्सल्य पक्ष को सर्वश्रेष्ठ मानकर
अगीकार किया था किन्तु शनै. शनं उसमें परि-वर्तन
आया और वह माधुर्य के कान्ताभाव की ओर झुकता गया। गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने तो
कान्ताभाव को पूरी तरह अपनाया और उनकी इस स्वीकृति का प्रभाव अप्टछाप के कवियो की
रचनाओ पर पडा। उन्होने स्वयं भी 'शृङ्गार मडनम्' लिखकर दाम्पत्य भाव-पोपक भक्ति को श्रेष्ठतर मान लिया था। यद्यपि गुमाईजी इस पद्धति को अति
गोप्य या केवल रसिक जनो के लिए ही ग्राह्य मानते थे। उन्होने स्वय कहा है कि जो
भक्तजन रसमार्ग से अनभिज्ञ है वे इस ग्रन्थ का अवलोकन न करें। डा० दीनदयालु गुप्त
ने अपने 'अष्टछाप
और वल्लभ सम्प्रदाय' नामक ग्रंथ में युगल स्वरूप (दाम्पत्यभाव) की उपासना विधि का सकेत देते हुए लिखा है- 'वल्लभाचार्य जी ने पहले माहात्म्य ज्ञान पूर्वक वात्सल्य-भक्ति का ही प्रचार किया था। वाद को उन्होने अपने
उत्तर जीवन काल में तथा उनके उत्तराधिकारी गो० विठ्ठलनाथ जी ने किशोर-कृष्ण की युगल-लीलाओ का तथा युगल स्वरूप की उपासना विधि का भी
समावेश अपनी भक्ति-पद्धति
में कर लिया ।' सूरदास, नन्ददास तथा परमानन्ददास की रचनाओ मे इस कोटि के माधुर्य भाव-परक पदो का समावेश भी उत्तरकाल मे ही हुआ। उस समय
भक्ति-क्षेत्र
में व्रज प्रदेश पूर्ण रूप से कान्ता-भाव की भक्ति का समर्थक हो गया था । इसी समय वगाल में चैतन्य ने माधुर्यभाव
से कृष्णोपासना प्रारभ की किन्तु उस उपासना का चरम उत्कर्ष व्रज में ही दृष्टिगत
हुआ। चैतन्य प्रतिपादित कीर्तन और नाम-स्मरण की प्रणाली को माधुर्य के उज्ज्वल पक्ष से सयुक्त करके दाम्पत्यभाव
की सुदृढ़ भूमि पर स्थित करने का श्रेय रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को है। इन
महानुभावो ने वृन्दावन को अपनी साधना स्थली बनाया और उज्ज्वल रस को शास्त्रीय रूप
देने के निमित्त सस्कृत भाषा में शास्त्रीय ग्रयो का प्रणयन किया। यथार्य में
कान्ताभाव को भक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप देने का श्रेय इन्ही महानुभावो को है। यह
ठीक है कि इनकी भावना में परकीया को प्रधानता मिली और परकीया के रूप में दाम्पत्य
का एक मोहक रूप इन्होंने अपने ग्रथो में प्रस्तुत किया। किन्तु जिस परकीया भाव को
प्रारभ में सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया वही कालान्तर विभिन्न वैष्णव भक्ति-सम्प्रदायो को वर्तमान युग में 'चतु सम्प्रदाय' के अन्तर्गत परि-गणित करने की परिपाटी इतनी अधिक प्रचलित है कि
प्रत्येक सप्रदाय के आचार्य या उनके अनुयायी अपने नवीन दार्शनिक सिद्धात, मन्तव्य तथा अभिनव साघन मार्ग होने पर भी चतु
सप्रदायो में कही न कही अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रयत्नशील देखे जाते हैं।
यदि कोई आचार्य अपने सप्रदाय को स्वतत्र मानकर उसके पार्यक्य पर बल देता है तो उसे
चतु सप्रदाय वाले वैष्णव स्वीकार करना नहीं चाहते। फलत विवश होकर सर्वथा नवीन होने
पर भी उसे पुरातन सीमाओ में अपना स्थान बनाने को बाध्य होना पडता है। अनेक वैष्णव
भक्त आचार्यों के समक्ष चतु सम्प्रदाय की यह सकीणं चार दीवारी आ खडी हुई है और
अधिकाश ने इच्छा या अनिच्छा से इसे स्वीकार करके अपने को वैष्णव समाज में शामिल
किया है। किंतु आश्चर्य का विषय है कि विद्वानो ने 'चतु सम्प्रदाय' की प्राचीनता और वैष्णव कहलाने की अनिवार्यता पर आज
तक गम्भीरतापूर्वक विचार नही किया। राधावल्लभसम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य
हितहरिवश जी के समक्ष जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ तो उन्होने निर्भयतापूर्वक अपने
सम्प्रदाय को सर्वथा स्वतत्र वैष्णव सम्प्रदाय कहा। चतु सम्प्रदाय के भीतर कही भी
अन्तर्भाव करने का मोह उन्हे अपनी ओर आकृष्ट न कर सका । चतु सम्प्रदाय के अन्तर्गत
होकर वैष्णव सम्प्रदाय कहलाने की अनिवार्य शर्तों पर भी आपने ध्यान नही दिया और
विधि निषेष से अतीत विधान (प्रीतिरीति) प्रस्तुत कर अपना स्वतत्र सम्प्रदाय स्थापित किया जो विगत सवा चार सौ
वर्षों से निरन्तर घाभिक समाज में सब प्रकार स्वीकृत और समाहत वैष्णव भक्ति-सम्प्रदाय के रूप मे प्रतिष्ठित है। यथार्थ में चतु
सम्प्रदाय की भावना जिस कल्लित आधार पर अवस्थित है उसे भली-भाति हृदयगम न करने के कारण ही विशाल और व्यापक
वैष्णव धर्म को चतु सम्प्रदाय की सकीर्ण सीमा में आवद्ध करने की अघ परपरा चली आ
रही है। दक्षिण और बगाल चतु सम्प्रदाय के प्रलोभन में पडकर किसी के साथ सयुक्त
होना नितान्त अनिवार्य शतं नही है। इस सम्प्रदाय में गौरागमहाप्रभु नाम से चैतन्य
को ईश्वर के अवतार के रूप में ही माना जाता है।अवतारी पुरुप किसी सामान्य व्यक्ति
का अनुयायी नही होता अत चैतन्य महाप्रभु का सम्प्रदाय स्वतन्त्र ही माना जाना
चाहिए विष्णु
स्वामी सम्प्रदाय और वल्लभ सम्प्रदाय
रुद्र सम्प्रदाय के अन्तर्गत विष्णुस्वामी सम्प्रदाय
पर भी इसी दृष्टि से विचार करना हम आवश्यक समझते हैं। विष्णुस्वामी के उद्भव काल
का अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। कुछ विद्वानो की सम्मति में उनका जन्म दसवी
शताब्दी में हुआ और कुछ विद्वान् नाभा जी के भक्तमाल के छप्पय के आधार पर तेरहवी
शताब्दी से पहले का बताते है। नाभा जी का छप्पय किसी ऐतिहासिक साक्ष्य पर आघृत न
होने से जन्म सवत् आदि की दृष्टि से प्रमाण रूप में गृहीत नही हो सकता। केवल
श्रद्धाभाव से ही उसमें कतिपय धनुश्रुतियो को लेकर ज्ञानदेव को विष्णुस्वामी का शिष्य
कहा गया है। मराठी 'सन्तलीलामृत' पुस्तक में ज्ञानदेव को निवृत्तिनाथ का शिष्य कहा गया
है। कुछ सायणाचार्य या विद्याशंकर को ही विष्णुस्वामी ठहराते हैं। कुछ विद्वानो की
सम्मति में श्रीधरस्वामी विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के अनुगत थे और उन्होने अपनी टीका
में विष्णुस्वामी के सिद्धान्तो का आभास दिया है। किन्तु यह सब कल्पनामात्र है, इसका कोई पुष्ट आधार नही मिलता । इतिहास में अव तक
तीन व्यक्ति विष्णुस्वामी नाम से विख्यात है (१) देवतनु विप्णुस्वामी, (२) रामगोपाल विष्णुस्वामी और (३) वल्लभाचार्य के गुरु विष्णुस्वामी। फलत यह निर्णय करना कठिन है कि किस
विष्णुस्वामी ने सम्प्रदाय प्रवत्तित किया। वर्तमान युग में विष्णु स्वामी
सम्प्रदाय के अनुयायियो की सख्या अति न्यून है और साम्प्रदायिक दृष्टि से
साहित्यिक सामग्री का भी पूर्णत अभाव है। जो कुछ ग्रथ उपलब्ध होते हैं वे भी
असदिग्ध रूप से विष्णुस्वामी रचित प्रतीत नही होते । विष्णुस्वामी कब, किस स्थान पर रहे और उन्होंने अपने सम्प्रदाय के
सिद्धान्तो के प्रचार के लिए मठ-मन्दिर स्थापित किये इसका भी कही उल्लेख नही मिलता। फर्कु हर ने
विष्णुस्वामी के दो मठो की चर्चा की है जिनमें से एक काकरौली में और दूसरा कामवन
में है।' कामवन के मठ का विष्णुस्वामी से अभी तक सीधा सम्बन्ध नही माना जाता है।२
वल्लभ सम्प्रदाय के ग्रथो से तथा किम्वदन्तियो से यह पता चलता है कि श्री
वल्लभाचार्य जी विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर बैठे और उन्होने इस
सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को निर्धारित किया। यह भी जनश्रुति है कि महाराष्ट्र सन्त
श्री ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलोचन, हीरालाल और श्रीराम विष्णुस्वामी मतावलम्बी थे। महाराष्ट्र मे प्रचार पाने
वाला भागवत धर्म जो पीछे वारकरी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके
अनुयायी ज्ञानदेव, नामदेव आदि प्रसिद्ध भक्त हुए, विष्णुस्वामी मत का ही रूपान्तर है। यह निर्णय डा० गुप्त ने केवल जनश्रुति
के आधार पर ही निकाला है। इसका कोई ऐतिहासिक आधार प्रतीत नही होता, उन्होने स्वय यही स्वीकार किया है। विष्णुस्वामी के
नाम से अनेक रचनाएँ विख्यात है किन्तु 'सर्वज्ञसूक्त' नामक ग्रथ को ही प्रमाणकोटि में रखा जाता है। उनका प्रस्थानत्रयी पर भाष्य
नही मिलता। यदि प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखना सम्प्रदाय प्रवर्त्तन की अनिवार्य
शर्त है तो विष्णुस्वामी सम्प्रदाय पर वह पूरी तरह चरितार्थ नही होती, फिर भी विष्णुस्वामी सम्प्रदाय को चतु सम्प्रदाय में
आचार्य कोटि के सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण एव गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्रव इस
सम्प्रदाय से सम्बद्ध कहे जाने वाले वल्लभ सम्प्रदाय पर विचार करके यह बडौदा
विश्वविद्यालय के प्रो० जी० एच० भट्ट ने मैसूर में हुई ओरियटल कान्फ्रेंस में अपना
जो निवन्ध पढा था उसमे यह सिद्ध किया है कि ऐतिहासिक या दार्शनिक दृष्टि से
विष्णुस्वामी और वल्लभाचार्य का कोई सम्बन्ध स्थापित नही किया जा सकता। वस्तुत ये
दोनो स्वतत्र वैष्णव सम्प्रदाय है। वल्लभाचार्य ने अपने मत को पुष्टिमार्ग का नाम
देकर वैसे भी नवीन कलेवर दे दिया है जो विप्णुस्वामी की परम्परा में न तो दार्शनिक
दृष्टि से जोडा जा सकता है और न कोई ऐतिहासिक आधार ही उसे एक घरातल पर खड़ा करता
है। सम्भव है परम्परानुगत धारणा के विपरीत यह मन्तव्य कुछ विस्मयकारक लगे किंतु
सत्य को स्वीकार करने में सकोच नही होना चाहिए। वल्लभाचार्य की भत्क्ति-पद्धति का नूतन रूप और उसमे कृष्ण के माधुर्य भाव की
उपासना की स्वीकृति अपनी विशिष्ट देन है जो विष्णुस्वामी के युग में किसी भी रूप
में प्रचलित नही थी। सारत यह स्वीकार करना ठीक ही है कि वैष्णव सम्प्रदायो के
स्वतंत्र रूप से प्रवर्तित होने की बात परम्परा से ही चली आ रही है इसलिए चतु
सम्प्रदायान्तर्गत होना कोई अनिवार्य शर्त नही है।
निम्बार्क सम्प्रदाय और हरिदासी
सम्प्रदाय
निम्बार्क सम्प्रदाय से सम्बद्ध सखी सम्प्रदाय हरिदास
स्वामी द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय पर भी इस दृष्टि से विचार करना हम आवश्यक समझते
हैं। हम यह पहले लिख चुके हैं कि निम्बार्क मत प्राचीनता की दृष्टि से विशेष
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कतिपय विद्वानो ने तो निम्बार्काचार्य को सबसे प्राचीन
माना है और उनके दार्शनिक विचारो में गम्भीर विवेचन देखकर उन्हें भक्ति सम्प्रदायो
का अग्रणी मननशील आचार्य ठहराया है। नवीन अनुसधान के परिणामो के अनुसार इनका समय
बारहवी शताब्दी का अन्त या तेरहवी शताब्दी का प्रारम्भमाना जाता है। निम्बार्क कृत
'वेदातपारिजातसौरभ' ब्रह्मसूत्र भाष्य अति सक्षिप्त होने पर भी प्रौढता
की दृष्टि से उल्लेखनीय समझा जाता है। निम्बार्काचार्य के प्रमुख पाँच ग्रथो में (पारिजात सौरभ, दश श्लोकी, मंत्र रहस्य पोडश।, प्रपन्न कल्पवली और श्रीकृष्णस्तवराज) इस सम्प्रदाय के सिद्धातो का भलीभाति प्रतिपादन हुआ
है। निम्बार्क सम्प्रदाय का दार्शनिक सिद्धात द्वैताद्वत के नाम से प्रसिद्ध है।
जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी। भेदाभेद का सिद्धात
कुछ मनीपियो के अनुसार अति प्राचीन है। इसी आधार पर निम्बार्क की प्राचीनता भी
सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। इस सम्प्रदाय के सिद्धात और भक्ति-पद्धति को हृदयंगम करने के लिए 'दश श्लोकी' का अनुशीलन करना पर्याप्त है। इस सम्प्रदाय मे कृष्ण ही उपास्य, भजनीय, सेव्य और पूज्य है। कृष्ण की भक्ति छोड किसी और की सेवा-पूना करना व्यर्थ है। 'नान्यागति कृष्ण पदारविन्दात्' ही इस सम्प्रदाय का आराध्य कहा गया है। किन्तु कृष्ण
के साथ राधा को भी इष्टदेवी के रूप मे स्वीकार किया गया।
अङ्गतु
वामे वृषभानुजां सुदा विराजमानामनुरूप सौभगाम् ।
राधा को स्वकीया के रूप मे स्वीकार करके उनकी समस्त
लीलाओ मे स्वकीयात्व का आरोप किया जाता है। श्री हरिव्यासाचार्य ने इस सम्प्रदाय
मे शात, दास्य, वात्सल्य, सख्य और माधुयं इन पाच रसो का समर्थन किया और माधुर्य को उत्कृष्टता प्रदान
की। प्रेमलक्षणा, अनुरागात्मिका पराभक्ति ही इस सम्प्रदाय मे सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। सखी
सहस्रः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम् । (दश श्लोकी, श्लोक सं० ५) इस सम्प्रदाय के श्राचार्य निम्बार्क ने उपनिपद् या गीता पर कोई भाष्य नही
लिखा। 'गीता
वाक्यार्थ' नामक एक ग्रथ की सूचना मिलती है किन्तु ग्रथ अभी तक प्रकाश मे नही आया। फलत. 'पारिजात सौरभ' ही भाप्य कोटि का एकमात्र ग्रंथ है। हा, परवर्ती आचार्यों में श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बराचार्य, लक्ष्मण भट्ट, पुरुषोत्तमाचार्य, केशव कश्मीरी आदि ने अनेक ग्रथो की रचना कर सम्प्रदाय
को उच्च दार्शनिक स्तर पर पहुँचाया। हिंदी साहित्य मे इस सम्प्रदाय के महात्माओ ने
अपनी वाणियाँ लिखी और माधुर्य भक्ति को परिपुष्ट बनाने मे योग दिया। इन वाणियो का
रस भक्ति के विकास में विशिष्ट स्थान है। वैष्णव सम्प्रदायो का इतिवृत्त इतना
व्यापक है कि उसे न तो चतु सम्प्रदाय के अन्तर्गत सीमित किया जा सकता है और न किसी
काल या देश की सीमा-मर्यादा
में आबद्ध करके देखा जा सकता है। विष्णु की कल्पना और उसके विभिन्न अवतारों की
पूजा पुरातन काल से चली आ रही है। वैदिक वाङ्मय से लेकर मध्ययुगीन पुराण ग्रथो तक
विष्णु के विविध रूपो का वर्णन इस बात का प्रमाण है कि विष्णु के नारायण, वासुदेव, कृष्ण श्रादि रूपो की उपासना-आराधना वैष्णव भक्ति के अन्तर्गत समझी जाती रही है। अत किसी मी सम्प्रदाय
को वैष्णव होने के लिए चतु सम्प्रदाय की सकीर्ण परिधि में रहना अनिवार्य नही । जो
विष्णु की उपासना-आराधना, सेवा-अर्चा करता है वही वैष्णव है। वैष्णवता भक्ति के उस रूप पर आश्रित है जो
विष्णु के विविध रूपो मे से किसी को भी स्वीकार कर विकसित होती है। विष्णु के
अर्चावतार या व्यूहावतार की कल्पना भी विष्णु भक्ति को मासल रूप देने के उद्देश्य
से की गई है। अत कोई भी भक्त इन रूपो मे से यथारुचि किसी को भी ग्रहण करके अपनी
भक्ति-भावना
को व्यक्त करने का अधिकारी है और वह सच्चे अर्थो मे वैष्णव जन ही समझा जायगा ।
सकीर्ण साम्प्रदायिक रूढियो मे विश्वास रखने वाले कतिपय आधुनिक कट्टरपथियो ने
राधावल्लभ सम्प्रदाय के सम्बन्ध में यह आरोप लगाया है कि यह सम्प्रदाय यथार्थ
वैष्णव सम्प्रदाय नही है। जब तक चतु सम्प्रदायो के साथ यह अपना साक्षात् सम्वन्ध
स्थापित न करे हम इसे वैष्णव मानने को उद्यत नही। इस आरोप को ध्यान में रखकर ही
हमने चतु सम्प्रदाय शब्द की आधुनिकता, उसका सीमा विस्तार तथा अनेक वैष्णव सम्प्रदायो के स्वतन्त्र अस्तित्व का
वर्णन पिछले पृष्ठो में किया है। राधावल्लभ सम्प्रदाय को विशुद्ध वैष्णव सिद्ध
करने के साथ हम यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि यह सम्प्रदाय अपनी साधना-पद्धति, विचार-भावना, सेवा-पूजा आदि में किसी अन्य सम्प्रदाय का अनुगत नही है। गोस्वामी हितहरिवशजी ने
विभिन्न सम्प्रदायो की पद्धतियो का मनन करने के उपरान्त अपनी स्वतन्त्र प्रणाली से
इस सम्प्रदाय की स्थापना की थी। विधि-निषेध के बाह्याचार को तो उन्होने एकदम मिथ्याडम्बर मानकर उपेक्षणीय तक कह
डाला था। जिसे देखकर अपने वैष्णव होने का दम्भ करने वाले कितने ही कट्टरपथियो को
उनके इस साहस पर आश्चर्य और क्रोध तक हुआ। किन्तु सच्चा वैष्णव कृष्ण की भक्ति के
परमतत्व पर दृष्टि रखता है, वाह्याचार के आडम्बर पर नही ।
जेव
रूपः
विगत पचास वर्षों में हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक त
प्रस्तुत करने वाले अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इन ग्रथो 100/650 कतिपय राधावल्लभीय भक्तो का वर्णन हुआ है। श्री
हितहरिवंशजी को छोड़कर अन्य किसी भक्त कवि के विवरण मे राधावल्लभ सम्प्रदाय की
किसी सैद्धान्तिक या धार्मिक भावना पर कुछ भी नही लिखा गया। व्यास तथा ध्रुवदास
जैसे प्रौढ भक्त कवियो के काव्य को भी केवल सरसरी दृष्टि से उल्लेख करके छोड दिया
है। इस उपेक्षा का मूल कारण साम्प्रदायिक वाणियो की अनुपलब्धि तथा सिद्धान्तो का
अज्ञान ही है। अभी तक इस सम्प्रदाय की भक्ति और उपासना पद्धति को समझने-समझाने का कोई प्रयास नही हुआ फलतः इसके प्रतिभाशाली, भावुक एव भक्त कवियो की उपेक्षा होती रही। जो कुछ
लिखा गया वह प्रायः अग्रेज लेखक विलसन, ग्राउस और ग्रियर्सन के लेखो के आधार पर ही है। भक्ति-पद्धति के स्वरूप को समझने के लिए नाभाजी का भक्तमाल
वाला छप्पय ही पर्याप्त समझा जाता रहा । आश्चर्य है कि कवियो की इतनी विपुल सख्या
और काव्य-सौन्दर्य
का इतना अधिक प्राचुर्य भी आलोचको और सहृदयो को आकृष्ट न कर सका। यह ठीक है कि
हस्तलिखित वाणी ग्रथो के सुलभ न होने से इस प्रकार की उपेक्षा रही किन्तु जिज्ञासु
के लिए कुछ भी अप्राप्य नही रहता । नीचे की पक्तियो मे हम कतिपय विशिष्ट ग्रंथो
में वर्णित तथ्यो पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे। विवेचन मे हमारा
उद्देश्य भ्रमनिवारण तथा तथ्य उद्घाटित करना मात्र है, किसी प्रकार के खडन गडन में पडकर निन्दा-स्तुति का मार्ग ग्रहण करना हमे अभीष्ट नही । तथ्य-निर्णय के लिए जहाँ खडनात्मक शैली स्वीकार की गई है
उसे अन्यथा नही समझना चाहिए । हमने जिन ग्रथो का आगे वर्णन किया है वे हिन्दी
साहित्य के विशिष्ट ग्रथ है। इनके अतिरिक्त और भी पाँच-सात ग्रथो में राधावल्लभ सम्प्रदाय का वर्णन है
किन्तु वह इन्ही में से किसी न किसी का रूपान्तर मात्र है अत सवको स्थान नही दिया
गया। डा० रमाशकर शुक्ल रसाल और प० अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध के इतिहास ग्रथ
प्रसिद्ध होने पर भी कोई नवीन सूचना प्रस्तुत नही करते अतः हमने उन्हे छोड़ दिया
है। इस ग्रंथ में दो स्थलो पर गो० हितहरिवंशजी का नामोल्लेख है। प्रथम स्थल पर
केवल उनका एक पद दिया है और दूसरे स्थल पर इस प्रकार गद्य में परिचय है। "हितहरिवंश स्वामी गुसाई वृन्दावन निवासी । व्यास
स्वामी के पुत्र सम्वत् १५५६ मे उत्पन्न । इनके पिता व्यास जी ने राधावल्लभी सम्प्रदाय
चलाया। यह देववन के रहने वाले गौड ब्राह्मण थे । हितहरिवंश जी महान् कवि थे।
सस्कृत में राधासुधानिधि ग्रंथ और भाषा में 'हितचौरासी' नामक ग्रंथ बनाया ।
निष्कर्ष:
राधावल्लभ
सम्प्रदाय भारतीय भक्ति परंपरा में एक विलक्षण एवं विशिष्ट स्थान रखता है। यह
सम्प्रदाय केवल भक्ति का प्रचारक नहीं, अपितु भक्ति
को प्रेम की परम ऊँचाई तक ले जाने वाला साधन मानता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता
यह है कि यह सम्प्रदाय राधा को परब्रह्म के रूप में स्थापित करता है,
जो
अन्य किसी वैष्णव सम्प्रदाय में नहीं मिलता।
जहाँ
परंपरागत वैष्णव सम्प्रदायों में भगवान श्रीकृष्ण या विष्णु को उपास्य माना गया है,
वहीं
राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा को ही सर्वशक्तिमान, सर्वाधार
और मूल तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। कृष्ण को राधा के आनन्द स्वरूप के
रूप में देखा जाता है। यह सम्प्रदाय इस मत को दृढ़ता से प्रतिपादित करता है कि
राधा ही सृष्टि की आद्यशक्ति हैं और उनका प्रेम ही मोक्ष का माध्यम है।
इस
सम्प्रदाय की सैद्धांतिक विशेषता यह भी है कि यह दर्शन, तर्क
या ज्ञान को द्वितीय स्थान पर रखकर प्रेम, अनुभूति
और माधुर्य को प्राथमिकता देता है। भक्त और भगवान के बीच सम्बन्ध को नैयायिक या
कर्मकाण्डीय दायरे में न बाँधकर स्वाभाविक प्रेम के रूप में परिभाषित किया गया है।
यह सम्प्रदाय रस सिद्धान्त, विशेषतः माधुर्य
रस को सर्वोच्च मानता है।
राधावल्लभ
सम्प्रदाय का भक्ति मार्ग किसी जटिल विधि-विधान पर आधारित नहीं,
बल्कि
सरल हृदय से राधा में प्रेमपूर्ण समर्पण करने पर आधारित है। यह सम्प्रदाय बताता है
कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए ना तो कठोर तप की आवश्यकता है, ना
ही गहन ज्ञान की – केवल निष्कलंक, स्वार्थरहित
प्रेम ही पर्याप्त है।
इस
प्रकार,
राधावल्लभ
सम्प्रदाय एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो राधा के माधुर्य स्वरूप,
रसपूर्ण
भक्ति,
और
सहज प्रेम के दर्शन को केंद्र में रखकर भक्ति का सबसे भावमय रूप प्रस्तुत
करता है। यह सम्प्रदाय आज भी वृन्दावन सहित अनेक स्थानों पर अपने विशुद्ध भक्ति
रूप के लिए जाना जाता है।
संदर्भ ग्रांथ सूची
v "वेवर नामक पश्चिमी संस्कृत पंडित ने इस
कथा (नारायणीयाख्यान) का विपर्यास करके यह दीर्घ शंका की थी कि भागवत धर्म में
वर्णित भक्ति तत्व, श्वेत द्वीप से अर्थात् हिन्दुस्तान
के बाहर के किसी अन्य देश से लाया गया है और भक्ति का यह तत्व इस समय ईसाई धर्म के
अतिरिक्त और कहीं भी प्रचलित नहीं था। अब पश्चिमी पण्डितों ने यह भी निश्चित किया
है कि वेवर साहब की उपयुक्त शंका निराधार है।"
गीता
रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र' श्री वाल
गंगाधर तिलक (हिन्दी) पृष्ठ ५४६
v ऋग्वेद के मत्रों में भक्ति के अवयवों का प्रतीक
शैली से प्रतिपादन
श्रवण
- 'यो
जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेवु ध्रुवोभियु उय चिदभ्यसत् ।'
ऋग्वेद
म० १। अ० १५६ । मत्र २ ।- कीर्तन- 'विष्णोर्नु
क वीर्याणि प्र वोच य पायिवानि विममे रजाति ।'
ऋग्वेद
१।१५४।१
v त्वहिन पिता वत्तो त्व माता शतक्रतो वभूविथ ।
अघाते सुन्ममीमहे । ऋग्वेद ८।६८।११ तमु स्तोतार पूर्व्य यथा विद ऋत्तस्य गर्भ
जनुषा पिपर्तन ।, आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते
विष्णो सुर्मात भजामहे ।। त्रऋग्वेद १।१५६१३
v डा०
बेनीप्रसाद रचित 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता'-
पृष्ठ
४२ ।
v 'इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहूरयो दिव्य
स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एक
सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाह ॥
ऋग्वेद
१ । १६४ । ४३-
'तदेवाग्निस्तवावित्यस्तद्
वायुस्तवु चन्द्रमा ।
तदेव
शुक्र तद् ब्रह्म ता आप स प्रजापति ।।'
यजुर्वेद
३१ । १३6 / 650
v 'महाभाग्यात्
देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते ।
एकस्य
श्रात्मनः अन्ये देवाः प्रत्यगानि भवन्ति ।।'
यास्क,
निरुक्त
दैवत कांड (७-४ । ८, ६)
v कीथ
का लेख कल्याण कल्पतरु अगस्त १६३६, पृष्ठ ५५४ ।
v नारदपंचरात्र-
श्लोक स० २,७,२८,३२-४
v भत्तिसूत्र
नारद ७६-८३,
भक्तिसूत्र
शाडिल्य - श्रध्याय २, सूत्र ८३
v सूरदास
(भक्ति का विकास) पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ २६
v श्रप्टादश
पुराणार्ना श्रवणाद्यत्फलभवेत् ।
तत्त्फलं
समवाप्नोति वैष्णवोनात्र संशय. ।। महाभारत १८।६।६७
.png)