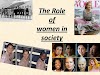स्वास्थ्य की दृष्टि से सिद्धासन की अवधारणा हठयोगिक ग्रन्थों के विशेष परिप्रेक्ष्य में
सचिन
कुटे, शोधार्थी योग
योग
एवं आयुर्वेद विभाग
साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वधिालय साँची रायसेन
सारांश
वर्तमान समय आधुनिकीकरण व
प्रयोगवादी काल है,
जहाँ ढेरों
आविष्कार हो रहे हैं। और प्रयोगों की कसौटियों पर मानव जीवन व पर्यावरण का क्षरण
हो रहा है। आज 21वीं शताब्दी में मानव जीवन इतना अस्त-व्यस्त व
प्रदूषित हो रहा है कि स्वयं के शरीर की देखरेख करना एक कार्य के समान हो गया है।
स्वस्थ रहना अपने आप में चुनौती बनती जा रही है। जिन पंचमहाभूतों - आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से हमारा शरीर बना, जब वे स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण,
पृथ्वी (भूमि)
प्रदूषण, तो स्वस्थ रहना मानव जीवन में कल्पना मात्र बनता
जा रहा है। ढेरों बीमारियाँ,
जिनमें से
अधिकतर कॉरपोरेट कंपनियों में सिटिंग जॉब करने वाले लोगों को होती हैं, जैसे कि लंबर,
सर्वाइकल, स्पोंडिलोसिस,
एंजायटी, डिप्रेशन की समस्या,
व व्यक्ति के
सर्वांगीण विकास - शारीरिक,
मानसिक, आध्यात्मिक - के लिए हठयोग आश्रय स्थल है। आज आसनों की महत्ता को देखें तो
कोई भी ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो हमें सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रदान कर
सके। दवाइयों का असर भी सीमित समय तक व शरीर के कुछ भाग तक ही होता है, मानसिक,
भावनात्मक व आध्यात्मिक
नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास केवल और केवल योग से ही संभव है।
मूल शब्द-
स्वास्थ्य, आसन,
सिद्धासन,
हठयोग,
शारीरिक
और मानसिक स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास
प्रस्तावना
प्राचीन काल से ही व्यक्ति के
विकास में स्वास्थ्य का महत्व कहा गया है। पहला सुख निरोगी काया। कोई व्यक्ति तभी
सुखी व आनंदित हो सकता है जब वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो। एक स्वस्थ
व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों को चुनौती देकर समाज में एक अच्छा स्तर प्राप्त
कर सकता है और समाज के प्रति कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन कर आध्यात्मिक
उन्नति की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का और स्वस्थ मन
में ईश्वर का निवास होता है। ईशावास्योपनिषद में भी कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने
की कामना कर कर्मों में लिप्त न होकर इसके अतिरिक्त परम कल्याण का कोई अन्य मार्ग
नहीं बताया गया है।[1]
स्वास्थ्य
की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ विख्यात हैं।
स्वास्थ्य का अर्थ समझें तो शरीर
के विभिन्न अंगों तथा संस्थानों का ठीक ढंग से कार्य करना है। शरीर के माध्यम से
ही सारे कार्य सम्पन्न होते हैं। अतः शरीर स्वस्थ होने पर ही कार्यों को सफलतापूर्वक
सम्पादित किया जा सकता है।[2]
आयुर्वेद शास्त्र के दो प्रयोजन हैं: प्रथम, स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा
करना; द्वितीय, रोगी मनुष्य के रोग का निवारण करना, अर्थात् यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो वह स्वस्थ बना रहे और यदि किसी के
शरीर में कोई विकार है,
तो उसका निवारण हो
सके। यह आयुर्वेद का उद्देश्य है।[3]
आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में स्वास्थ्य की परिभाषाएँ बताते हुए कहा है:
वात, कफ और पित्त का सम होना; तेरह अग्नियों (एक जठराग्नि, सात धातु पाचक, पाँच भूत पाचक) का सम होना; सात धातुओं (रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र) का सम होना; व तीन प्रकार के मलों का सम होना; आत्मा, इंद्रियाँ और मन तीनों की प्रसन्नता ही
स्वास्थ्य है।[4]
विश्व
स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है: स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक सुख की एक पूर्ण
अवस्था है, न केवल रोग विशेष तथा शारीरिक
कमी की अनुपस्थिति। समग्र स्वास्थ्य के अंतर्गत फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, आध्यात्मिक - शरीर के सभी आयामों पर
चर्चा की जाती है। महर्षि पतंजलि ने भी सभी प्रकार के साधकों (ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी) सभी के लिए अष्टांग योग का
मार्ग सुलभ कर कैवल्य प्राप्ति का लक्ष्य बताया गया है, जो देखें तो स्वास्थ्य की परिभाषा को
परिपूर्ण (सार्थक) करता है,
जिसमें आसन
(शारीरिक स्वास्थ्य),
प्राणायाम व
प्रत्याहार (मानसिक स्वास्थ्य),
यम, नियम (भावनात्मक स्वास्थ्य) और धारणा, ध्यान, समाधि (आध्यात्मिक स्वास्थ्य) को
परिपूर्ण किया जाता है। यह महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले बताया था। रोगों की
उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति के तीनों गुणों (सत्, रज, तम) की साम्यावस्था का न होना है।
सम्पूर्ण सृष्टि इन तीनों गुणों से बँधकर रहती है। जिस तरह समग्र नदियों का जल
समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खोकर समुद्र में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार समग्र स्वास्थ्य का प्रयोजन
आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति व मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो।
हठयोगिक
ग्रंथों में आसन व स्वास्थ्य
हठयोग, जिसे आमतौर पर शारीरिक योग अभ्यास का
मूलभूत आधार माना जाता है,
शारीरिक स्थितियों
(आसन), प्राणायाम (श्वास-प्रश्वास की
तकनीक) और ध्यान की प्रणाली को शामिल करता है। हठयोग में 'हठ'
शब्द 'ह' और 'ठ'
दो अक्षरों से
मिलकर बना है।
हकारः कीर्तितः सूर्यष्ठकारश्चन्द्र उच्यते ।
सूर्याचन्द्रमसोर्योगाद्
हठयोगो निगद्यते ॥ (सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति १)
हकार
का अर्थ सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी से है और ठकार का अर्थ चन्द्र स्वर या इडा
नाड़ी से लिया गया है। इन सूर्य और चन्द्र स्वरों के मिलन को ही हठयोग कहा गया है, क्योंकि सूर्य और चन्द्र के मिलन से वायु
सुषुम्ना में चलने लगती है,
जिससे मूलाधार में
सोई हुई कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर चलने लगती
है तथा षट्चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्मरंध्र में पहुँचकर ब्रह्म के साथ एकत्व
को प्राप्त होती है। यही आत्मा और परमात्मा तल का मिलन है और विभिन्न ग्रंथों में
हठयोग प्राप्ति के विभिन्न साधन व योगांग बताए गए हैं।
शोधनं
दृढता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम्,
प्रत्यक्षं
च निर्लिप्तं च घटस्थसप्तसाधनम् ॥ (घेरंड संहिता १.९)
सात
साधनों द्वारा महर्षि घेरंड मुनि ने शरीर शुद्धि के उपायों को बताया है। षट्कर्म द्वारा
शोधन शरीर और मन को विकार रहित बनाता है। आसनों से दृढ़ता, शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक बल मिलता है। स्थैर्य
(स्थिरता) मुद्रा व बंध द्वारा शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है। धैर्य (धैर्य)
प्रत्याहार से मनुष्य अपना धैर्य नहीं खोता, किसी भी परिस्थिति में सहनशील होना व
सहनशीलता का भाव आता है। लाघव (हल्कापन) प्राणायाम द्वारा योगी में हल्कापन आता है, शरीर भारी नहीं होता। प्रत्यक्ष
(प्रत्यक्षता) ध्यान द्वारा प्रत्यक्षता, ग्रहणशीलता
(ग्रहण करने का स्वभाव) आती है,
जिसमें सूक्ष्म या
आंतरिक अनुभव होते हैं। निर्लिप्त (निर्लिप्तता) समाधि से निर्लिप्तता आती है, अर्थात् मन का आसक्त न होना – ये सभी स्वास्थ्य में उपयोगी हैं। रोगी
व्यक्ति को भी अरोगी बनाने के ये सात साधन हैं।[5]
पीठानि कुम्भकाश्चित्रा दिव्यानि करणानि च ।
सर्वाण्यपि हठस्यासे राजयोगफलप्रदम् ॥
(हठप्रदीपिका १.६७)
हठयोग
प्रदीपिका में आसनों को स्वामी स्वात्माराम सूरि ने प्रथम स्थान दिया है। हठयोग को
राजयोग का अभिन्न अंग माना गया है। अथवा यदि यह कहा जाए कि हठयोग,
राजयोग
का पूर्वाभ्यास है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं
होगी। इसी का उल्लेख करते हुए स्वामी स्वात्माराम सूरि ने अपनी अमूल्य कृति
हठप्रदीपिका के प्रथम उपदेश में आसनों के लाभ व विधि को दर्शाया है। विभिन्न आसन,
विभिन्न
कुम्भक, विभिन्न उत्कृष्ट मुद्राएँ –
यह
सब हठयोग अभ्यास राजयोग में सफल होने तक करने चाहिए। हठयोग एवं राजयोग मिलकर ही
पूर्ण योग का निर्माण करते हैं। यद्यपि योग का चरम लक्ष्य चित्त की समस्त
वृत्तियों का पूर्णतया निरोध करना है।
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२ ॥ (पातञ्जल
योगसूत्र)
हठयोग
को काया साधना प्रधान पद्धति माना जाता है। प्रथम प्रभाव शरीर पर पड़ता है,
उपरांत
सूक्ष्म एवं कारण शरीर पर। अतः हठयोग राजयोग के शिखर पर पहुँचने वाली सीढ़ी के
समान है। सामान्य मनुष्य के लिए महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग सर्वाधिक प्रसिद्ध
है – यम, नियम,
आसन,
प्राणायाम,
प्रत्याहार,
धारणा,
ध्यान,
समाधि
– जिसमें आसनों को तृतीय स्थान पर रखा गया है,
क्योंकि
शरीर और मन की साधना किए बिना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।
हठयोग का उद्देश्य:
राजयोग की प्राप्ति,
समग्र
स्वास्थ्य, आरोग्य की प्राप्ति,
व्यक्ति
का सर्वांगीण विकास, शक्तियों का जागरण,
आध्यात्मिक
विकास। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में योगासन की संक्षिप्त परिभाषा है:
स्थिरसुखमासनम् ॥ ४६ ॥ (पातञ्जल योगसूत्र २.४६)
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ॥ ४७ ॥
(पातञ्जल योगसूत्र २.४७)
वह
स्थिति, जो सुखद और स्थिर हो। इस
परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की क्षमता विकसित करने के लिए आसनों
का अभ्यास किया जाता है, जो
ध्यान के लिए एक आवश्यक योग्यता है। राजयोग में आसन से अभिप्राय बैठने की स्थिति
से है, जबकि हठयोग में इसका तात्पर्य
कहीं बढ़कर है। आसन शरीर की वे विशिष्ट अवस्थाएँ हैं, जो
नाड़ियों और चक्रों को खोलती हैं। वे उच्च जागरूकता प्राप्त करने के साधन हैं। यह
हमारे शरीर, श्वास, मन
और उसके परे की शक्तियों की खोज के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। हठयोगियों का
अनुभव है कि आसनों के द्वारा शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। अतः हठयोग
में आसनों का स्थान सर्वोपरि है। हठप्रदीपिका में आसनों को प्रथम स्थान पर रखा हुआ
है:
हठस्य प्रथमाङ्गत्वादासनं पूर्वमुच्यते।
कुर्यात्तदासनं स्थैर्यमारोग्यं चाङ्गलाघवम् ॥
(हठप्रदीपिका १.१७)
आसन
स्वामी
सत्यानन्द सरस्वती अपनी पुस्तक 'आसन
प्राणायाम मुद्रा बंध' में आसनों की
क्रियाविधि को समझाते हुए कहते हैं: आसनों की क्रियाविधि व उत्पत्ति पशुओं की
भंगिमा को दर्शाती है, और उनका नाम पशुओं के
नाम पर किया गया है। आसनों के अभ्यास से किस प्रकार हार्मोन के स्त्राव को
नियंत्रित एवं प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, खरगोश
की भंगिमा का अनुसरण कर शशांकासन में एड्रीनलीन के प्रभाव को प्रभावित किया जा
सकता है, जो कि संघर्ष पलायन प्रक्रिया
को नियंत्रित करता है। पशुओं की विभिन्न भंगिमाओं का अनुकरण कर ऋषियों ने अपने
स्वास्थ्य रक्षण का उपाय खोज निकाला था और इसके द्वारा वे प्रकृति की चुनौतियों का
मुकाबला करने में सक्षम हुए।[6] आसनों
का वर्गीकरण देखें तो, जिसमें आसनों को खड़े
होकर, लेटकर, बैठकर
किया जाता है। वर्तमान समय में आसनों को केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही किया जा
रहा है। योग ग्रंथों में उल्लेख है कि प्रारंभ में चौरासी लाख आसन थे,
जो
जीव की चौरासी लाख योनियों के प्रतीक हैं। मोक्ष प्राप्ति के पूर्व हर जीव को इन
सभी योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। ये आसन प्राणी की प्रारंभिक अवस्था से मोक्ष
की अवस्था तक के प्रगतिशील विकास को प्रकट करते हैं। युग के अनुरूप ऋषियों एवं
योगियों ने क्रमशः आसनों को रूपांतरित किया और संख्या कम होते-होते,
कुछ
सौ के अंदर ला दिया है। यहाँ सैकड़ों आसनों में से सर्वाधिक उपयोगी मात्र चौरासी
आसनों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
सिद्धासन की अवधारणा हठयोगिक
ग्रंथों में
सिद्धासन की अवधारणा
हठप्रदीपिका में
एक पाँव की एड़ी को सीवनी में अच्छी तरह लगाकर और दूसरे
पाँव को शिश्न के ऊपर दृढ़ता से रखें। चिबुक को हृदय प्रदेश पर अच्छी तरह स्थापित
कर, इंद्रियों को संयमित कर तथा भूमध्य-दृष्टि
होकर निश्चल रहना चाहिए। इसे सिद्धासन कहते हैं। इसे ही दूसरे लोग वज्रासन कहते
हैं, कुछ लोग इसे मुक्तासन कहते हैं और दूसरे
कुछ लोग गुप्तासन कहते हैं। मोक्षद्वार का भेदन करने वाला अर्थात् मोक्ष प्राप्त
कराने वाला यह सिद्धासन है। आसन से मानसिक तथा शारीरिक स्थिरता,
आरोग्यता
तथा शरीर में हल्कापन आता है। हठप्रदीपिका में पंद्रह आसनों को बताया गया है,
जिनमें
से चार आसनों को सारभूत – सिद्धासन,
पद्मासन,
सिंहासन,
भद्रासन
– मोक्ष की प्राप्ति वाला सिद्धासन
सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। उन चौरासी आसनों
में से केवल सिद्ध आसन का ही सदा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि
इससे शरीरस्थ बहत्तर हजार नाड़ियों का मलशोधन होता है। जिस प्रकार यमों में
मिताहार और नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, उसी
प्रकार यह सिद्धों का सिद्धासन भी सभी आसनों में महत्त्वपूर्ण है।
सिद्धासन की अवधारणा गोरक्ष
संहिता में
योनिस्थान को एड़ी से दबाएँ, हृदय
में हनु (ठुड्डी) लगाएँ, दूसरा
पैर लिंग के ऊपर, इंद्रियों को स्थिर कर
संयम पूर्वक भूमध्य-दृष्टि में स्थापित करें। गोरक्ष संहिता में भगवान शिव ने
चौरासी लाख आसन बताए हैं। आसनों से रोग नाश बताया गया है। इनमें से गोरक्षनाथ
द्वारा दो आसनों – सिद्धासन व कमलासन
(पद्मासन) – और सिद्धासन से मोक्ष की
प्राप्ति महत्त्वपूर्ण बताई गई है।
सिद्धासन की अवधारणा घेरंड
संहिता में
जितेन्द्रिय योगी एक पाँव की एड़ी को अण्डकोश और गुदा
के मध्य लगाकर दूसरे पाँव की एड़ी को मेढ़्र में लगा ले। चिबुक को हृदय में लगाकर
स्थिर रूप से सीधा रहे। दृष्टि को निश्चल रखकर भौहों के मध्य में देखे। इसका
अभ्यास सिद्ध होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे सिद्धासन कहते हैं। महर्षि
घेरंड ने घेरंड संहिता में भी भगवान शिव द्वारा बताए चौरासी लाख आसन व उनमें से भी
चौरासी आसन श्रेष्ठ बताए हैं। उन चौरासी आसनों में भी बत्तीस आसनों को अतिविशिष्ट
बताया व सिद्धासन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बताई है।
सिद्धासन की अवधारणा शिवसंहिता
में
योग साधक एक पाँव की एड़ी से योनिस्थान को यत्नपूर्वक
दबाकर पुनः दूसरे पाँव की एड़ी को लिंग के ऊपर स्थापित करे। योगी सदा स्थिर,
जितेन्द्रिय
रहकर भौहों के मध्य में ऊपर देखे। इस प्रकार एकान्त में विशेष रूप से शरीर को सीधा
रखे तथा उद्वेगों से शून्य रहे। शिवसंहिता में चौरासी आसन व चौरासी आसनों में से
चार – सिद्धासन,
पद्मासन,
उग्रासन,
स्वस्तिकासन
– की विधि को बताया गया है। तृतीय अध्याय में
सिद्धासन को मुक्तासन व परम गति की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है।
सिद्धासन की अवधारणा
हठरत्नावली में
एक पाँव की एड़ी को सीवनी में अच्छी तरह लगाकर,
दूसरे
पाँव को शिश्न के ऊपर दृढ़तापूर्वक रखे। इंद्रियों को संयमित कर,
दृष्टि
को भौहों के मध्य में लगाकर सीधे और स्थिर रहे। यह सिद्धासन है,
जो
मोक्ष के द्वार खोलता है। आसनों का अभ्यास रोगों को दूर करता है और स्थिरता,
स्वास्थ्य
एवं हल्कापन प्रदान करता है। सर्वशक्तिमान शम्भु ने मनुष्य की चौरासी लाख योनियों
को मानते हुए, हठरत्नावली में चौरासी आसनों
का उल्लेख किया है, जो कि आरोग्य और सुख
प्रदान करते हैं, जिसमें आसनों का वर्णन
तृतीय अध्याय में किया है। जिनमें से दस मुख्य व चार श्रेष्ठ माने गये हैं,
जैसे
सिद्धासन, पद्मासन,
सिंहासन,
भद्रासन
हैं।
सिद्धासन की अवधारणा
सिद्धसिद्धांत पद्धति में
सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चित्त स्वरूप में सदा
विद्यमान रहना तथा स्वस्तिकासन, पद्मासन,
सिद्धासन
इनमें अपनी इच्छा अनुसार किसी एक को लगाकर एकाग्र होकर आसन की विधि बताई गई है।
निष्कर्ष
इस
आधुनिक युग में हमारा जीवन पूर्णतः मशीनों पर निर्भर करता है। हमारा जीवन प्रकृति
से बहुत दूर हट चुका है और अनेक रूपों में उसने अपने प्राकृतिक सौंदर्य को खो दिया
है। हमारा भोजन बनावटी रसायनों का मिश्रण रह गया है, जो
धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे शरीर एवं व्यक्तित्व पर घातक प्रभाव डालता
है। योगासनों का अभ्यास हमें पुनः अपना प्राकृतिक स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रदान कर
सकता है। शारीरिक आराम और इंद्रिय सुख के लिए आधुनिक मनुष्य के पास सुविधाएँ हैं।
यह कार्यालय में काम करता है। कॉर्पोरेट कंपनी में सीटिंग जॉब करने वाले कर्मचारी
जो शारीरिक (सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस) मानसिक
(एंजायटी, डिप्रेशन) विकारों से विकृत
हैं और आधुनिक जीवन के नकारात्मक प्रभावों पर काबू पाने के लिए शांति और विश्राम
की खोज में नींद की गोलियाँ तथा अन्य प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं,
लेकिन
शांति, विश्राम और सुख के बजाय उन्हें
अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक
और भावनात्मक तनावों का सामना करना पड़ता है। समाज की दुश्चिंताओं और कुंठाओं के
भार से मुक्त होने का उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। योगाभ्यास के द्वारा योगासनों के
अभ्यास से वह आधुनिक सभ्य जीवन के रोग जैसे कब्ज, गठिया,
जकड़न,
निराशा,
कुंठा,
तनाव
आदि से अपने आप को मुक्त कर सकता है। आसनों के अभ्यासी जीवन के उत्तरदायित्वों एवं
समस्याओं का सामना करने के लिए अपने में अधिक शक्ति और स्फूर्ति पाएँगे। पारिवारिक
एवं सामाजिक संबंध स्वतः अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाएँगे। वैज्ञानिक आविष्कारों के
इस आधुनिक युग में जीवन को आराममय बनाने के असंख्य साधन हैं,
परंतु
विरले लोग ही इस विलास सामग्री का आनंद ले पाते हैं।
सदर्भ ग्रंथ सूची
1.
कुर्बन्नेबेह कमर्माणि
जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥
ईशावास्योपनिषद ॥२ ॥
2.
प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड,
पतंजलि योग दवारा सम्ग्र स्वास्थ्य,
पू.सं.78
3.
प्रयोजनं चास्य (आयुर्वेदस्य)
स्वस्थ्य स्वस्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च । (च०सू० 30/24)
4.
सुमदोषः समाम्निश्च
समधातुमलक्रियाः । प्रसन्नात्मेंद्रीवयमनाः स्वास्थः इत्याभिधीयते।। सुश्रुत साहित
(15/10)
5.
स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती,
घेरण्ड संहिता,
बिहार योग भारती,
मुंगेर,
बिहार, 1997-
पृसं 15
6.
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती,
आसान प्राणायाम मुद्रा बन्ध,
पृ.सं. 10
7.
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती,
घेरंड संहिता,
बिहार योग भारती,
मुगेर बिहार
8.
स्वामी दिगम्बरजीडा पीताम्बर
झा, हठप्रदीपिका,
स्वात्माराम-कृत,
कैवल्यधाम श्रीमन्माधव योगमन्दिर समिति स्वामी
कुवलयानन्द मार्ग, लोनावला
४१० ४०३ (पुणे)
9.
अनुवादक परमहसस्वामी अनन्त
भारती (महामहोपाध्याय डॉ ब्रह्ममित्र अवस्थी),
सिद्धसिद्धान्तपद्धति चौखम्मा ओरियन्टालिया
प्राच्यविद्या, दिल्ली
(भाग्न)
10. स्वानी
महेशानन्दजी (निर्देशक) डॉ. बाबूराम शर्मा (सहायक निदेशक) शिवसंहिता कैवल्यधाम,
श्रीमन्माच योग मन्दिर समिति,
लोनावला 410 403 जिला पुणे
[1] कुर्बन्नेबेह
कमर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥
ईशावास्योपनिषद ॥२ ॥
[2] प्रो.
(डॉ.) सोहन राज तातेड, पतंजलि योग दवारा सम्ग्र स्वास्थ्य, पू.सं.78
[3] प्रयोजनं
चास्य (आयुर्वेदस्य) स्वस्थ्य स्वस्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च।(च०सू० 30/24)
[4] सुमदोषः
समाम्निश्च समधातुमलक्रियाः । प्रसन्नात्मेंद्रीवयमनाः स्वास्थः
इत्याभिधीयते।।सुश्रुत साहित(15/10)
[5] स्वामी
निरंजनानन्द सरस्वती, घेरण्ड संहिता,
बिहार
योग भारती, मुंगेर, बिहार, 1997- पृसं 15
[6] स्वामी
सत्यानन्द सरस्वती, आसान प्राणायाम मुद्रा बन्ध, पृ.सं.
10
.png)