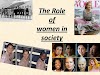विश्व शांति और बौद्ध शिक्षा
पासंग रिंजी तामांग
सहायक प्राध्यापक
बिरसा मुंडा महाविद्यालय
हातिघिसा, दार्जिलिङ - 734429
अभिसरण (Abstract):
वर्तमान विश्व में, रूस-यूक्रेन युद्ध, इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न
असमानता और सामाजिक अशांति जैसे संघर्ष व्यापक हो गए हैं। ये संघर्ष मानव जीवन में
दुख, हिंसा और
अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। इस संदर्भ में, शांति स्थापित करने में बौद्ध शिक्षा का महत्व अत्यंत
महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्ध दर्शन अहिंसा, करुणा और आंतरिक शांति पर बल देता है, जो व्यक्तिगत स्तर से लेकर
वैश्विक स्तर तक शांति के निर्माण में योगदान दे सकता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, महात्मा गौतम बुद्ध ने चार
आर्य सत्य (दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध
का मार्ग) या अष्टांगिक मार्ग (सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, जीविका, प्रयास, ध्यान और समाधि) जैसी शिक्षाएँ दी हैं। ये शिक्षाएँ संघर्ष
के मूल कारणों, जैसे लोभ, घृणा और आसक्ति, की पहचान करती हैं और
उन्हें दूर करने का तरीका सिखाती हैं। अहिंसा और करुणा व्यक्तिगत स्तर पर आंतरिक
शांति का निर्माण करके बाह्य शांति को सुदृढ़ बनाती हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार, संसार में केवल मन की शांति ही संभव है। बौद्ध दर्शन दुख, लोभ, आसक्ति और अज्ञान को संघर्ष
और अशांति के मूल कारणों के रूप में व्याख्यायित करता है। इसके समाधान के रूप में, करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग और सचेतन
जीवन जैसे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जो व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाते हैं।
हालाँकि, विश्व शांति के लिए बौद्ध
शिक्षा की प्रभावशीलता केवल आध्यात्मिक परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे संरचनात्मक और
संस्थागत परिवर्तन से भी जोड़ा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दलाई लामा और थिच न्हात हान
जैसे धार्मिक नेताओं द्वारा शांति निर्माण में निभाई गई भूमिका भी उल्लेखनीय है।
अंततः, बौद्ध शिक्षा
आध्यात्मिक अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सामाजिक सहिष्णुता के माध्यम से स्थायी और
समावेशी विश्व शांति की नींव रखने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती है।
यह शोधपत्र विश्व शांति को
बढ़ावा देने में बौद्ध शिक्षा के योगदान का संक्षेप में मूल्यांकन करता है। यह
अध्ययन 'संलग्न बौद्ध
धर्म' की अवधारणा के
माध्यम से बौद्ध शिक्षा के व्यावहारिक अनुप्रयोग - जैसे मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और संघर्ष
समाधान आदि को संक्षेप में समझने का भी प्रयास करता है।
कुञ्जी शब्द: बौद्ध शिक्षा, विश्व शांति, अहिंसा, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, सामाजिक न्याय, संघर्ष समाधान।
प्रस्तावना:
आज दुनिया के अधिकांश देश
किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना कर रहे हैं, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संघर्ष शामिल हैं। कभी देशों के बीच
संघर्ष होता है, कभी सरकारों और
देश के भीतर या बाहर विशिष्ट समूहों के बीच, और कभी-कभी एक ही देश के भीतर समूहों के बीच संघर्ष होता
है। संघर्ष केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी होता है। आज की कठिन और
चुनौतीपूर्ण जीवनशैली के कारण, लोग बड़े पैमाने पर मानसिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं।
इसलिए, ऐसे विश्व में
जहाँ संघर्ष, तनाव, हिंसा और असमानता व्याप्त
है, बुद्ध की
शिक्षाएँ मैत्री, करुणा, शांति और अहिंसा का मार्ग दिखा सकती हैं। ये समकालीन संघर्ष
आर्थिक असमानता, राजनीतिक विभाजन
और धार्मिक कट्टरता के कारण होते हैं। इन पर विचार करते हुए, यह माना जा सकता है कि
बौद्ध धर्म के दर्शन (जैसे दुख और करुणा के सिद्धांत) शांति-निर्माण और संघर्ष
समाधान में योगदान दे सकते हैं।
विश्व शांति और इसकी मूलभूत चुनौतियाँ:
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित
अर्थशास्त्र और शांति संस्थान ने जून 2025 में जारी अपनी विशेष वार्षिक रिपोर्ट "ग्लोबल पीस
इंडेक्स" में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पिछले 17 वर्षों में दुनिया कम शांतिपूर्ण हो गई है। इस रिपोर्ट के
अनुसार, वर्तमान में 59 सक्रिय राज्य-आधारित
संघर्ष हैं, जो द्वितीय
विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे अधिक और पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
यूक्रेन-रूस युद्ध, इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष सहित संघर्षों में हजारों लोगों
की जान जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक शांति में लगातार गिरावट आ
रही है क्योंकि कई देश बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों, बढ़ते संघर्षों, पारंपरिक गठबंधनों के टूटने और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता की
पृष्ठभूमि में अपने सैन्यीकरण के स्तर को बढ़ा रहे हैं। (आईईपी, 2025) आज की दुनिया
में शांति से जुड़ी वैश्विक चुनौतियाँ और अधिक जटिल होती जा रही हैं। इन चुनौतियों
का मानव जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। नीचे कुछ प्रमुख चुनौतियाँ दी गई
हैं:
• युद्ध और सशस्त्र संघर्ष - दुनिया के कई हिस्सों (जैसे यूक्रेन, गाजा, अफ्रीका के कुछ हिस्से, आदि) में युद्ध और संघर्ष
जारी हैं, जिसके
परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान, शरणार्थी संकट, कुपोषण, सामाजिक विभाजन और घृणा में वृद्धि, और शांति निर्माण प्रक्रिया को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है।
• हिंसा और आतंकवाद - वर्तमान में, दुनिया के कुछ देशों में घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय और धार्मिक दंगे, आतंकवादी हमले आदि हो रहे
हैं। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक असुरक्षा, गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और विकास में बाधाएँ उत्पन्न हुई
हैं।
• जलवायु संकट - तापमान वृद्धि, समुद्र तल में वृद्धि, सूखा, बाढ़, जंगल की आग और प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा
और संघर्ष आज के जलवायु संकट से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। जलवायु संकट का
विश्व शांति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ता है। इसमें भोजन और पानी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों पर हिंसक संघर्ष आदि शामिल
हैं।
• सामाजिक
असमानता - आज की दुनिया में जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर संघर्ष व्याप्त हैं, जिसके कारण अवसरों की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार तक पहुँच का अभाव, सामाजिक समरसता का अभाव आदि विद्रोह के कारक उभर
रहे हैं।
ये सभी
चुनौतियाँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, शांति की स्थिरता के लिए, इन सभी पहलुओं का समाधान आवश्यक है।
विश्व शांति को
बढ़ावा देने में बौद्ध शिक्षा का महत्व:
धम्मपद में कहा
गया है - जयवेरं पसवति दुक्खंसेति पराजितो।
अपसन्तो सुखंसेति
हित्वा जयपराजयं।
महात्मा बुद्ध के उपरोक्त वचन हमें यह संदेश देते हैं कि
विजय पागलपन के प्रति हमारी शत्रुता को प्रबल करती है, जबकि जो व्यक्ति पराजय से दूर हटकर आगे बढ़ सकता
है, वह चैन की नींद
सो सकता है और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है।
बौद्ध धर्म का
संक्षिप्त परिचय-
बौद्ध धर्म की स्थापना छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ
गौतम (बुद्ध) ने की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद, उन्होंने सत्य, करुणा और शांति का संदेश देना शुरू किया।
प्रारंभ में यह धर्म भारत और नेपाल में फैला। बाद में, सम्राट अशोक के संरक्षण में, बौद्ध धर्म दक्षिण एशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और अन्य क्षेत्रों में पहुँचा। बाद में, इसका विस्तार कोरिया, जापान और तिब्बत तक हुआ। आज, बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों में फैला हुआ है।
1. अहिंसा और
करुणा बौद्ध शिक्षाओं के मूल मंत्र हैं:
• अहिंसा:
अहिंसा को बौद्ध दर्शन का मुख्य आधार माना जाता है। बौद्ध धर्म की एक प्रमुख
शिक्षा पंचशील के प्रथम शील में वर्णित है - पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं
समादियामि। इसका अर्थ है केवल जीवों के प्रति हिंसा से बचना या उससे दूर रहना।
बौद्ध धर्म सभी जीवों के प्रति हिंसक न होने की शिक्षा देता है। तदनुसार, बुद्ध के शिष्यों ने 'अहिंसा' की नीति को प्रथम सूत्र के रूप में अपनाया।
हिंसा का त्याग मन को द्वेष और क्रोध से मुक्त करता है और सामूहिक शांति को संभव
बनाता है। महात्मा बुद्ध के युद्ध संबंधी विचारों के बारे में जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय के विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केंद्र के सहायक प्राध्यापक, प्रोफ़ेसर चौडूरी उपेंद्र राव लिखते हैं -
"पाली साहित्य से पता चलता है कि बुद्ध सभी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध थे, चाहे वह मनोरंजन के लिए हो, बलिदान के लिए हो या युद्ध के लिए। यदि किसी
समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से हो सकता है, तो उसे पहले किया जाना चाहिए... धम्मपद में कहा
गया है कि हिंसा से शत्रुता कभी शांत नहीं होती। शत्रुता केवल मित्रता से ही शांत
होती है। जो लोग जानते हैं कि एक दिन सभी मर जाएँगे, वे कभी एक-दूसरे से शत्रुता नहीं करते।"
• करुणा:
सभी के प्रति दया और सहयोग की शिक्षा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख अंग है। धम्मपद में
कहा गया है, "जो करुणा में
रहता है, उसे संघर्ष की
कोई इच्छा नहीं होती"। अर्थात्, करुणा रखने वाले का मन संघर्ष की इच्छा से मुक्त होता है।
करुणा का अभ्यास समाज में सद्भाव लाता है।
2. बौद्ध
शिक्षाओं का मूल दर्शन (चार आर्य सत्य)
बौद्ध धर्म का
मूल दर्शन चार आर्य सत्यों पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं - दुःख, दुःख का कारण/दुःखों का समुच्चय, दुःख का निरोध और दुःख निरोध का मार्ग। बुद्ध ने इन्हें आर्य
सत्य या आर्य सत्य कहा है:
1. दुःख:
जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ (जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, प्रियजनों से
वियोग, मनोवांछित
वस्तु का न मिलना, आदि) सभी दुःख
हैं।
2. दुःख का
कारण: इसे समुच्चय सत्य भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि तृष्णा और अज्ञान
ही दुःख के मूल कारण हैं।
3. दुःख का
निरोध: यदि तृष्णा को पूरी तरह से रोक दिया जाए, त्याग दिया जाए और नष्ट कर दिया जाए, तो दुःख को रोका या नष्ट किया जा सकता है।
4. दुःख
निरोध का मार्ग: दुःख निरोध के मार्ग के रूप में, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा पेश की है, जिसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-
1) ज्ञान
(प्रज्ञा)
क. सम्यक्
दृष्टि
ख. सम्यक्
संकल्प
2) शील
(शील)
क. सम्यक् वाक्
ख. सम्यक् कर्म
ग. सम्यक्
आजीविका
3) योग
(समाधि)
क. सम्यक्
प्रयास
ख. सम्यक्
स्मृति
ग. सम्यक्
समाधि
अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का आधार है जो दस पारमिताओं को
सही दिशा में आगे बढ़ाता है और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।
ये चार आर्य सत्य हमें मानवीय दुःख को समझने और उसे समाप्त
करने के तरीके में मार्गदर्शन करते हैं। बौद्ध दर्शन दुःख की पहचान करता है और
उसके समाधान के व्यावहारिक उपाय खोजता है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध
शिक्षाएँ विश्व में संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने और शांति को बढ़ावा देने में
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं। बौद्ध शिक्षाओं के ये मूल्य और अभ्यास
व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर अहिंसक जीवन को बढ़ावा देते हैं। नियमित
ध्यान का अभ्यास आंतरिक शांति और भावनात्मक नियंत्रण प्रदान करके मानसिक संघर्षों
के समाधान में योगदान देता है। ऐसे बौद्ध मूल्यों (अहिंसा, करुणा, त्याग और समता) से प्रेरित व्यक्ति और समूह शांति के मार्ग
पर अग्रसर होते हैं।
बौद्ध शिक्षाओं
पर आधारित शांति स्थापना के प्रयासों के कुछ उदाहरण:
• सम्राट
अशोक की अहिंसक नीति (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) - कलिंग युद्ध में हजारों
लोगों की मृत्यु देखकर व्यथित सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने
बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और करुणा को अपने शासन का
आधार बनाया। उन्होंने शांति का संदेश पहुँचाने के लिए न केवल भारत, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया में भी बौद्ध मिशन भेजे।
इसने युद्ध के बजाय कूटनीति, संवाद और
धार्मिक सह-अस्तित्व की मिसाल कायम की।
• शांति के
लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की स्थापना 1970 में दुनिया में शांति, अहिंसा और सह-अस्तित्व का संदेश फैलाने के
उद्देश्य से की गई थी। एशियाई बौद्ध सम्मेलन (Asian Buddhist
Conference for Peace - एबीसीपी) विश्व भर में शांति संवर्धन के
क्षेत्र में कार्यरत है। इसका मुख्यालय उलानबटार (मंगोलिया) में है। यह सम्मेलन
एशिया के विभिन्न बौद्ध देशों की एक संयुक्त पहल है। इसमें न केवल भिक्षुगण, बल्कि शांतिप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान और राजनीतिक हस्तियाँ भी भाग लेते हैं।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युद्ध, हिंसा और परमाणु हथियारों का विरोध करके शांतिपूर्ण
सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म पर आधारित करुणा, मैत्री और अहिंसा के आदर्शों को वैश्विक स्तर पर
स्थापित करना भी है। एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों में
राष्ट्रों के बीच पारस्परिक मैत्री और सहयोग बढ़ाना, गरीबी, अशिक्षा, जातीय विभाजन
जैसी समस्याओं का मिलकर समाधान करना, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के पक्ष में आवाज़ उठाना, निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के विरुद्ध
जनजागृति फैलाना आदि शामिल हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से एशियाई देशों ने आपसी
संबंधों को मज़बूत करने और बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं को आधुनिक विश्व की चुनौतियों
से जोड़ने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में, एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन केवल एक धार्मिक समागम
नहीं, बल्कि विश्व
शांति, सामाजिक न्याय
और सह-अस्तित्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
• यद्यपि भारत
में बीसवीं शताब्दी से पहले भी महत्वपूर्ण बौद्ध सम्मेलन हुए हैं, फिर भी बीसवीं शताब्दी के बाद और भी महत्वपूर्ण
सम्मेलन हुए हैं, जिनमें 1956
में बोधगया में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके
बाद, 2011, 2014, 2019 और 2023 में नई दिल्ली, बोधगया, साँची, सारनाथ आदि स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित
किए गए, जिनका मुख्य
उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक विश्व शांति, धार्मिक सह-अस्तित्व और सांस्कृतिक सद्भाव से
जोड़ना था।
• संघर्ष
समाधान एवं शांति अध्ययन केंद्र (Centre for Conflict Resolution and Peace Studies) – विश्व में संघर्ष
समाधान के तरीकों का अध्ययन और विकास, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, शैक्षिक और नीति निर्माण में योगदान, समाज में सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देना आदि
उद्देश्यों के साथ 2 अक्टूबर 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय में संघर्ष समाधान एवं
शांति अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई थी। यह केंद्र शांति निर्माण पर पाठ्यक्रम, शोध परियोजना आदि का संचालन करती हैं और संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है। इसके साथ साथ यह केंद्र क्षेत्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है।
• श्रीलंका
में सर्वोदय श्रमदान आंदोलन: यह 1958 में डॉ. ए.टी. अरियारत्ने द्वारा
श्रीलंका में शुरू किया गया एक सामुदायिक विकास और सामाजिक परिवर्तन अभियान है। यह
आंदोलन गांधीवादी विचारधारा के साथ-साथ बौद्ध दर्शन से भी गहराई से प्रभावित है।
बौद्ध शिक्षाओं के महान सिद्धांत जैसे अहिंसा, करुणा, दान और चार अपरिमेय भावनाएँ (मैत्री, करुणा, समता और उपेक्षा) सामुदायिक विकास और संघर्ष समाधान में
उपयोग की गईं। यह आंदोलन सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और सहयोग की भावना पर बल देता है। इसने
गृहयुद्ध के दौरान अलग हुए विभिन्न जातीय समुदायों के बीच संवाद और मेल-मिलाप
स्थापित किया, जिससे स्थानीय
स्तर पर शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा मिला।
• दलाई लामा
और मध्य मार्ग: 1950 में चीनी जन मुक्ति सेना द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण करने
के बाद से, तिब्बत के
विश्व-प्रसिद्ध धार्मिक नेता दलाई लामा, तिब्बतियों की पहचान और स्वायत्तता की रक्षा के लिए अहिंसक
प्रथाओं और मध्य मार्ग को अपनाकर एक न्यायसंगत समाधान की तलाश में रहे हैं। दलाई
लामा के प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थायी शांति स्थापना और मानवाधिकार
संरक्षण का एक उदाहरण स्थापित किया है। चीन के साथ संघर्ष के दौरान शांति स्थापित
करने और विश्व में शांति एवं सद्भाव स्थापित करने के उनके अद्वितीय प्रयासों के
लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बौद्ध दर्शन
पर आधारित शांति स्थापित करने के उनके प्रयासों और सभी जीवों के प्रति उनकी करुणा
ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया है।
• म्यांमार
में भिक्षुओं द्वारा संचालित सुधार आंदोलन: म्यांमार में बौद्ध धर्म प्रमुख
धर्म बना हुआ है। देश की राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, औपनिवेशिक शासन द्वारा उत्पीड़न और सामाजिक
असमानता को दूर करने में भिक्षुओं की अग्रणी भूमिका रही है। जैसे ब्रिटिश
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन, 8 अगस्त 1988
को तत्कालीन सैन्य शासन के विरुद्ध लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के पक्ष में आंदोलन
आदि। संघर्ष के बाद बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना शांति और पुनर्निर्माण का मुख्य
आधार बनी। अहिंसा, समानता, करुणा, क्षमा, मेल-मिलाप, ध्यान आदि बौद्ध सिद्धांतों ने कंबोडिया में
शांति स्थापित की। वहाँ के बौद्ध मठों ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई।
• इंडोनेशिया
- योग्याकार्ता वक्तव्य (Yogyakarta Statement) -
योग्याकार्ता सम्मेलन 2015 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। 3 और 4 मार्च, 2015 को जकार्ता और
बोरोबुदुर मंदिर में आयोजित बौद्ध और मुस्लिम धार्मिक नेताओं के एक विशेष सम्मेलन
में धार्मिक अतिवाद और हिंसा को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों की घोषणा जारी की
गई, जिसे योग्याकार्ता वक्तव्य के नाम से जाना जाता
है। इस घोषणा के माध्यम से, बौद्ध और मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने एक स्पष्ट
संदेश दिया और धार्मिक अतिवाद को अस्वीकार करने और न्यायपूर्ण शांति के लिए मिलकर
काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, अर्थात धर्म का
उपयोग हिंसा के लिए नहीं, बल्कि शांति और न्याय के लिए किया जाएगा। यह
सम्मेलन केवल एक औपचारिक सम्मेलन नहीं था, बल्कि भविष्य
में सर्वधर्म सद्भाव और विश्व शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।
• वियतनाम - थिच न्हात हान और 'संलग्न बौद्ध
धर्म': प्रसिद्ध वियतनामी बौद्ध भिक्षु थिच न्हात हान (Thich Nhat Hanh) ने 'संलग्न बौद्ध
धर्म' (Engaged Buddhism) की अवधारणा
प्रस्तुत की और विश्व शांति, सामाजिक सक्रियता और पर्यावरणीय न्याय पर ध्यान
केंद्रित किया। उन्होंने ध्यान और करुणा को सामाजिक आंदोलनों से जोड़कर अहिंसक
समाधान और सतत विकास के लिए काम किया है।
सक्रिय बौद्ध
धर्म, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु बौद्ध धर्म
की ध्यान, करुणा और अहिंसा की शिक्षाओं को सीधे लागू करने
का अभ्यास है। इस अवधारणा को बीसवीं शताब्दी के मध्य में प्रसिद्ध वियतनामी बौद्ध
भिक्षु थिच न्हात हान ने लोकप्रिय बनाया था। इसके मुख्य विचार इस प्रकार हैं:
1. दैनिक जीवन में ध्यान और सचेतनता को लागू करना, अर्थात केवल ध्यान में बैठना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक गतिविधि के प्रति सजग और करुणामय दृष्टिकोण
अपनाना।
2. सामाजिक न्याय और शांति में सक्रिय भूमिका निभाना।
3. अहिंसक रूप से संघर्षों का समाधान करना, अर्थात संघर्षों के मूल कारणों का पता लगाना और संवाद, सुलह और सहयोग के माध्यम से समाधान खोजना।
4. पर्यावरण
संरक्षण पर ध्यान देना।
थिच न्हात हान के अनुसार, यदि हम ध्यान
का उपयोग केवल अपनी मानसिक शांति के लिए करते हैं, तो यह केवल आधा
उपयोग है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों के दुखों को कम करना और समाज को अधिक
न्यायपूर्ण बनाना है। इसलिए, सक्रिय बौद्ध धर्म आधुनिक समाज में आध्यात्मिकता
और सामाजिक उत्तरदायित्व को जोड़ने वाले एक सेतु की तरह है। आज की जटिल दुनिया में, सक्रिय बौद्ध अभ्यास संघर्ष समाधान, मानवाधिकार और
समानता, जलवायु परिवर्तन, मानसिक
स्वास्थ्य (ध्यान और ध्यान साधना के माध्यम से तनाव, उदासी और क्रोध
को कम करने की अवधारणा), अंतर्धार्मिक संवाद (विभिन्न धर्मों के लोगों के
बीच सहिष्णुता और सहयोग का वातावरण बनाना) आदि क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध
हुए हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान, थिच न्हात हान और उनके अनुयायियों ने युद्ध के
विरुद्ध अहिंसक अभियानों, शरणार्थियों के बचाव और पुनर्निर्माण में
प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर अपने उद्देश्य को पूरा किया। इसी प्रकार, श्रीलंका और कंबोडिया में गृहयुद्धों के बाद, बौद्ध भिक्षुओं ने सामुदायिक पुनर्निर्माण और सुलह के लिए
सक्रिय बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी देशों में माइंडफुलनेस-आधारित तनाव न्यूनीकरण
कार्यक्रमों ने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे सक्रिय बौद्ध धर्म के लिए प्रेरणा माना जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, थाईलैंड में, बौद्ध भिक्षुओं
ने जंगलों को बचाने के लिए 'वृक्ष अभिषेक' जैसे
प्रतीकात्मक अभियान चलाए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध-मुस्लिम सुलह
परियोजनाओं ने अंतर्धार्मिक संवाद के माध्यम से हिंसक संघर्ष को कम करने में
योगदान दिया है।
कुछ सीमाओं के बावजूद, सक्रिय बौद्ध
धर्म ने अब तक कई सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। संघर्ष समाधान, मानसिक स्वास्थ्य सुधार, पर्यावरण
संरक्षण और अंतरधार्मिक संवाद में। लेकिन इसका पूर्ण उद्देश्य (विश्व शांति, अन्याय का अंत और सभी संघर्षों का समाधान) अभी तक प्राप्त
नहीं हुआ है।
• नेपाल - यद्यपि नेपाल बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा
बुद्ध की जन्मभूमि है, फिर भी कुछ वर्ष पूर्व तक इसे एक हिंदू राष्ट्र
के रूप में जाना जाता था। हालाँकि, समय-समय पर (1986, 1998,
2011, 2016, 2018, 2019, 2022, आदि में) लुम्बिनी और काठमांडू आदि में बौद्ध
शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि
लुम्बिनी को विश्व से परिचित कराना और बौद्ध शिक्षाओं को विश्व शांति और मानवीय
मूल्यों से जोड़ना था। 5 मार्च, 2025 को अखिल नेपाल
भिक्षु महासंघ द्वारा आयोजित चतुर्थ त्रिपिटक पाठ समारोह में भाग लेने वाले
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध गुरुओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण की अपनी
कामनाओं से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस समारोह में नेपाल, भारत, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया और जापान सहित 16 देशों के लगभग
दो हज़ार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भाग लिया।
• भूटान और
सकल राष्ट्रीय खुशी - हाल ही में, कुछ साल पहले, भूटान ने 'सकल राष्ट्रीय खुशी' (GNH) नामक एक
अवधारणा विकसित की। GNH एक ऐसी पद्धति है जो किसी
देश की समग्र खुशी, मनोबल, सामाजिक रूप से
समावेशी विकास, सामुदायिक जीवन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि
के विभिन्न पहलुओं को मापने का प्रयास करती है। जहाँ अन्य देश सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को देश के विकास का सूचक मानते हैं, वहीं भूटान GNH को विकास के सूचक के रूप में उपयोग करता है। भूटान मुख्यतः
बौद्ध देश है। तदनुसार, यह अवधारणा बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों से
गहराई से जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म करुणा, अहिंसा, ध्यान, आत्म-संयम, आत्म-संतुष्टि
और सतत कल्याण पर जोर देता है। ये सभी मूल्य खुशी सूचकांक के चार मुख्य स्तंभों के
अनुरूप हैं: सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक
संरक्षण और सुशासन। आज, विश्व खुशी रिपोर्ट रिपोर्ट आंशिक रूप से भूटान
की जीएनएच अवधारणा से भी प्रभावित है। लेकिन अधिकांश यूरोपीय देशों को इस रिपोर्ट
में शीर्ष स्थान दिया गया है।
• आंतरिक शांति: व्यक्तिगत और सामुदायिक
स्तर पर, बौद्ध ध्यान (माइंडफुलनेस) अभ्यास ने तनाव, क्रोध और हिंसा को कम करके संघर्ष को रोकने में मदद की है।
उदाहरण के लिए, आधुनिक चिकित्सा और शांति शिक्षा कार्यक्रमों
में इसका उपयोग बढ़ रहा है जिससे जेलों, स्कूलों और
युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हिंसा में कमी आई है। यह संघर्ष के मूल कारणों का
समाधान करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, जिसे बौद्ध
दर्शन 'आंतरिक शांति' से 'बाह्य शांति' के रूप में वर्णित करता है।
ये केवल प्रतिनिधि उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि बौद्ध
शिक्षा के मूल्यों और प्रथाओं को अपनाकर दुनिया में शांति और सुलह की पहल संभव है।
विश्व शांति को
बढ़ावा देने के लिए सुझाव:
1. शैक्षिक नीति में बदलाव: सरकार शिक्षा नीति में अहिंसा और
शांति शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर सकती है।
2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: देशों के बीच शांति शिक्षा में
आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाया जा सकता है।
3. सामुदायिक कार्यक्रम: स्थानीय स्तर पर बौद्ध सिद्धांतों पर
आधारित शांति शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
4. शोध: बौद्ध शांति शिक्षा की प्रभावशीलता पर और शोध किया जा
सकता है और इसे आधुनिक संदर्भ में लागू किया जा सकता है।
निष्कर्ष:
आज की दुनिया में, बौद्ध शिक्षाओं
को व्यवहार में लाकर शांति निर्माण में योगदान देने की संभावनाएँ हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चूँकि बौद्ध शिक्षाएँ आंतरिक
शांति और करुणा पर ज़ोर देती हैं, इसलिए व्यक्तियों में संघर्ष से निपटने की
क्षमता बढ़ती है। विभिन्न देशों के धार्मिक नेता और संगठन अंतर्धार्मिक संवाद और
सामूहिक परियोजनाओं का समर्थन कर रहे हैं। 2015 के
योग्याकार्ता वक्तव्य को इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। थिच न्हात हान
जैसे नेताओं ने ध्यान साधना के माध्यम से समाज में अहिंसा और करुणा के बीच संबंध
को दर्शाने का काम किया है। इसी प्रकार, स्थानीय बौद्ध
संगठन पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और सामुदायिक विकास में शांति और
सद्भाव परियोजनाएँ सक्रिय रूप से चला रहे हैं। हालाँकि, बौद्ध शांति
दर्शन को व्यावहारिक रूप से लागू करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं। धार्मिक शांति
निर्माण एक अस्पष्ट अवधारणा है और इसमें कई जोखिम हैं। धार्मिक नेताओं का अपने
समुदायों में सीमित प्रभाव, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
राज्य-स्तरीय वार्ता और उच्च-स्तरीय चर्चाओं की अक्षमता, और आधुनिक
वैज्ञानिक जगत में प्राचीन धार्मिक सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए, यह कठिन प्रश्न, कई प्रश्न खड़े
करते हैं। इससे अन्य धर्मों के साथ वैचारिक संघर्ष भी हो सकते हैं। इसके अलावा, लोगों को ध्यान और करुणा साधना में संलग्न होने के लिए समय
और इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, जो व्यस्त आधुनिक जीवनशैली में चुनौतीपूर्ण हो
सकता है। इन कठिनाइयों के बावजूद, बौद्ध शिक्षाओं के आदर्शों और प्रथाओं को, जो दुख के मूल कारणों का विश्लेषण करके और उसके अंत का
मार्ग दिखाकर, नकारा नहीं जा सकता, और शांति की
संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। यदि धार्मिक नेता और साधक मिलकर काम करें, तो बौद्ध शिक्षाओं का उपयोग समकालीन संघर्षों को सुलझाने
में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
**************************************************************************
संदर्भ:
1. राव, चौडूरि
उपेन्द्र, 2013. पालि भाषा, बौद्धधर्म (दर्शन, साहित्य तथा संप्रदाय), शेरब
जांग्पो सोसायटी, नई दिल्ली
2.
रावल, ललिजन (अनु.), वि.स. २०७६. गौतम बुद्ध, बौद्ध
दर्शन (मूल लेखक- राहुल सांकृत्यायन), इन्डिगो इन्क प्रा.लि., काठमाडौँ
3.
सिंह, हरिश्चन्द्र लाल, The Dhammapada/धम्मपद, सुखी होतु नेपाल/बुद्ध बिहार,
भृकुटीमण्डप, काठमाडौँ
4.
स्थविर, भिक्षु संघरक्षित, मई 2011, बुद्ध र बुद्ध धर्म,
सत्यसन्देश प्रचारक प्रकाशन, काठमाडौँ
5.
कोण्डन्य, 2011, शान्तिका लागि हात मिलाऔँ, बुद्ध र
शान्ति शिक्षा, मोतीलाल शिल्पकार, जावलाखेल, ललितपुर
6.
घिमिरे, पशुपति, 2013, के थिए त आधारभूत बौद्ध शिक्षाहरू ?, बौद्धवादका तीन आयाम (ISBN:
978-9937-2-6933-9), प्र. बुद्धिसागर घिमिरे
प्रमुख अनलाइन स्रोत:
Academy of Management
Information and Decision Sciences. (2021). Buddhist education: The noble
path to peace. Journal of Management Information and Decision Sciences,
24(6S). https://www.abacademies.org/articles/buddhist-education-the-noble-path-to-peace-12878.html
Aich, T. K. (2013).
Buddha philosophy and western psychology. Indian Journal of Psychiatry, 55(Suppl.
2), S165–S170. https://doi.org/10.4103/0019-5545.105534
Frydenlund, I., &
Hayward, S. (2015, May 19). The Buddhist face of peace: Buddhist peace
initiatives in times of religious intolerance. Peace Research Institute
Oslo (PRIO). https://www.prio.org/comments/342
Human Rights Watch.
(2009, September 22). The resistance of the monks: Buddhism and activism in
Burma. https://www.hrw.org/report/2009/09/22/resistance-monks/buddhism-and-activism-burma
Institute for Economics
& Peace. (2024). Global Peace Index. https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
Kumbhar, S. (n.d.). Peace
and conflict resolution: Indian perspectives. https://jndmeerut.org/wp-content/uploads/2024/01/6-3.pdf
MGIMO University.
(2022). Asian Buddhist Conference for Peace. https://concept.mgimo.ru/jour/article/view/901
Nobel Prize Outreach
AB. (1989). The Nobel Peace Prize 1989: The 14th Dalai Lama – facts. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1989/lama/facts/
PWOnlyIAS. (2025). World
Happiness Report 2025. https://pwonlyias.com/world-happiness-report-2025/
Sustainable Development
Solutions Network. (n.d.). World Happiness Report: Analysis. https://www.worldhappiness.report/analysis/
Tiwary, K. N. (2023).
Buddhism and non-violence: Exploring the relationship between Buddhist
teachings and conflict resolution. ShodhKosh: Journal of Visual and
Performing Arts. https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v4.i1
.png)