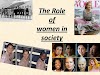ममता कालिया का ‘दौड़’ उपन्यास: आजीविकावाद संदर्भ
प्रदुन
कुमार
शोधार्थी,
केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय
Pradunkumar.2300807016@cukerala.ac.in
प्रस्तावना
हिंदी
उपन्यास परंपरा ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से अनेक सामाजिक,
आर्थिक
और सांस्कृतिक विमर्शों को अपनी कथावस्तु का केंद्र बनाया है। बदलते सामाजिक
परिदृश्य, परिवारिक
संबंधों, स्त्री-जीवन
की जटिलताओं और रोज़गार–संघर्षों को हिंदी उपन्यासकारों ने गहराई से चित्रित किया
है। इसी क्रम में ममता कालिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे हिंदी की उन
रचनाकारों में हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन की पेचीदगियों,
स्त्री-जीवन
की विडंबनाओं और रोज़गार की निरंतर भागदौड़ को कथा का आधार बनाया। इनमें खासकर दौड़
उपन्यास ने हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया है। ‘दौड़’
उपन्यास बाज़ार के दबाव और आजीविकावाद से जनित सांस्कृतिक विघटन, संबंधों
के विघटन और मानवीय भावनाओं की क्षति का यथार्थ चित्रण करता है। इसमें
आजीविका-संबंधित दौड़ का बारीकी से विश्लेषण देखने को मिलता है।
ममता कालिया का उपन्यास 'दौड़'
आधुनिक
भारतीय मध्यमवर्गीय समाज में आजीविका की चुनौतियों का सशक्त चित्रण करता है। यह
शोध आलेख उपन्यास में आजीविका के प्रश्नों की पड़ताल करता है,
जिसमें
बाजारवाद, आर्थिक
उदारीकरण, और
युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं का विश्लेषण किया गया है।
बीज शब्द :
जीविका, आजीविका,
रोजगार,
प्रतिस्पर्धा,
जीविकोपार्जन
क्षेत्र में स्त्री,
तनाव,
वृद्ध विमर्श, पलायन,
विस्थापन,
पारिवारिक संबंध,
नौकरी में असुरक्षा।
मूल
आलेख
व्यक्ति
अपनी और परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी जीविका उपार्जित करता
है। आजीविकवाद को समझने से पहले हमें आजीविका को समझना होगा। जीविका व आजीविका में
काफी समानता है,
किन्तु कुछ सूक्ष्म अंतर भी है। जीविका वह प्रक्रिया या साधन है जिसके द्वारा
व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये आमतौर पर भौतिक संसाधनों,
काम धंधों या व्यवसाय से संबन्धित होता है। जीविका न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति करता
है तथा इसका दृष्टिकोण सीमित रहता है। अर्थात ये वर्तमान को देखते हुए कार्यान्वित
किया जाता है। भविष्य की चिंता नहीं होती
है। इसमें नियमितता नहीं होती है। जैसे की दिहारी मजदूर,
खेती आदि। “जीविका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग रूप में विशिष्ट होती है तथा उनमें
बदलाव भी आता रहता है।”[1]
वहीं दूसरी ओर आजीविका केवल जीविका अर्जित करने का साधन नहीं है बल्कि स्थिरता,
सामाजिक सुरक्षा,
सम्मान जनक जीवन स्तर और दीर्घकालिक आय के स्त्रोत भी शामिल होते हैं। जैसे शिक्षक,
कृषि
प्रसंस्करण आदि। यहाँ कृषि प्रसंस्करण से तात्पर्य है जब किसान कृषि उपज की सेल्फ
लाइफ बढ़ता है ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो और बाजार में बेचा जा सके। जबकि
सामान्य खेती में किसान फसल की सेल्फ लाइफ की और ध्यान नहीं देता वह वर्तमान में
उस फसल का क्या करना है उसपर ध्यान देता है। इस संबंध में खान सर का कथन है,
“कोई पकोड़ा तल रहा है या चोरी कर रहा है तो वह उसकी जीविका है रोजगार या आजीविका नहीं।”[2]
भारत में जीविकोपार्जन
हेतु कई माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। PLFS
2023-24 के अनुसार,
कुल
श्रम शक्ति लगभग 58 करोड़
है। क्षेत्रवार, कृषि
में 46.1% श्रमबल
कार्यरत है, जो
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। उद्योग (विनिर्माण) में 11.4%,
सेवा
में 28.9%, और
निर्माण में 13.6%।
रोजगार स्थिति के अनुसार, कुल
कार्यबल का 58.4% स्वरोजगार
में लगा हुआ है, जिसमें
स्व-खाता कार्यकर्ता, नियोक्ता
और पारिवारिक सहायक शामिल हैं। नौकरी करने वाले केवल
21.7% हैं, जबकि
कैजुअल लेबर 19.9% है।
यह दर्शाता है कि स्वरोजगार प्रमुख है, लेकिन
नौकरी आधारित रोजगार की गुणवत्ता और वृद्धि की आवश्यकता है। स्वरोजगार में महिलाओं
का हिस्सा 67% तक
पहुंच गया है, जो
आर्थिक आत्मनिर्भरता का संकेत है।
|
श्रेणी |
रोजगार प्रतिशत (%) |
अनुमानित रोजगार संख्या (करोड़ में) |
टिप्पणी |
|
क्षेत्रवार |
|||
|
कृषि |
46.1 |
26.7 |
ग्रामीण
आजीविका का मुख्य स्रोत; 70% ग्रामीण
परिवार निर्भर। |
|
उद्योग
(विनिर्माण) |
11.4 |
6.6 |
वृद्धि
की क्षमता लेकिन कम रोजगार सृजन। |
|
सेवा |
28.9 |
16.8 |
आईटी,
खुदरा
और वित्तीय सेवाओं से प्रेरित। |
|
निर्माण |
13.6 |
7.9 |
बुनियादी
ढांचा परियोजनाओं से वृद्धि। |
|
कुल |
100 |
58 |
- |
|
रोजगार
स्थिति |
|
||
|
स्वरोजगार |
58.4 |
33.9 |
मुख्य
रूप से कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र; महिलाओं
में 67%। |
|
नौकरी/वेतनभोगी |
21.7 |
12.6 |
शहरी
क्षेत्रों में अधिक; औपचारिक रोजगार। |
|
कैजुअल
लेबर |
19.9 |
11.5 |
दैनिक
मजदूरी;
कम
आय और असुरक्षा। |
|
कुल |
100 |
58 |
- |
सारणी
1
ऊपर दिए गए सारणी
में क्षेत्रवार वितरण 2023-24
डेटा के अनुसार
दिया गया है। दूसरा सारणी रोजगार स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें स्वरोजगार, नौकरी तथा श्रमिकों के रोजगार संख्या को दिखाता है।
समय
के साथ आजीविका केवल भौतिक आवश्यकता तक सीमित न रहकर,
सामाजिक – सांस्कृतिक पहलुओं से भी जुड़ने लगी। एक व्यक्तिगत क्रिया न रहकर एक
विचारधारा के रूप में सामने आने लगी। आज आजीविका हमारी सामाजिक पहचान का निर्धारण
करती है। इसलिए भले इंजीनियर बन कर कम तंख्वाह मिले और ऑटो रिक्शा चलाकर ज्यादा,
लेकिन व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहेगा। आजीविकवाद के संबंध में ममता कालिया लिखती
हैं, “व्यावसायिकता से
आजीविकवाद (केरियारिज़्म) पैदा होता है और यह आजीविकवाद पारिवारिक सम्बन्धों को और
सम्बन्धों की भावात्मक्ता,
आत्मीयता आदि को नष्टप्राय कर देता है।”[3]
आजीविकावाद का अभिप्राय है, मानवीय
अस्तित्व में आजीविका (रोज़गार,
करियर,
आर्थिक सुरक्षा) को सर्वोपरि मानना और नैतिक, सांस्कृतिक
मूल्यों की अपेक्षा सिर्फ अर्थ की ओर झुकाव।
आधुनिक हिंदी साहित्य, विशेषकर
1980 के बाद,
जब
भारत में बेरोज़गारी, अस्थायी
नौकरियाँ और निजीकरण का दौर तेज़ हुआ, तब
उपन्यासकारों ने आजीविका के प्रश्न को अपनी रचनाओं में गहराई से उकेरा। ‘दौड़’ इसी
परंपरा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।
‘दौड़’
के पात्र नौकरी की असुरक्षा से निरंतर जूझते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी
स्थायी नौकरी मिलना कठिन हो जाता है। जिनके पास नौकरी है,
वे
भी भविष्य की अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। उपन्यास में पात्रों की चिंता केवल
वेतन पाने की नहीं है, बल्कि
स्थायी पद पाने की है। प्राइवेट कंपनियां कम वेतन देकर ज्यादा काम चाहती है। उपन्यास
के शुरू में ही जब चित्रेश दो जंप्स वेतन वृद्धि मांगता है कंपनी उसे जंप आउट करना
ही बेहतर समझती है। कॉरपोरेट सेक्टर में जुबान खोलने पर,
वृद्धि मांगने पर या कंपनी में घाटा होने पर कंपनी के पास सबसे प्राथमिक उपाय
नौकरी से निकालना होता है। अभिषेक ने कहा,
“निजी
सेक्टर में सबसे खराब बात यही है,
नथिंग इस ऑन पेपर,
एमडी ने कहा घाटा है तो मानना पड़ेगा की घाटा है। पब्लिक सेक्टर में कर्मचारी सर पर चढ़ जाते हैं पाई-पाई
का हिसाब दिखाना पड़ता है।”[4]
भूमंडलीकरण
के बाद से जब से बाजारवाद,
उपभोक्तावाद आया है,
तब से देखा जाए तो वर्तमान समय में आज इतनी प्रतिस्पर्धा बन गई है नौकरी के
क्षेत्र में इतनी असुरक्षा है कि व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है कि कब उसकी नौकरी
चली जाएगी? इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे आधुनिक तकनीक के
साथ व्यक्ति अपने आप को संतुलित नहीं कर पाया,
तकनीक के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाया या फिर आज नौकरियां कम है और बेरोजगार
ज्यादा। अनुपम जो इस कंपनी में काम करता था उसे बस यह कहकर निकाल दिया गया की
कंपनी घाटे में चल रही है। ममता कालिया लिखती हैं,
“उपभोक्तावादी
समय में एक अच्छी आजीविका प्राप्त करना जितना बड़ा उद्देश्य है। उस आजीविका के
स्रोत को सुरक्षित रखना उससे बड़ी चुनौती है।”[5]
पुरुषों
की तरह स्त्रियाँ भी नौकरी की असुरक्षा से जूझती हैं,
लेकिन
उनके लिए यह असुरक्षा और भी गंभीर हो जाती है। अस्थायी नौकरी की स्थिति में सबसे
पहले स्त्रियों की नौकरी खतरे में पड़ती है। विवाह और मातृत्व की ज़िम्मेदारियाँ
स्त्रियों की पेशेवर यात्रा में अवरोध उत्पन्न करती हैं। महिलाओं को मातृत्व लाभ
अधिनियम 1961 के तहत कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं जिसके अनुसार महिलाएं गर्भवती
अवस्था अथवा बच्चों के पालन पोषण के लिए छुट्टियां ले सकती हैं लेकिन कुछ कंपनियां
इसे मानने से इंकार करती है अथवा कुछ ऐसी स्थिति कायम कर देती हैं जिससे वह स्त्री
खुद ही काम छोड़कर चली जाए कुछ ऐसी स्थिति यहां पर राजुल के साथ होती है।
राजुल
एक विज्ञापन कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद कंपनी को लगा कि राजुल के
पारिवारिक जिम्मेदारियों का प्रभाव कंपनी के काम पर पड़ेगा। इसलिए कंपनी उसे
निकालना चाहती थी। “उसकी विज्ञापन एजेंसी मानती थी कि घर और दफ्तर दोनों मोर्चे
संभालना लड़कियों के बस कि बात नहीं।”[6]
गर्भवती अवस्था में राजुल को कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक कार्यभार सोपा गया ताकि
वह स्वयं नौकरी छोड़ दे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राजुल ने विज्ञापन कंपनी से
त्यागपत्र दे दिया।
उपन्यास
का दूसरा बड़ा पक्ष बेरोज़गारी और प्रतिस्पर्धा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी
युवा नौकरी पाने के लिए दर-दर भटकते हैं। नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का
दबाव और उसमें असफल होने की आशंका उन्हें मानसिक रूप से थका देती है। वर्तमान की
दौड़ में उनकी डिग्रियाँ भी रोजगार की गारंटी नहीं देतीं। मध्यवर्गीय समाज में
नौकरी केवल आर्थिक साधन नहीं है, बल्कि
सामाजिक मान्यता का प्रतीक भी है। परिवार के भीतर भी उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती
है। माता-पिता और रिश्तेदारों की अपेक्षाएँ उसे और अधिक बोझिल बना देती हैं। पवन
कहता है, “जब
यहाँ सुख से रहता था तब भी तो आप लोग दुखी थे। आपने कहा था मां की आपके बड़े बाबू
के लड़के तक ने एमबीए प्रवेश परीक्षा पास कर ली। उस दिन मुझे कैसा लगा था। आपके
सपने मेरा संघर्ष बन गए।”[7]
क्या यहां पर केवल बेटा ही गलत था?
माता-पिता ने बचपन से दूसरों के साथ तुलना की। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है मतलब
तुम सफल नहीं हो। यानी वर्तमान समय में सफलता को नौकरी से ही आंका जाता है।
आजीविका
की इस निरंतर दौड़ में व्यक्ति के जीवन-मूल्य और रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। प्रतिस्पर्धा
और असुरक्षा का दबाव पात्रों को स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बना देता है। आजीविका के
संघर्ष ने आधुनिक समाज के नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित किया है। नौकरी पाने या
सुरक्षित रखने के लिए लोग अनुचित साधनों का सहारा लेने लगते हैं। उपन्यास के पात्र
भी इस विडंबना से अछूते नहीं हैं। वे परिस्थितियों के दबाव में कई बार अपने
सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि नौकरी की दौड़ केवल
आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि
यह व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता की परीक्षा भी है। क्या बाजार के इस मोड़ पर
नैतिकता का सवाल उठाए जा सकता है? राजुल
के ऐसा सवाल उठाने पर अभिषेक भड़क उठता है। “सीधा-साधा एक प्रोडक्ट बेचना है इसमें
तुम नैतिकता और सच्चाई जैसे सवाल मेरे सिर पर दे मार रही हो। बाजार के अर्थशास्त्र
में नैतिकता जैसा शब्द लाना कंफ्यूजन है। मैं अब तक पाँच सौ किताबें तो मैनेजमेंट
और मार्केटिंग पर पढ़ी होगी और उसमें नैतिकता पर कोई चैप्टर नहीं है।”[8]
वर्तमान
समय में युवाओं का कामयाबी के प्रति दृष्टि में बदलाव देखने को मिलता है। जहां
उनका मानना है कि जितना नौकरी बदलेंगे,
उतनी कामयाबी मिलेगी। अपने अन्य कामयाब साथियों की तरह ही पवन ने भी यही सोचा था
कि अगले साल कंपनी ने उसे उच्चतर ग्रेड अगर नहीं दिया तो वह कंपनी छोड़ देगा। जहां
हर महीने वेतन मिले वही जगह अपनी होती है इस वाक्य को मंत्र की तरह जीती एक युवा
पीढ़ी है जो बढ़ते बाजार में खड़ी है। इस बाजार में आकांक्षाएं हैं,
भारी भरकम वेतन प्राप्त करने की लालसा हैं,
खुद को साबित करने का जुनून है और हर क्षण में जीने की जिद्द है। यहां शहर का अर्थ
केवल रोजगार में खुलता है। यहां स्मृतियां एकदम व्यर्थ है और सपने सिर्फ तरक्की से
जुड़े हैं। पवन कहता है, “सच
तो यह है पापा जहां हर महीने वेतन मिले वही जगह अपनी होती है और कोई नहीं।”[9]
‘दौड़’
उपन्यास में स्त्री पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आजीविका का प्रश्न
स्त्री के लिए पुरुष से कहीं अधिक जटिल है। स्त्रियों के संदर्भ में आजीविका का
संघर्ष और भी गहन है। नौकरी करने वाली स्त्री को घर और बाहर दोनों का संतुलन बनाए
रखना पड़ता है। उसे नौकरी की असुरक्षा के साथ-साथ लैंगिक भेदभाव,
पारिवारिक
दबाव और सामाजिक पूर्वाग्रहों से भी जूझना पड़ता है। उपन्यास में स्त्री पुरुष
सबके संघर्ष को दिखाया गया है कि किस प्रकार से वह कार्यस्थल पर संघर्ष कर रहे हैं।
तथा किस प्रकार से पारिवारिक और कामकाजी जीवन के मध्य संतुलन बैठाने में संघर्ष कर
रहे हैं।
उपन्यास
के माध्यम से देखने को मिलता है कि कैसे आर्थिक आत्मनिर्भरता स्त्री के लिए मुक्ति
का माध्यम हो सकता है। स्टेला और राजूल दोनों आत्मनिर्भर है। स्टेला ने पारिवारिक
ज़िम्मेदारी के कारण अपने बिजनेस को बंद नहीं किया। लेकिन राजूल ने परिवार को
संभालने के लिए,
उसकी जिम्मेदारियां को निभाने के लिए नौकरी छोड़ दी और बाद में उसकी ग्लानि उसके
हृदय में रह गई कि उसे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी या
परिवार की जिम्मेदारी केवल स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है। राजुल कहती है,
“हिंदुस्तानी मर्द को शादी के सारे सुख चाहिए बस जिम्मेदारी नहीं। मेरा कितना हर्ज
हुआ। अच्छी भली सर्विस छोड़ने पर मेरी सब कलीग्स कहती थी राजूल शादी करके अपनी
आजादी चौपट करोगी। आजकल तो डिंक्स का जमाना है ‘डबल
इनकम नो किड्स’।”[10]
स्त्री और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी है। पुरुष इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
पुष्पपाल सिंह लिखते हैं,
“पत्नी का पेशा किसी भी कॉल गर्ल से कम नहीं,
कॉल गर्ल के पास यह छूट होती है कि वह हर कॉल पर प्रस्तुत न हो,
पर पत्नी के पास या विकल्प भी नहीं होता।” [11]
उपन्यास
में कई प्रसंग ऐसे हैं जहाँ पात्र केवल जीविका की चिंता से नहीं,
बल्कि
पारिवारिक दबाव से भी जूझते दिखाई देते
हैं। आर्थिक असुरक्षा और जीविका की चिंता रिश्तों को भी प्रभावित करती है। उपन्यास
में परिवार के भीतर तनाव अक्सर नौकरी और आय के कारण उत्पन्न होता है। बेरोज़गारी
की स्थिति में रिश्तेदार व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं। पति-पत्नी के
संबंधों में भी नौकरी और वेतन का अंतर टकराव का कारण बनता है। ममता कालिया ने यह
दिखाया है कि जब जीविका ही अस्थिर हो, तो
रिश्तों का स्थायित्व भी डगमगा जाता है। ममता कालिया लिखती हैं,
यह
पीढ़ी अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों को भी करियर की भेंट चढ़ा चुकी है। अपने
विवाह को लेकर पवन कहता है, “हमारे
एजेंडा पर बहुत सारे काम है शादी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा तीन दिन चार दिन खाली
रख सकते हैं।”[12]
नौकरी
या जीविका जब तक साधन के रूप में होती है तो आसपास के सभी चीजों के साथ संतुलन
बैठाना चाहती है,
लेकिन जिस दिन उसने साध्य का रूप धारण कर लिया तो युवा का पूरा ध्यान केवल और केवल
अपनी जीविका उन्नति,
अपने भविष्य की ओर तथा अपने करियर की ओर चला जाता है। उसके बीच में आने वाली सभी
चीज उसे एक बंधन जैसा महसूस करवाते हैं,
एक रुकावट सा महसूस करवाती हैं। “साध्य
और साधन के बीच असंतुलन तथा असमंजस व्यक्ति के जीवन में तनाव को जन्म दे रहा है।”[13]
इस
उपन्यास में हम ऐसे ही पारिवारिक संबंधों को बदलते हुए देखते हैं जहां जीविका
क्षेत्र में आने वाली या फिर तरक्की के बीच में आने वाली चीज रुकावट मान ली जाती
है। जब पिता द्वारा पवन से यह कहा जाता है कि बेटा नौकरी यहीं इलाहाबाद में ही ले
लो ना। तुम इतनी दूर चले गए हो। अब हम बूढ़े बुजुर्ग कैसे रहेंगे?
पवन
कहता है, “जब
मैं यहां सुख से रहता था,
तब भी तो आप लोग दुखी थे। आपने कहा था मां की आपके बड़े बाबू के लड़के तक ने MBA
प्रवेश
परीक्षा पास कर ली। उस समय मुझे कैसा लगा था। चैन से तो मैं यहां भी रहा था पर आप
अपने सपने पूरे करना चाहते थे। आपके सपने मेरा संघर्ष में बन गए। यह मत सोचिए कि
संघर्ष अकेले आता है वह सबक भी साथ लाता है।”
घर
से वापस जाने के दिन पवन ने मां के नाम बीस हज़ार का चेक काटा। “मां हमारे आने से
आपका बहुत खर्चा हुआ है यह मैं आपको पहली किस्त दे रहा हूं वेतन मिलने पर और दूंगा।”[14]
पवन पर पैसे का नशा इस प्रकार चढ़ गया कि उसे लगता है कि जो भी उसके लिए माता-पिता
ने किया उसे वह पैसे से उतार देगा। वह माता-पिता द्वारा किए गए चीजों को कर्ज के
रूप में देखा है। ममता कालिया इस संबंध में लिखती हैं,
“जिन
युवा प्रतिभाओं ने यह कमान संभाली उन्होंने कार्य क्षेत्र में तो खूब कामयाबी पाई
पर मानवीय संबंधों के समीकरण उनसे कहीं ज्यादा खींच गए तो कहीं ज्यादा ढीले पड़ गए।”[15]
बच्चे
पढ़ लिखकर या तो अच्छे पैकेज के लिए विदेश भाग रहे हैं या फिर घर से हजारों मिल
दूर। इस विशुद्ध आजीविकावाद से पारिवारिक
और विकट सामाजिक स्थितियां पैदा हो रही है। रेखा जब छोटे बेटे सघन की भी घर से दूर
जाने की ललक देखती है तो कहती है, “इसको
भी ले जाओगे तो हम दोनों अकेले रह जाएंगे। वैसे ही यह सीनियर सिटीजन कॉलोनी बनते
जा रही है। सबके बच्चे पढ़ लिखकर बाहर चले
जा रहे हैं। हर घर में समझो एक बूढ़ा,
एक बूढ़ी,
एक कुत्ता और एक कार बस यही रह गया है।”
बच्चों
को सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार कर हर घर परिवार के मां-बाप खुद एकदम असुरक्षित
जी रहे थे। उपन्यास में जहां प्राचीनतम और नवीनतम संस्कारों के टकराहट को दिखाया
गया है उसी प्रकार वर्तमान समय में सामाजिक संकट के अभिव्यक्ति भी स्पष्ट रूप से
देखने को मिलती है जिसमें से एक है वृद्धि समस्या भी है। मिस्टर सिंह साहब,
सोनी साहब, मजीठिया
साहब यह कई उदाहरण है वृद्ध समस्या से
पीड़ित। जो एक कामयाब संतान पाने के लिए उसे बचपन से ही समझाते रहते हैं कामयाबी
का अर्थ क्या है। कामयाबी का अर्थ केवल जीविकोपार्जन
में नहीं है। “यह सब कामयाब संतानों के मां-बाप थे हर एक के चेहरे पर भय और आशंका
के साए थे। बच्चों की सफलता उनके जीवन में सन्नाटा बुन रही थी।”[16]
जब
हम देखेंगे कि कैसे आजीविका के संघर्ष में व्यक्ति इतना आधुनिक हो गया है कि उसमें
संवेदनहीनता की भावना प्रकट हो गई है। या यह कह सकते हैं कि व्यक्ति कम संवेदनशील और
अधिक तार्किक हो गया है। मिस्टर सोनी के
देहांत पर बेटा सिद्धार्थ नहीं आता है। जब उसे कॉल किया जाता है कि बेटा तेरे पिता
को हृदय का घात लगा है। तुम्हारे पिता का
देहांत हो गया है। उनकी चिता को आग देने आ जा। सिद्धार्थ न्यूयॉर्क में किसी
एमएनसी कंपनी में काम कर रहा होता है। सिद्धार्थ कहता है,
“आप
ऐसा कीजिए इस काम के लिए किसी को बेटा बनाकर दाह संस्कार करवाइए मेरे लिए तेरह दिन
रुकना मुश्किल होगा।”[17]
भारत में अभी भी संवेदना सुख नहीं गई,
फूलों में कुछ महक बांकी है। लोगों में नैतिकता और हिम्मत बची है। कॉलोनी के लोग पूरा इंतजाम कर
देते हैं क्योंकि फर्ज पहचानते हैं।
‘दौड़’
उस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें छोटे शहरों का मध्यवर्ग जीविका के
लिए महानगरों की ओर पलायन करता है और वहाँ संघर्ष करता है। दौड़ में इस समय के
नवयुवकों की दशा का चित्रांकन करती है जो घर छोड़कर नौकरी करने निकले हैं अटैची
में कपड़े,
आंखों में सपना और अंतर में आकुलता लिए। ना जाने कहां-कहां से नौजवान लड़के नौकरी
की खाते इस शहर में आ पहुंचे हैं। हर स्तर पर व्यक्ति अपना शहर,
अपना घर, अपना
गांव छोड़कर जाता है शहरों में नौकरी करने के लिए। जहां कार्यस्थल पर चुनौतियां है
तथा उसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी काफी चुनौतियां होती है। “सच्ची बात तो यह
है कि अपने घर और शहर से बाहर आदमी हर रोज एक नया सबक सीखता है।”[18]
सामाजिक
संकट केवल वृद्धि समस्या या संवेदनहीनता तक नहीं रह गयी। केवल मानवीय स्थिरता तक
मानवीय संबंधों तक नहीं रह गई। सामाजिक संकट भौगोलीय स्तर पर देखने को भी मिलती है।
जहां पर सबसे बड़ी समस्या के रूप में हम पलायन की समस्या को पाते हैं। “परदेस में
आदमी कभी नहीं जम सकता,
तंबू का कोई ना कोई खूटा उखड़ा ही रहता है।”[19]
‘दौड़’
उपन्यास में पवन,
सघन और सिद्धार्थ आदि पात्रों के माध्यम से पलायन की समस्या को भी अनावृत किया गया
है। रोजगार एवं बेहतर करियर की आशा व्यक्ति को अपने गांव अपने संस्कृति से दूर कर
देता है। देखा जाए तो पलायन और विस्थापन दोनों कहीं ना कहीं मिलते-जुलते हैं लेकिन
तीनों में कुछ सूक्ष्म अंतर भी अवश्य ही पाए जाते हैं। दोनों के लिए अंग्रेजी में
एक शब्द का प्रयोग होता है ‘माइग्रेशन’।
लेकिन हिंदी में यह दोनों अलग-अलग संदर्भ अलग-अलग अर्थ प्रकट करते हैं।
विस्थापन
का अर्थ है,
किसी व्यक्ति या समूह का अपनी मूल जगह से जबरन या अनैच्छिक रूप से हटाया जाना। यह
अक्सर बाहरी कारकों जैसे प्राकृतिक आपदा,
युद्ध,
विकास परियोजनाएं आदि के कारण होता है। यह अधिक संख्या में आदिवासी साहित्य में
देखने को मिलता है। जहां औद्योगिक खनन के कारण आदिवासी क्षेत्रों से आदिवासियों को
विस्थापित कर दिया जाता है। इससे उन आदिवासियों के आजीविका तथा संस्कृति के पहचान
पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
वही
अगर हम पलायन की बात करें तो पलायन का अर्थ है,
लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वेच्छा से या परिस्थितियों के कारण जाना। जो
अक्सर आजीविका,
बेहतर जीवन स्तर,
स्वास्थ्य या सुरक्षा की तलाश में होता है। पलायन स्थाई या अस्थाई दोनों हो सकता
है। इसमें व्यक्ति की कुछ हद तक अपनी मर्जी शामिल होती है हालांकि यह आर्थिक या
सामाजिक दबाव के प्रेरणा से हो सकता है। देश में सबसे ज्यादा पलायन रोजगार के लिए
हो रहा है। गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
इस
प्रकार अगर देखा जाए तो आजीविका या जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति पलायन काफी संख्या
में कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम दो प्रकार का पलायन देखते हैं। भौतिक पलायन और
मानसिक पलायन। शारीरिक रूप से शहर छोड़ देना यानि व्यक्ति नौकरी,
शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए गांव छोड़कर शहर चला जाये तो यह भौतिक पलायन होगा। जैसे
इस उपन्यास में पवन, सघन
और सिद्धार्थ भौतिक रूप से अपने घर से बाहर जाते हैं और आजीविका प्राप्त करते हैं।
हम भौतिक पलायन को देखें तो यहां पर एक पवन का उदाहरण है वह कहता है,
“यहां
मेरे लायक सर्विस कहां यह तो बेरोजगारों का शहर है। ज्यादा से ज्यादा नूरानी तेल
की मार्केटिंग मिल जाएगी और क्या?”[20]
जब इलाहाबाद शहर में कंपनियां है लेकिन उसे उतना अधिक वेतन नहीं मिलेगा इतनी अधिक
सुविधा नहीं मिलेगी उतना अच्छा करियर नहीं बनेगा तो करियर यानी कि भविष्य की पहचान
को लेकर के व्यक्ति अपने शहर छोड़ कर दूसरे शहर जा रहा है।
दौड़’
उपन्यास में सघन ताइवान में नौकरी मिलने विदेश चला जाता है। और पीछे घर में केवल
बूढ़े माता-पिता रह जाते हैं। ममता कालिया लिखती है,
“निवासी और प्रवासी केवल पर्यटक और पंछी नहीं होते,
बच्चे भी होते हैं। वह दौड़-दौड़ कर दर्जी के यहां से अपने लिए नए सिले कपड़े लाते
हैं, सूटकेस में अपना
सामान और कार्य जमाते हैं। मनी बेल्ट में अपना पासपोर्ट,
वीजा और चंद डॉलर लेकर रवाना हो जाते हैं अनजान देश प्रदेश के सफर पर माता-पिता को
सिर्फ स्टेशन पर हाथ हिलाते छोड़कर।”[21]
मानसिक
पलायन में मानसिक रूप से व्यक्ति गांव परिवेश,
संस्कृति से अलग हो जाता हैं भले ही भौतिक रूप से वह शहर में हो अथवा गाँव में हो। इसका
कारण आधुनिकता,
असंतोष की भावना,
पहचान का संकट,
मानसिक परिवर्तन आदि हो सकता है। जैसे कई लोग शहर में नौकरी करने जाते हैं और वापस
अपने गांव आने पर गांव और शहर की तुलना करते हैं। शहर में यह सुविधा है गाँव में
नहीं है। धीरे-धीरे मानसिक पलायन के कारण शहर व्यक्ति का अपना हो जाता है और गांव
पराया। मानसिक पलायन के संदर्भ में ममता कालिया लिखती हैं,
“जहां
शहरी चकाचौंध में युवा गांव की मिट्टी में कमियां निकालने लग जाता है और वह शहर वह
सहयोगी कर्मचारी अपना हो जाता है।”[22]
निष्कर्ष
आज
मनुष्य सभ्यता के उसे मोड़ पर खड़ा है जहां चाहूं ओर बाजार ही बाजार है। समकालीन
दौर में वस्तुएं बोलती है और इंसान चुप्पी साधे हुए है। मानवीय संवेदनाएं आहिस्ता-आहिस्ता
बाजार की संवेदनाओं में तब्दील होने लगी है। संबंध की स्थापना भी करियर की दृष्टि,
लाभ की दृष्टि से की जा रही है। यह सत्य है कि इस तेज दौड़ते जिंदगी में किसी एक
जगह ठहर कर अपना कैरियर बनाना संभव नहीं है फिर भी इन चीजों के कारण मानवीय
संबंधों में जिस तेजी से बदलाव आया है वह एक चिंतन यह विषय अवश्य है। इस उपन्यास में आजीविका जीवन का, संबंधों
का और मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्र बन जाती है, जिससे
उसके सामाजिक और पारिवारिक धरातल पर गहरे प्रभाव पड़ते हैं। ममता
कालिया ने इस उपन्यास में दिखाया है कि नौकरी केवल आर्थिक साधन नहीं है,
बल्कि
व्यक्ति की सामाजिक पहचान और अस्तित्व का आधार भी है। नौकरी की असुरक्षा व्यक्ति
को मानसिक, सामाजिक
और भावनात्मक स्तर पर अस्थिर बना देती है। इस प्रकार,
‘दौड़’ केवल व्यक्तिगत कथा नहीं रह जाती,
बल्कि
यह पूरे भारतीय मध्यवर्ग की कथा बन जाती है।
संदर्भ
ग्रंथ सूची
1.
मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, अध्याय-1, भाग-1, कक्षा-12, NCERT, प्रथम संस्करण, 2017, पृष्ठ. 5
2.
खान सर, खान सर ने बताया जीविका और
बेरोजगारी में अंतर, https://youtu.be/v2lqdtn1FRg?si=xw-rYINBX3gsnaKs , 22 सितंबर 2025
13.
अनीता राजपुरिया, मध्यमवर्गीय परिवार: समस्याएँ एवं समाधान, शताक्षी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2010, पृष्ठ 161
सारणी
सूची
सारणी 1 में प्रयोग किए गए महत्वपूर्ण वैबसाइट,
1.
"Economic Survey
2023-24." Ministry of Finance, Government of India, 22 July 2024,
egazette.gov.in. Accessed 9 Oct. 2025.
2.
"Periodic Labour Force
Survey (PLFS) Annual Report 2023-24." National Statistical Office,
Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, 2024,
mospi.gov.in. Accessed 9 Oct. 2025.
3.
"India Employment Report
2024: Youth Employment, Education and Skills." International Labour
Organization (ILO), 2024,
www.ilo.org/sites/default/files/2024-08/India%20Employment%20-%20web_8%20April.pdf.
Accessed 9 Oct. 2025.
4.
"India: Distribution of
the Workforce across Economic Sectors from 2012 to 2022." Statista, 30 May
2024,
www.statista.com/statistics/271320/distribution-of-the-workforce-across-economic-sectors-in-india/.
Accessed 9 Oct. 2025.
.png)