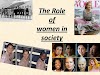डॉ. नेहा कल्याणी
सहायक व्याख्याता
गो. से.
अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर
सारांश :- भाषा विज्ञान भाषा के
अंगों सहित उसके उपांगो , विकास, विश्लेषण आदि का क्रमिक अध्ययन
करता है , इसलिए उसे भाषा विज्ञान कहते हैं । भाषा विज्ञान भाषा का
वैज्ञानिक अध्ययन करता है और भाषा शिक्षण का संबंध भाषा के शिक्षण से हैं । इस
प्रकार दोनों प्रत्यक्षत : भाषा के अध्ययन और अध्यापन से सम्बद्ध होने के कारण आपस
में भी सम्बद्ध है।
भाषा शिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology - IT) का संयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी
परिवर्तन ला रहा है। आधुनिक डिजिटल युग में भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रियाएँ
पारंपरिक पद्धतियों से आगे बढ़कर डिजिटल संसाधनों, मल्टीमीडिया टूल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अधिक प्रभावी और सुलभ
हो गई हैं। कंप्यूटर अनुवाद और भारतीय भाषाओं के संबंध में
सर्वाधिक प्रमाणिक कार्य करने वाली
सी
डेक (CDAC) पुणे ने भारत सरकार के सहयोग से भारतीय भाषाओं में अनेक
अनुसंधानों को किया है। हिंदी में अनुवाद करने के लिए मंत्र नमक पैकेज का विकास
किया है ।यह पैकेज अनुवाद के भाषा वैज्ञानिक पहलू और अनुप्रयुक्त भाषा तथा व्याकरण
के समुचित मिश्रण से तैयार किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी ने भाषा शिक्षण को नए आयाम दिए हैं। डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और AI आधारित तकनीकों के माध्यम से भाषा सीखने की प्रक्रिया
अधिक सहज, सुलभ और प्रभावी बन रही है।
बीज शब्द :- भाषा शिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, डाटा
प्रोसेसिंग।
प्रस्तावना :- भाषा विज्ञान भाषा के अंगों सहित उसके उपांगो , विकास, विश्लेषण आदि का क्रमिक अध्ययन करता है , इसलिए उसे भाषा
विज्ञान कहते हैं । भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और भाषा शिक्षण का संबंध भाषा
के शिक्षण से हैं । इस प्रकार दोनों प्रत्यक्षत : भाषा के अध्ययन और अध्यापन से
सम्बद्ध होने के कारण आपस में भी सम्बद्ध
है। भाषा की शिक्षा देने का
उद्देश्य यह है कि मनुष्य उचित रूप से बोल समझ सके एवं शुद्ध प्रभावोत्पादक , मधुर
, रमणीय शैली में अपने विचारों का सम्प्रेषण कर सके । शुद्ध भाषा का अर्थ यह है कि वक्ता ,लेखक को
अपनी भाषा के व्याकरण लेखन पर आश्रित शिष्टजन के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा
शैली का ही प्रयोग होना चाहिये ।
किंतु वर्तमान समय में भाषा शिक्षण भाषा अध्ययन एवं विश्लेषण, अनुवाद, भाषा संबंधी
नवीनतम अवधारणाओं को कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोग किया जा रहा है । वर्तमान कंप्यूटर
युग ने भाषा के क्षेत्र में भी क्रांति लाई है । कंप्यूटर की भाषा
को संक्षेप में मशीनी भाषा भी कह सकते हैं । कंप्यूटर विश्व की समस्त भाषाओं को
बोल सकता है ,लिख सकता है, पढ़ सकता है, स्कैन कर सकता है; परंतु आश्चर्य है ये कार्य वह केवल 0 और 1 के माध्यम से
करता है अर्थात विश्व की समस्त भाषाये इन दो अंकों के माध्यम से पढी, लिखी और सुनी जा सकते हैं । इसी भाषा को कंप्यूटर के क्षेत्र में द्विचर अर्थात बाइनरी(binary) नाम दिया गया है । संसार की किसी भी भाषा को इन दो अंको से
कुटांकित किया जाता है । उदाहरण के लिए हमें अ कहना है तो 01 कुट बना सकते हैं या a कहना है तो 001 । इस प्रकार हर अक्षर के लिए आगे पीछे जीरो या वन लगाकर कुट बनाए जा सकते हैं ।
एक बार ऐसा कुटांकन होने के बाद कंप्यूटर इस भाषा को समझ लेता है । वर्तमान समय में घरों के
इलेक्ट्रॉनिक तालों में भी आपकी आवाज भर दी जाती है इसका सिद्धांत यह है कि
प्रत्येक व्यक्ति की स्वरतंत्री में अंतर होता है आवाज में भिन्नता होती है । परिणामत: कंप्यूटर आसानी
से आपकी आवाज पहचानता है । जब कभी कंप्यूटर पर चर्चा होती है तो समझा जाता है कि
यह उपकरण केवल अंग्रेजी में ही कार्य करते हैं , किंतु ऐसा नहीं
आज इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि विश्व की किसी भी भाषा
में परिचालित किया जा सकता है। अंकगणितीय तर्क व प्रोग्रामिंग तथा परिचालन का सामान्य ज्ञान होने
पर कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य किया जा सकता है। 80 के दशक में रेलवे विभाग में हिंदी माध्यम से कंप्यूटर पर
थोड़ा-थोड़ा कार्य होने लगा था तथा 90 के दशक में बैंकों में कंप्यूटरों के द्विभाषीकरण की प्रक्रिया शुरू तो हो गई
किंतु वह नगण्य ही थी।
मौजूदा तकनीकी उपकरणों को प्रक्रिया द्वारा द्विभाषिक बनाया जा सकता है । आज
अनेक कंपनियां द्विभाषिक सॉफ्टवेयर पैकेज भी तैयार करते हैं।1987 मैं राजभाषा विभाग द्वारा सभी सरकारी विभागों को निर्देश
जारी किए गए थे कि द्विभाषिक उपकरण ही खरीदे जाएं जिससे उनमें हिंदी के साथ
अंग्रेजी में भी डाटा एंट्री की व्यवस्था हो।
सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी:- भाषा शिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology - IT) का
संयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। आधुनिक डिजिटल
युग में भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रियाएँ पारंपरिक पद्धतियों से आगे बढ़कर
डिजिटल संसाधनों, मल्टीमीडिया टूल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अधिक प्रभावी और सुलभ
हो गई हैं।
संचार क्षेत्र
में हुई तीव्रगामी क्रांति ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक नई विधा को जन्म दिया
जिसे सूचना प्रौद्योगिकी कहा गया है । वस्तुत सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर और
संचार विज्ञान का ही समेकित रूप है । संचार के क्षेत्र में हुए विकास, अनुसंधान तथा
भूमंडलीकरण की आंधी ने कुछ समय के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि प्रतीत होने लगा
कि अब सारे संसार में अंग्रेजी का ही वर्चस्व होगा किंतु भारत , चीन और जापान जैसे स्वाभिमानी राष्ट्रों ने कंप्यूटर में अपनी भाषा की व्यवस्था की। अब
कंप्यूटर द्वारा हिंदी में शब्द संसाधन और इसी प्रकृति के कार्य भी होने लगे
यद्यपि इस क्षेत्र में कंप्यूटर्स पर हिंदी के उपयोग की गति कुछ धीमी रही किंतु
समय के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहें।
यद्यपि प्रारंभ में कंप्यूटर पर हिंदी में या भारतीय भाषाओं में काम करने में
अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा परंतु देखते ही देखते हैं कंप्यूटरों पर
हिंदी भाषा का वर्चस्व कायम हो गया । वर्ड
प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर पूरी दक्षता से काम करने लगे, परंतु कंप्यूटर
द्वारा पूर्ण सक्षमता से कार्य करने पर भी जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हिंदी में प्रिंट
लेने की गति धीमी होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी की उपयोगिता पर प्रश्न
चिन्ह लगना शुरू हो गया ; परंतु यह स्थिति भी ज्यादा दिन नहीं रही प्रिंटर पर ‘ई-प्राम्प’ को लगा देने से हिंदी में भी कंप्यूटर बड़ी तेजी से प्रिंट आउट देने लगे । बाद में इंकजेट
प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के आने से भाषाई मुद्रण की गति और गुणवत्ता दोनों ही
अंग्रेजी की ही भांति सुंदर और त्वरित होने लगी ।
हिंदी में डाटा प्रोसेसिंग :- पत्राचार व
रिपोर्ट आदि को तैयार करने का
विवरण या तालिकाएं बनाने में अन्य वर्ड प्रोसेसिंग से जुड़े कार्य हिंदी में आसानी
से होने लगे । बैंकों में सरकारी विभागों में तथा व्यापार में स्वीकार्यता मिली , लेकिन बैंकों में
संपूर्ण शाखा स्वचालन (Total Branch Automation) जैसी संकल्पना के
जन्म के कारण बैंकों को हिंदी द्वारा डाटा प्रोसेसिंग की समस्या से जूझना पड़ा । वित्त मंत्रालय
द्वारा बैंकों के व्यापार में कंप्यूटरों की अनिवार्यता के साथ-साथ बैंकों का
व्यापार कोर द्वारा किया जाने का भी निर्देश दिया गया।
पुन: यहां आकर हिंदी की गति धीमी हो गई क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग
का यह कार्य अलग-अलग बैंकों से होने के कारण अंग्रेजी में ही पूर्ण रूप से स्थापित
नहीं हो पाया था। इस दिशा में जयपुर
की कंपनी नेचुरल टेक्नोलॉजी में बैंक में नाम से एक द्विभाषिक पैकेज बनाया जो काफी
हद तक बैंकिंग कारोबार को द्विभाषी करने में समर्थ परंतु इस पैकेज की समस्या या थी
कि यह सिर्फ विंडोस वातावरण में ही चलता था जबकि लगभग 25 वर्ष पूर्व बैंकों में शाखा स्वचालन का यह कार्य डॉस
आधारित वातावरण में ही होता था अत: यह अधिक लोकप्रिय
ना हो सका।
डॉस आधारित पैकेजों के लिए इंटरफेस नामक विकल्प बड़ा सुगम और सरल था। इस विकल्प में अंग्रेजी में काम
करने के बावजूद डाटा स्वत: हिंदी में अनुवादित हो जाता था। यह मूल अंग्रेजी पैकेज के
साथ कोई बदलाव नही करता था जिससे आंकड़ों के खराब होने की कोई संभावना नहीं रहती थी । साथ ही ग्राहक को
हिंदी में भाषिक प्रिंट आउट देने का विकल्प भी रहता था। किंतु आरंभिक दौर में
इंटरफेस के अनुवाद में त्रुटियां होती थी तथा यह
भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप नहीं था । इन दोनों समस्याओं के कारण यह
अधिक लोकप्रिय ना हो सका।
द्विभाषी कंप्यूटर और विभिन्न समितियो की भूमिका :- बैंकों में द्विभाषी कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा
देने हेतु श्री के. एल . मगन की अध्यक्षता
में एक समिति बनाई गई और उन्होंने यह निर्णय दिया कि द्विभाषीकरण का यह कार्य
बैंकों को अपने-अपने स्तर पर करना चाहिए तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस
क्षेत्र के लिए दो समितियो का गठन किया गया । पहली समिति का कार्य
था कंप्यूटर हेतु हिंदी में द्विभाषी शब्दकोश तैयार करना जो शीघ्र ही पूर्ण हुआ
तथा दूसरी समिति का कार्य था कंप्यूटरों के प्रयोग में एकरूपता लाने की दृष्टि से
कार्य करना इस हेतु यूनिकोड को अविष्कृत किया गया जो पूर्णतया सफल भी रहा है।
कुछ उत्साही कंप्यूटर अधिकारियों ने हिंदी फॉन्ट को इंटरफ़ेस का सहारा लेकर और
बैंकिंग को द्विभाषी करने का प्रयास किया; लेकिन हिंदी फॉन्ट तथा इसमें प्रयुक्त होने
वाली इंटरफेस प्रक्रिया का समुचित
इंटीग्रेशन ना हो पाने के कारण यह प्रयास भी सफल न हो पाए। इसलिए इंटरफ़ेस का
विकल्प चुनने वाले संगठनों को चाहिए कि वह निरंतर शब्दकोश परिष्कृत करते रहें और
कोर से तैयार होने वाले सभी रिपोर्ट और फोर्मेटो को मानकीकृत कर लें ; क्योंकि किसी भी
फॉर्मेट में थोड़ा सा भी भाषागत अंतर होने पर यहां तक कि शब्दों के बीच
में यदि एक अतिरिक्त स्पेस भी आ जाए तो इंटरफेस उसका भी अपने ढंग से अनुवाद कर
देता है या उसे शब्द का अर्थ कंप्यूटर के शब्दकोश में मौजूद न हो तो वह उसका
ध्वन्यात्मक अनुवाद कर देता है; जिसके परिणामस्वरुप गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है ।
अनुवाद क्षेत्र :- आज हम उसे मुकाम पर खड़े हैं जहां पर कंप्यूटर और भारतीय
भाषाओं का फासला खत्म हो चुका है ।आज कंप्यूटर
भारतीय भाषाओं में वे सभी कार्य कर रहे हैं जो अंग्रेजी में भी संभव है, किंतु आज
भी अनुवाद के क्षेत्र में कंप्यूटर पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता क्योंकि अनुवाद संकल्पना अत्यधिक
अमूर्त व जटिल होने के कारण इसकी कृत्रिम
बुद्धिमत्ता अर्थात कंप्यूटर से अनुवाद एक
दुष्कर कार्य है। अनुवाद के क्षेत्र में तो प्रत्येक शब्द, वाक्य ,अभिव्यक्ति
में उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता और अनुवाद
कौशल की अपेक्षा की जाती है ।एक ही पंक्ति का अनुवाद यदि भिन्न-भिन्न ज्ञान
और क्षमता वाले व्यक्तियों से कराया जाए तो उसका रूप भिन्न-भिन्न होता है तो उस
अनुवाद के हर रूप में एक
नयापन होगा, नई अनुभूति होगी, नए भाव होंगे, नई सांस्कृतिक विरासत होगी और अलग-अलग
बौद्धिक क्षमता और अनुवादक की रुचि की झलक भी इन रूपों में मिलेगी । अर्थात कंप्यूटर द्वारा किया गया अनुवाद प्रयोगकर्ता
द्वारा परिष्कृत और परिमार्जित किए जाने की आवश्यकता आज भी प्रतीत होती है । मौलिक चिंतन के
लिए तो मनुष्य की सृजनशील मस्तिष्क की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। कंप्यूटर अनुवाद
और भारतीय भाषाओं के संबंध में सर्वाधिक प्रमाणिक कार्य करने वाली सी डेक (CDAC) पुणे ने भारत
सरकार के सहयोग से भारतीय भाषाओं में अनेक अनुसंधानों को किया है। हिंदी में
अनुवाद करने के लिए मंत्र नमक पैकेज का विकास किया है ।यह पैकेज अनुवाद के भाषा
वैज्ञानिक पहलू और अनुप्रयुक्त भाषा तथा व्याकरण के समुचित मिश्रण से तैयार किया
गया है
भाषा शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका
सूचना
प्रौद्योगिकी के उपयोग से भाषा शिक्षण अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण (interactive) और
व्यक्तिगत (personalized) बनाया जा सकता है।
1. ई-लर्निंग
प्लेटफॉर्म्स
ऑनलाइन
भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Duolingo, Coursera, Udemy, Rosetta Stone और EdX महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ऑडियो, वीडियो, और
इंटरैक्टिव क्विज़ के माध्यम से भाषा सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं।
2. मल्टीमीडिया
साधन
भाषा
शिक्षण में वीडियो, पॉडकास्ट, एनिमेशन, इन्फोग्राफिक्स और डिजिटल पुस्तकें (E-books) शिक्षार्थियों की समझ और रुचि बढ़ाने में मदद करती हैं।
3. आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग
AI आधारित टूल्स जैसे कि Google Translate, ChatGPT, Grammarly भाषा सीखने वालों के लिए
भाषा सुधार, अनुवाद और अभ्यास करने में सहायक हैं।
4. मोबाइल
एप्लिकेशन और गेमिफिकेशन
Memrise, Babbel जैसे ऐप्स भाषा सीखने और
शब्दों की उच्चारण प्रक्रिया
को गेमिंग तत्वों से जोड़कर अधिक मज़ेदार और प्रभावी बनाते हैं।
5. वर्चुअल
और ऑगमेंटेड रियलिटी (VR/AR)
VR और AR तकनीकों
के माध्यम से भाषा शिक्षण को अधिक व्यावहारिक और अनुभवात्मक (experiential) बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, Mondly VR जैसे प्लेटफॉर्म भाषा
अभ्यास के लिए वर्चुअल वातावरण उपलब्ध कराते हैं।
भविष्य
की संभावनाएँ
- व्यक्तिगत शिक्षण (Personalized Learning): AI और बिग डेटा के माध्यम से भाषा शिक्षण को व्यक्ति की
आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
- चैटबॉट और वॉयस
असिस्टेंट्स: AI आधारित बॉट्स और डिजिटल असिस्टेंट्स, जैसे
कि Siri, Alexa और Google Assistant, भाषा
शिक्षण को और अधिक सहज और संवादात्मक बना सकते हैं।
- ऑनलाइन शिक्षण समुदाय: डिजिटल
प्लेटफॉर्म्स पर वैश्विक भाषा शिक्षण समुदाय बनाकर छात्रों को एक-दूसरे से
सीखने का अवसर मिलेगा।
निष्कर्ष
सूचना प्रौद्योगिकी ने भाषा शिक्षण को नए आयाम दिए हैं। डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और AI आधारित तकनीकों के माध्यम से भाषा सीखने की प्रक्रिया
अधिक सहज, सुलभ और प्रभावी बन रही है। भविष्य में इन तकनीकों के
और अधिक विकसित होने से भाषा शिक्षण की गुणवत्ता में और सुधार होगा। यह तकनीकी शिक्षण
भाषा के व्याकरण, शब्दावली, और साहित्य
के साथ-साथ अभिव्यक्ति, समझ, और संवाद
कौशल को विकसित करने पर केंद्रित होता है।
संदर्भ ग्रंथ :-
1.
भाषाविज्ञान – भोलानाथ
तिवारी , वाणी प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन 1951
2.
भाषाविज्ञान का परिचय, लेखक: डॉ. हरदेव बाहरी, लोकभारती प्रकाशन, 1973
3.
हिन्दी भाषाविज्ञान, डॉ.
रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन, 1954
4. भाषा विज्ञान: सिद्धांत और प्रयोग, डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, विश्व
पुस्तक प्रकाशन, 1990
5.
हिन्दी
भाषा -स्वरूप और विकास , कैलाशचंद्र भाटिया ,मोतीलाल चतुर्वेदी , प्रभात प्रकाशन
१९८९
.png)