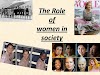शिक्षा के बदलते स्वरूप में डिजिटल शिक्षण पद्धति की प्रासंगिकता
सिंधु कुमारी
डॉ० भवप्रीता कुमारी
प्रस्तावना
मानव सभ्यता का
इतिहास गवाह है कि शिक्षा ही समाज की आत्मा होती है। शिक्षा मनुष्य को केवल ज्ञान
ही नहीं देती बल्कि जीवन मूल्यों, संस्कृति और
सामाजिक चेतना का निर्माण करती है। समय और परिस्थितियों के साथ शिक्षा की प्रकृति
बदलती रही है। यदि हम अतीत में देखें तो कभी शिक्षा मौखिक परंपरा पर आधारित थी, कभी हस्तलिखित ग्रंथों पर, और कभी छपी हुई
पुस्तकों पर। 20वीं सदी तक शिक्षा का मूल स्वरूप भौतिक कक्षा और
आमने–सामने संवाद तक ही सीमित था। किन्तु 21वीं सदी, जिसे तकनीकी
युग कहा जाता है, ने शिक्षा को डिजिटल दिशा में मोड़ दिया। आज
शिक्षा केवल पुस्तकों, ब्लैकबोर्ड और
कक्षाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंटरनेट, स्मार्टफोन, वर्चुअल
क्लासरूम, ई-पुस्तकालय, और
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे साधनों पर आधारित नई पद्धति का रूप ले चुकी है। यही
है डिजिटल शिक्षण पद्धति, जिसकी
प्रासंगिकता वर्तमान समय में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई है।
शिक्षा का
बदलता स्वरूप
1. पारंपरिक
शिक्षा
भारत में
प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी जहाँ छात्र गुरु के आश्रम में रहकर
शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती
थी। मध्यकाल में मठ, मकदम, मदरसे और
पाठशालाएँ बनीं। औपनिवेशिक काल में आधुनिक विद्यालय और विश्वविद्यालय अस्तित्व में
आए। इन सबमें मुख्य साधन मौखिक शिक्षा, पुस्तकों और
प्रत्यक्ष कक्षा का वातावरण रहा।
2. औद्योगिक और
आधुनिक शिक्षा
औद्योगिक
क्रांति के बाद शिक्षा में विज्ञान और तकनीक का समावेश हुआ। प्रयोगशालाएँ, चार्ट, प्रोजेक्टर और
स्लाइड्स जैसी तकनीकें आईं। अब शिक्षा केवल रटने की प्रक्रिया न होकर अनुभव और
प्रयोग पर आधारित होने लगी।
3. डिजिटल युग की
शिक्षा
21वीं सदी में इंटरनेट ने शिक्षा का चेहरा बदल दिया। शिक्षा अब ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल
लाइब्रेरी और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध है। कोविड-19 महामारी ने इसे और तेज़ गति से आगे बढ़ाया।
डिजिटल शिक्षण
पद्धति की परिभाषा
डिजिटल शिक्षण
पद्धति (Digital Learning Methodology) वह प्रणाली है
जिसमें शिक्षण और अधिगम की पूरी प्रक्रिया डिजिटल उपकरणों—कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर—और
ऑनलाइन संसाधनों जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई-बुक, वीडियो लेक्चर, वर्चुअल लैब
आदि के माध्यम से संपन्न होती है।
डिजिटल शिक्षण
की प्रासंगिकता
1. शिक्षा की
सार्वभौमिक पहुँच
ग्रामीण
क्षेत्रों के छात्र, जो कभी
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहते थे, अब इंटरनेट के
माध्यम से विश्व-स्तरीय शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं।
2. समय और स्थान
की लचीलापन
पारंपरिक कक्षा
समयबद्ध होती है, जबकि डिजिटल शिक्षा कहीं भी और कभी भी संभव है।
छात्र रात में, यात्रा के दौरान या घर पर बैठकर भी पढ़ सकते
हैं।
3. बहुआयामी
शिक्षण
वीडियो, ग्राफिक्स, एनीमेशन और 3D मॉडल से सीखना और भी आसान हो गया है। उदाहरण के लिए, जीवविज्ञान का कोई जटिल अध्याय 3D एनिमेशन में
दिखाया जाए तो छात्र उसे अधिक आसानी से समझ लेता है।
4. वैश्विक अवसर
डिजिटल पद्धति
से कोई भी छात्र दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों—हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी—के
ऑनलाइन पाठ्यक्रम घर बैठे कर सकता है।
5. आत्मनिर्भरता
और कौशल विकास
ऑनलाइन शिक्षा
छात्रों को केवल शिक्षक पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं खोज करने और समस्या हल करने
की आदत डालती है।
डिजिटल शिक्षा
के विभिन्न रूप
1. ई-लर्निंग
प्लेटफॉर्म – जैसे BYJU’s, Unacademy, Vedantu, Khan
Academy, Coursera।
2. वर्चुअल
क्लासरूम – Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ने शिक्षा को
इंटरैक्टिव बनाया।
3. MOOCs (Massive Open Online Courses) – जिनमें लाखों
छात्र एक साथ जुड़ सकते हैं।
4. डिजिटल
लाइब्रेरी और ई-बुक्स – राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (NDLI) और गूगल बुक्स।
5. एआई आधारित
लर्निंग – छात्र की क्षमता के अनुसार अलग-अलग स्तर की सामग्री उपलब्ध कराना।
6. वर्चुअल लैब्स
– जहाँ छात्र प्रयोग घर बैठे कर सकते हैं।
डिजिटल शिक्षा
के लाभ
डिजिटल शिक्षण
पद्धति ने शिक्षा को केवल आधुनिक ही नहीं बनाया है, बल्कि इसे सुगम, समावेशी और परिणामोन्मुख भी बनाया है। इसके लाभ अनेक स्तरों पर दिखाई
देते हैं—छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समाज और यहाँ तक कि राष्ट्र तक। आइए विस्तार से देखे
1. शिक्षा की
सार्वभौमिक पहुँच
·
डिजिटल साधनों ने शिक्षा को भौगोलिक सीमाओं से मुक्त कर दिया है।
·
अब गाँव–कस्बों का छात्र भी वही सामग्री देख सकता है जो महानगरों का
छात्र देखता है।
·
दिव्यांग छात्र जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते थे, वे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा से जुड़ सकते हैं।
·
विदेश में रह रहे भारतीय छात्र भी भारतीय शिक्षा प्लेटफॉर्म से आसानी
से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं
2. समय और स्थान
की स्वतंत्रता
·
पारंपरिक शिक्षा निश्चित समय और स्थान तक सीमित थी।
·
अब छात्र अपनी सुविधा के अनुसार सुबह, शाम या रात कभी
भी पढ़ाई कर सकता है।
·
नौकरीपेशा वाले लोग भी ऑनलाइन कोर्स करके अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं।
·
यात्रा के दौरान मोबाइल पर पढ़ाई संभव हो गई|
3. बहुआयामी और
रोचक शिक्षण
·
डिजिटल शिक्षा ने “केवल पढ़ना–लिखना” वाली शैली को खत्म कर दिया है।
·
वीडियो, एनीमेशन, 3D मॉडल और इन्फ़ोग्राफ़िक्स से जटिल विषय भी आसानी से समझ आते हैं।
·
गेमिफिकेशन (खेल की तरह सीखना) से शिक्षा मनोरंजक बनती है।
·
आभासी प्रयोगशालाएँ (Virtual Labs) विज्ञान जैसे
विषयों को और अधिक अनुभवात्मक बना देती हैं|
4. किफ़ायती
शिक्षा
·
डिजिटल शिक्षा पारंपरिक स्कूल, कोचिंग और
कॉलेजों की तुलना में काफी सस्ती होती है।
·
एक बार इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट डिवाइस होने पर असीमित सामग्री
उपलब्ध हो जाती है।
·
पुस्तकें खरीदने की जगह ई-बुक्स और ऑनलाइन नोट्स किफ़ायती विकल्प बनते
हैं|
5. त्वरित और
नवीनतम जानकारी
·
प्रिंटेड किताबों में जानकारी बदलने में सालों लग जाते हैं, परंतु डिजिटल सामग्री मिनटों में अपडेट हो सकती है।
·
किसी भी विषय पर नवीनतम शोध या खोज तुरंत छात्र तक पहुँच सकती है।
·
इससे शिक्षा “समसामयिक” और प्रासंगिक बनी रहती है
6. आत्मनिर्भरता
और शोध क्षमता
·
छात्र केवल शिक्षक पर निर्भर नहीं रहते बल्कि स्वयं खोज और रिसर्च
करना सीखते हैं।
·
इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से वे अपनी आलोचनात्मक सोच विकसित करते
हैं।
·
इससे छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आती है
7. वैश्विक अवसर
और सहयोग
·
डिजिटल शिक्षा ने दुनिया को “वैश्विक कक्षा” बना दिया है।
·
भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों के कोर्स कर सकते हैं और वहीं के
छात्रों से संवाद कर सकते हैं।
·
सांस्कृतिक आदान–प्रदान और वैश्विक दृष्टिकोण का विकास होता है।
8. शिक्षक और
छात्र के बीच बेहतर संवाद
·
वर्चुअल क्लासरूम में चैट, पोल, क्विज़ और ब्रेकआउट रूम जैसी सुविधाएँ संवाद को और सक्रिय बनाती हैं।
·
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षक छात्रों की प्रगति को तुरंत ट्रैक कर
सकते हैं।
·
इससे व्यक्तिगत शिक्षण संभव हो जाता है।
9. पर्यावरणीय लाभ
·
डिजिटल शिक्षा में पुस्तकों और कागज़ की कम खपत होती है।
·
इससे पेड़ों की कटाई और संसाधनों का अपव्यय कम होता है।
·
यात्रा की आवश्यकता कम होने से प्रदूषण भी घटता है।
10. जीवन कौशल और
रोजगारोन्मुखी शिक्षा
·
डिजिटल शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं है।
·
यह छात्रों को नई तकनीक, कंप्यूटर
साक्षरता, प्रस्तुतीकरण कौशल, टीमवर्क और समय प्रबंधन जैसे जीवन कौशल भी सिखाती है।
·
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले व्यावसायिक और तकनीकी कोर्स छात्रों
को रोजगारोन्मुख बनाते हैं
11. विशेष
आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सहायक
·
दृष्टिबाधित छात्र टेक्स्ट-टू-स्पीच सॉफ्टवेयर से पढ़ाई कर सकते हैं।
·
श्रवण बाधित छात्रों के लिए वीडियो में सबटाइटल्स उपलब्ध रहते हैं।
·
इस प्रकार डिजिटल शिक्षा समावेशी और संवेदनशील बन जाती है।
12. आकस्मिक
परिस्थितियों में शिक्षा की निरंतरता
कोविड-19 महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब केवल डिजिटल
माध्यमों ने शिक्षा की निरंतरता बनाए रखी। आपदा, प्राकृतिक संकट या आपात स्थिति में भी शिक्षा बाधित नहीं होती।
डिजिटल शिक्षा
की चुनौतियाँ :
डिजिटल शिक्षा
जितनी संभावनाएँ लेकर आई है, उतनी ही
चुनौतियाँ भी सामने हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो यह पद्धति
समाज के एक बड़े वर्ग को पीछे भी छोड़ सकती है। आइए इन चुनौतियों को विस्तार से
समझें:
1. डिजिटल विभाजन
(Digital Divide)
·
भारत जैसे देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्थायी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।
·
ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गियों में रहने वाले छात्रों के लिए
ऑनलाइन कक्षा में भाग लेना कठिन हो जाता है।
·
इससे शिक्षा में असमानता और बढ़ सकती है।
2. तकनीकी
अवसंरचना की कमी
·
भारत के कई विद्यालयों और कॉलेजों में अभी भी पर्याप्त कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और वाई-फ़ाई की सुविधा नहीं है।
·
बिजली की कमी और नेटवर्क की समस्या पढ़ाई को बाधित करती है।
·
छोटे शहरों के शिक्षक और छात्र तकनीक का उपयोग करने में सहज नहीं
होते।
3. मानवीय संवाद
का अभाव
·
पारंपरिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का आमने–सामने संवाद होता है, जिससे न केवल शिक्षा बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी होता है।
·
डिजिटल कक्षाओं में यह संबंध कमजोर हो जाता है।
·
छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक कौशल के विकास में बाधा आ
सकती है।
4. अत्यधिक
स्क्रीन टाइम और स्वास्थ्य समस्याएँ
लंबे समय तक
मोबाइल और कंप्यूटर पर पढ़ाई करने से आँखों की रोशनी पर असर पड़ता है। पीठ और गर्दन की समस्याएँ, नींद की
गड़बड़ी और मानसिक तनाव भी बढ़ सकते हैं| छोटे बच्चों
में यह समस्या और गंभीर हो सकती हैl
5. साइबर सुरक्षा
और गोपनीयता (Privacy Issues)
·
डिजिटल शिक्षा में छात्रों का डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है।
·
हैकिंग, डेटा चोरी और
साइबर अपराध का खतरा बना रहता है।
·
कई बार बच्चे असुरक्षित वेबसाइटों या अनुचित सामग्री तक भी पहुँच जाते
हैं।
6. गुणवत्तापूर्ण
सामग्री का अभाव
·
इंटरनेट पर शिक्षा से जुड़ी लाखों सामग्री उपलब्ध है, लेकिन सभी सही और उपयोगी नहीं होती।
·
कई बार छात्र भ्रामक या अप्रमाणिक जानकारी से भ्रमित हो जाते हैं।
·
शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए सामग्री का मूल्यांकन और नियंत्रण
आवश्यक है।
7. शिक्षकों का
प्रशिक्षण और मानसिकता
·
कई शिक्षक डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करने में सहज नहीं हैं।
·
पारंपरिक शैली के आदी शिक्षक जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उनका प्रभाव
वैसा नहीं रहता।
·
शिक्षकों को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना बड़ी चुनौती है।
8. ध्यान भटकने की
समस्या
ऑनलाइन पढ़ाई
करते समय छात्र आसानी से सोशल मीडिया, गेम या अन्य
वेबसाइटों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इससे उनकी
एकाग्रता कम हो जाती है और अध्ययन प्रभावित होता है।
9. भाषा और
क्षेत्रीय असमानताएँ
भारत में
शिक्षा केवल अंग्रेज़ी या हिंदी तक सीमित नहीं है, यहाँ सैकड़ों
भाषाएँ बोली जाती हैं।
डिजिटल सामग्री अधिकतर अंग्रेज़ी या प्रमुख
भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे
क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों को कठिनाई होती है।
10. सामाजिक और
आर्थिक असमानता
अमीर परिवार
अपने बच्चों के लिए बेहतर डिवाइस, इंटरनेट और
कोचिंग खरीद सकते हैं। गरीब परिवारों
के पास यह सुविधा नहीं होती, जिससे शिक्षा
में असमानता और गहरी हो जाती हैl
11. तकनीक पर
अत्यधिक निर्भरता
यदि बिजली चली
जाए या इंटरनेट बंद हो जाए तो शिक्षा बाधित हो जाती है। तकनीक पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता छात्रों की रचनात्मकता और
व्यवहारिक अनुभव को कम कर सकती हैl
12. सांस्कृतिक और
नैतिक चुनौतियाँ
डिजिटल शिक्षा
में छात्र विभिन्न वैश्विक संस्कृतियों से जुड़ते हैं, लेकिन कई बार यह अपनी स्थानीय संस्कृति और मूल्यों से दूरी भी पैदा कर
देता है। नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों का संचार डिजिटल
माध्यम से उतना प्रभावी नहीं हो पाता जितना पारंपरिक संवाद में होता है।
निष्कर्ष
डिजिटल शिक्षा
की चुनौतियाँ उतनी ही गंभीर हैं जितने इसके लाभ। डिजिटल विभाजन, गुणवत्ता का अभाव, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और मानवीय संवाद की कमी सबसे बड़ी रुकावटें
हैं। यदि सरकार, समाज और शिक्षा संस्थान मिलकर इन चुनौतियों का
समाधान करें, तो डिजिटल शिक्षा वास्तव में समानता, गुणवत्ता और सार्वभौमिकता की दिशा में क्रांति ला सकती है। डिजिटल शिक्षण पद्धति शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक, सुलभ, लचीला और व्यावहारिक बना रही है। यह केवल तकनीक
का प्रयोग नहीं बल्कि शिक्षा के नए युग की नींव है। चुनौतियाँ अवश्य हैं—डिजिटल
विभाजन, गुणवत्ता, स्वास्थ्य
संबंधी समस्याएँ—परंतु यदि इनका समाधान किया जाए तो डिजिटल शिक्षा भारत को
ज्ञान-सम्पन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यह स्पष्ट है
कि शिक्षा का भविष्य केवल किताबों और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल साधनों के साथ एक हाइब्रिड और नवोन्मेषी रूप धारण करेगा।
इसलिए डिजिटल शिक्षण पद्धति आज के समय में न केवल प्रासंगिक है, बल्कि अनिवार्य भी है।
References
Alenezi, M., Wardat, S., & Akour, M. (2023). The need of
integrating digital education in higher education: Challenges and
opportunities. Sustainability, 15(6), 4782.
Decuypere, M., Grimaldi, E., & Landri, P. (2021). Introduction:
Critical studies of digital education platforms. Critical Studies in
Education, 62(1), 1-16.
Dillenbourg, P. (2016). The evolution of research on digital
education. International Journal of Artificial Intelligence in
Education, 26(2), 544-560.
Gaikwad, R. B. (2024). The Role of Hindi in National Education: A
Historical and Pedagogical Analysis. Multidisciplinary Aspects of
Education.
Rachmad, Y. E. (2001). Digital Education Philosophy Theory. Education
Training Centre, Singapore.
Ross, J. (2017). Speculative method in digital education
research. Learning, Media and Technology, 42(2),
214-229.
Sharma, S. N. (2025). Indian Knowledge Systems–A Short
Review. Eduindex News.
Sharma, S. N., & Dehalwar, K. (2023). Council of Planning for
Promoting Planning Education and Planning Professionals. Journal of
Planning Education & Research, 43(4).
Williamson, B. (2016). Digital education governance: An
introduction. European Educational Research Journal, 15(1),
3-13.
.png)