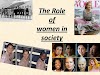श्रीमती डॉ. कोंडा चन्द्रा, व्याख्याता, एसटीएसएन सरकारी स्नातक महाविद्यालय, कदिरि
शोध सार: उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही नारी-उत्थान के लिए प्रयत्न शुरु होने लगे थे। समाज सुधारकों ने नारी के उत्थान के लिए शिक्षा,बाल-विवाह नियंत्रण, विधवा जीवन सुधार आदि को प्रधानता दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी की स्थिति में काफी बदलाव आया और आज भी वहअपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार निरंतर आगे बढ़ रही है। पचास-साठ तक आते-आते नारी की स्थिति में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला।अब साहित्यकारों ने भी नारी का वर्णन उसके सौन्दर्य, शील, आदर्श आदि के रूप में न करके उसे यथार्थता के धरातल पर अपने पात्रों के रूप मेंप्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है, जिससे साहित्य में भी क्रान्ति आ गयी। मेहरुन्निसा परवेज़ ने नारी को अपनी कहानियों में प्रधानता दी है। उन्होंनेनारी-जीवन के विविध आयामों को पाठकों के समक्ष उद्घाटित किया है। नारी-शोषण एवं समस्याओं पर जोर दिया है।
कुंजी शब्द: नारी समस्या, बेटे को प्रधानता देना, बेटी को बोझ समझना, विवाह की समस्या, दहेज-प्रथा, प्रेम की कुरबानी, अविवाहित जीवन कीविडम्बनाएँ, विवाहित जीवन की विडम्बनाएँ, बांझपन का बोझ, नारी के प्रति रूढ़िगत-विचार, अनमेल विवाह, वैधव्य के अभिशाप, परित्यक्त नारी, पर्दा-प्रथा, कामकाजी नारी की विडम्बनाएँ, नारी शोषण, निष्कर्ष।
नारी समस्या: स्त्री पर हो रहे अन्याय और अत्याचार का सिलसिला घर से शु डिग्री होता है। बचपन से उस पर अनेक प्रतिबंध लाद दिये जाते हैं।विवाह पश्चात उस पर पति का वर्चस्व अधिक देखा जाता है। उसे जीती-जागती, संवेदनाओं से भरपूर मनुष्य न समझकर, सिर्फ खिलौना समझा जानेलगा है। तन और मन की स्वतंत्रता तो दूर हँसने और मुस्कुराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसे अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ता है जिसकाउसके शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। हर दिन जिन्दगी और मौत के बीच जूझने के लिए मजबूर किया जाता है। "यह निरापद ही निश्चयपूर्वक कहाजा सकता है कि ऐसी कोई भी नारी जीवित नहीं होगी जिसने अपनी पीड़ा की मुक्ति के लिए कम से कम एक बार आत्महत्या के बारे में सोचा नहोगा।"1 व्यक्तित्व का अभाव, आर्थिक परतन्त्रता, राजनीतिक अवगणना, सामाजिक शोषण, दहेज-प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल-विवाह, विधवा-जीवन केलिए बाध्य, मानसिक शोषण, पाशविकता, बलात्कार, परपीडन-कामुक-पति द्वारा अत्याचार आदि कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिसका सामना पूरी दुनियाकी स्त्रियों को करना पड़ रहा है। ऐसी समस्याओं को मेहरुन्निसा परवेज़ ने अपनी कहानियों के द्वारा हमारे समक्ष रखा है।
बेटे को प्रधानता देना: आज भी भारतीय परिवारों में बेटियों को अधिकतर अवगणना ही मिलती आ रही है जो विशेषाधिकार बेटों को नसीब है, वह बेटियों के किस्मत में कहाँ? माता-पिता बेटे के जन्म को अधिक श्रेय मानते हैं क्योंकि, उनका विश्वास है कि बेटा उन्हें बुढ़ापे में सहारा देगा, अपनेवंश को आगे बढ़ायेगा, पुरखों को बलि देकर आध्यात्मिक लाभ पहुँचायेगा और अपने कर्मों द्वारा परिवार का नाम रोशन करेगा। "जमाना बदल गया है" कहानी में बहनें अपने भाई के किस्मत को सराहती हैं- "देखो लड़का होने का फायदा ........बिटियन की तो कोई कद्र ही नहीं, कोई पूछता नहीं, जैसेघूरे पर से उठाकर ले आए हो।"2
आज भी कई घरों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। यह माना जाता है कि घर का काम सीख लेने से उसका भविष्य सँवरजायेगा। मनुष्य के नज़रिये में कई बदलावों के आने के बावजूद भी अधिकतर लोग इस बात से सहमत हैं कि गृहस्थी संभालना स्त्री की जिम्मेदारी हैऔर इसका प्रशिक्षण उसे बचपन से ही दे दिया जाना चाहिए। "भोग हुए दिन" कहानी में सात साल की सोफिया घर पर बैठी लकडियाँ बेचती है, घरके दूसरे काम करती है और घर पर ही उसकी माँ उसे पढ़ाती है। लेकिन उसका भाई, जावेद स्कूल जाकर पढ़ता है। बेटियों को इस समाज में जन्म सेमरण तक लानतें सहनी पड़ती है। उसको जन्म देनेवाली माँ को भी इस प्रवृत्ति का हिस्सेदार बनना पड़ता है। "अपनी जमीन" कहानी में गोदावरी ने चारबेटियों को जन्म दिया, सास का ताना सुनना उसका दिनचर्या बन चुका था। पाँचवी बार बेटे को जन्म देकर उसने राहत की साँस ली, वरना "लड़कियोंकी माँ बनकर लानतें सहना" ही उसकी नियती बन चुकी थी। सास के लिए वह उसके बेटे का धन समाप्त करने खून चूसने वाली कुलच्छनी थी।उसकी सास इस बात को विस्मृत कर जाती है कि एक दिन वह भी बेटी थी।
बेटी को बोझ समझना: गरीबों के लिए बेटी कंधे पर बहुत बड़ा बोझ के समान है। उसे सपने देखने का कोई हक नहीं है। उसे अपने घर की हरस्थिति से समझौता करना पड़ता है। "सूकी बयड़ी" कहानी में होरा को अपनी बड़ी बहन के लिए अपने प्यार की बली चढ़ानी पड़ती है। वह अपने सारेदुखों को अपने अन्दर दफना देती है। "बेटी तो गरीब बाप के वास्ते भारी गठरी होए नी, न ढोए जाए, न उठाए जाए।"3 लड़कियाँ बचपन से हीभेद-भावपूर्ण बरताव को सहती हुई हीन-भाव से ग्रसित हो जाती हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। माँ-बाप के इस "बोझ" कोहल्का करने के लिए वे अपनी इच्छाओं और सपनों का गला घोंट देती हैं। माँ-बाप भी बेटी के भविष्य की चिन्ता किये बगैर ही अपना काम खत्म करकेगंगा नहा लेते हैं।
विवाह की समस्या: समाज ने विवाह को लड़कियों के जीवन की मंजिल माना है। भले ही आज इस नज़रिये में कुछ बदलाव जरूर आया है लेकिनऔसत भारतीय परिवारों में यही धारणा प्रबल है। बचपन से ही उसे विवाह के लिए तैयार किया जाता है। माँ-बाप के लिए यह एक विकट समस्याबनती जा रही है। अगर लड़कियाँ सुन्दर और गुणी हो तो गरीब होते हुए भी कहीं-न-कहीं रिश्ता हो ही जाता है लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो उसके लिएलड़का ढूँढना मुश्किल हो जाता है। विवाह को इतना महत्त्व दिये जाने के कारण लड़कियों पर इसका मानसिक दबाव पड़ता है। "बड़े लोग" कहानी मेंसूखी आपा का विवाह न हो पाने के कारण निराश है- "अम्मा कहती है, अल्लाह ने मेरा जोड़ा नहीं उतारा दुनिया में, क्या ऐसा हो सकता है? अल्लाहलूले-लंगडों का भी जोड़ा उतारता है, मेरा कैसे भूल गया।"4
लड़की का विवाह देर से होने पर, लड़की और उसके माँ-बाप, दोनों को अन्य लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं जिससे उन्हें मानसिक-संघर्ष के दौर सेगुजरना पड़ता है। "जाने कब" कहानी में शन्नो और उसके परिवार वालों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। "शन्नो के हाथ पीले करने का कब इरादाहै, भई? उम्र बढ़ रही है। इसके सामने की लड़कियाँ दो-दो बच्चों की माँ बन गई है। क्या जवानी का जिस्म अपने ही घर सड़ाकर दूल्हे को बूढ़ी हड्डियाँही पकडाओगे?"5 ऐसी बातें सुनकर शन्नो टूट जाती है और माँ-बाप भी अपने आपको कुसूरवार समझते हैं। लेकिन इसी आस में वे दिन व्यतीत करते हैंकि उनके भी अच्छे दिन आयेंगे।
दहेज-प्रथा: दहेज प्रथा के कारण लड़कियाँ घरवालों पर बोझ बनने लगी हैं। लड़की के जन्म से ही माँ-बाप इस चिंता में डूबे रहते हैं। अन्य अनेकसमस्याओं की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। विवाह के बाद, जिन्दगी भर के लिए माँ-बाप कर्ज में डूबे रहते हैं। "सूकी बयड़ी" कहानी में नीमड़ा और पत्नीमजदूरी करके घर-गृहस्थी चला रहे हैं। थोरा और होरा(बेटियाँ) का वे एक साथ विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन इसके खर्च के लिए पैसों के तौर परटेसुआ(बेटा) को दो साल के लिए बंधुआ मज़दूर बनाना पड़ता है। सारे घर की स्थिति ही डगमगा जाती है।
प्रेम की कुरबानी: अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर लड़कियाँ मुहब्बत तो कर लेती हैं लेकिन अधिकतर उसे अन्त तक निभाने में नाकामयाब होजाती हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हिन्दुस्तानी लड़कियाँ अब तक अपने आपको परंपराओं की बेडियों से मुक्त नहीं कर पायी हैं। "कयामत आगई है" कहानी में राबिया आपा अहसान भाई से प्रेम करती है लेकिन घरवाले उसका विवाह किसी और से कर देते हैं और उसे चुपचाप दुल्हन बननापड़ता है। वह घर में किसी को भी अपनी इच्छा बता नहीं पाती है। लेकिन आपा अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के मुताबिक करती है क्योंकि जोदुख उन्होंने झेले थे उसे वह अपनी बेटी को झलते नहीं देख सकती थी। अपनी मुहब्बत को सिर्फ कच्ची उम्र की नासमझी समझकर भुला देती है।लेकिन उनके दिल में अभी भी उस दर्द के निशान मौजूद हैं। "अब पहले का वह जमाना तो रहा नहीं जब मुहब्बत को सात कोठरियों के अन्दर छिपाकररखा जाता था। घरवाले जिससे भी बाँध दे, उसी के पीछे हो लिए। मुहब्बत काल कोठरी में बंद हुई तो बंद ही रह गई, पर मुँह खोलने की हिम्मत नहींहोती थी।"6 "सोने का बेसर" कहानी में कुमकुम और देबू की मंगनी होने वाली थी। लेकिन मंगनी के दिन देबू को कत्ल के जुर्म में जेल हो जाती है।दोनों घरों के सम्मान के कातिर कुमकुम की सगाई देबू के छोटे भाई, श्यामू से करा देते हैं। संस्कार और रीति-रिवाज़ के नाम पर कुमकुम की बली चढ़ादी जाती है और वह विरोध नहीं कर पाती हैं- "वह विद्रोह में एक शब्द नहीं बोल पाई थी। बडों के आगे कुछ नहीं बोल पाई थी।"7 आज भी भारतीयसमाज ने पूर्ण रूप से प्रेम-विवाह को अपनी स्वीकृति नहीं दी है। लेकिन परिवारवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर भी आज के युवक-युवतियाँजाने-अनजाने में अपने आपको ऐसे सम्बन्धों में फँसा हुआ पाते हैं। जब परिवारवालों द्वारा इन सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो मजबूरी मेंयुवा-पीढ़ी अपने बनाए सम्बन्धों को छोड़ या तोड़ पाती है। कहीं बच्चें अपने बुजुर्गों की मंजूरी के बिना भी इस डगर पर निकल पड़ते हैं।
अविवाहित जीवन की विडम्बनाएँ: सामाजिक मुहर के बगैर विवाह को कानूनी स्वीकृति नहीं मिलती है। "आकाशनील" कहानी में जम्मोबाईजिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिना "विवाह" किये एक पुरुष के साथ गुजारती है। वह उस आदमी के पाँच बच्चों की माँ भी बनती है। लेकिन उसपुरुष के मृत्युपरान्त कानून उसे पत्नी का दर्जा न देकर उस पुरुष के पिता को कानून उत्तराधिकारी घोषित करता है। जम्मोबाई के पास दर-दर की ठोकरेंखाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। "बरसों मैं उसके साथ रही......उसके पाँच-पाँच बच्चों की माँ बनी। जिन्दगी-भर वह मेरे शरीर कोरौंदता रहा और जब आज मैं चौराहे पर आ खडी हूँ तब सरकार, आपने मुझे एक नाजायज़ औरत करार दे दिया।"8
जिन्दगी-भर पति-पत्नी के रूप में साथ रहने पर भी समाज द्वारा वह अविवाहित ही समझी गयी और उसे "बदचलन" का खिताब दिया गया।कानून की तरफ से यहाँ न्याय हुआ है लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से उस औरत और पाँच बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इससे ये बच्चे भीगैरकानूनी कार्यों के दौड में शामिल होने की संभावना है।
विवाहित जीवन की विडम्बनाएँ: विवाह पश्चात नारी को नये माहौल में अपने आपको व्यवस्थित करने में वक्त लगता है क्योंकि उसके पितृ-गृहसे अलग वातावरण उसे पति के घर में मिलता है। विवाह के बाद नारी से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी यादों, स्वप्नों और खुशियों कोभुलाकर सिर्फ अपने पति और उसके घरवालों के लिए जीवन बिताये। पत्नी को पति की इच्छा के मुताबिक अपने आपको ढालना पड़ता है। इसकशमकश में उसका पूरा व्यक्तित्व ही बिखर जाता है। "लौट जाओ बाबूजी" कहानी में आशा को भी इसी दौर से गुज़रना पडता है। अन्तरजातीयविवाह करने के बावजूद भी गिरीश ने आशा से यही उम्मीद की थी जिससे आशा का भी मानसिक संघर्ष से गुज़रना पड़ता है।
"पुरुष नारी पर केवल अपना धर्म, संस्कार ही नहीं लादता, बल्कि अपने रिश्ते-नाते, अपना अतीत, अपनी यादें और अपना ही तरह का जीवनढोने पर मजबूर करता है......ब्याह के बाद केवल रिश्ते, समाज, परिवेश ही नहीं बदलता, बल्कि समूची-की-समूची जिंदगी ही बदल जाती है।"9विवाह पश्चात जब लड़की बहु बनकर ससुराल पहुँचती है तब मानो उस घर का सारा काम उसी के इन्तजार में है। कदम रखते ही घर की जिम्मेदारीउसके कंधों पर आ जाती है। अगर वह कामकाजी (नौकरीपेशा) हुई तो उसे दुहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बीमारी के दौरान भी घर का सारा कामउसी को करना पड़ता है। "अपने-अपने लोग" कहानी में सुमन गृहस्थी और नौकरी के बीच दिन-रात पिसती रहती है। कोई भी उसका हाथ नहीं बंटाताहै क्योंकि घर को संभालना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। "दादी, मैं महीना-भर जबलपुर क्या रह गई, घर भूतों का डेरा बन गया है। देखो न,घर में इतने लोग रहते हैं; पर जैसे काम करने के लिए मैं ही अकेली हूँ .....छुट्टी के दिन भी मुझे आराम नहीं मिलता।"10 अगर विवाह के बाद नारी कोपति से कोई खुशी और प्यार नहीं मिलता है तो भी वह उस घर को संवारती है। वह पति की हर खुशी का ख्याल रखती है। "अपने होने का एहसास" कहानी में पति द्वारा पत्नी को कभी भी खुशी का एक पल भी नसीब नहीं होता है। अनाथ होने के कारण उसे बचपन में बुआ ने पाल-पोसकर बड़ाकिया है। जवान होते ही एक विधुर से शादी करा दी जाती है। पति के घर में वह एक फालतू सामान की तरह पड़ी रहती है। माँ बन जाने के बाद भीउसका पति बच्चे को उससे अलग कर देता है। वह उस घर को हमेशा की तरह सँवारती रहती है साथ ही अपनी खुशी के लिए भी तरसती है। "दीमकघर बनाती है और उसमें रहता सांप है.....उसे भी यही बात हमेशा औरत के लिए लगी। दीमक की तरह वह घर बाँधती रही और साँप की तरह वहरहता रहा?"11
विवाह से पूर्व जो स्त्री बौद्धिक-स्तर पर आगे थी, जिन्दगी की हर चुनौती को स्वीकार करने को तत्पर रहती थी, वह विवाह पश्चात सिमटकरघर की चार-दीवारी में अपने आपको कैद कर लेती है। ऐसा न करने पर पति और पत्नी के अहं में ठकराव होने की गुंजाइश रहती है इससे दाम्पत्यजीवन में दरारें पैदा हो सकती हैं। "खामोशी की आवाज़" कहानी में अनु विवाह-पूर्व कॉलेज की हर गतिविधियों में शामिल होती थी और उसकी इसीखूबी के कारण रमेश ने उससे विवाह किया था। लेकिन विवाह-पश्चात उसकी दुनिया घर के अन्दर सीमित हो जाती है। "जिसका क्षेत्र केवल रसोई सेबेडरूम तक हो वह अब सोच ही क्या सकती है।"12
विवाह-पश्चात जब लड़की पहली बार अपने मायके आती है तब ससुराल लौटते वक्त उसे नये कपडे दिलवाने का रिवाज़ अनेक जगहों परप्रचलित है। लेकिन जिन घरों में आमदनी कम होती है उन घरों के लिए यह प्रथा भारी पड़ती है। "चमड़े का खोल" कहानी में शुभी अपने पति, देव केसाथ मायके आती है। लेकिन बाबूजी गाँव चले जाते हैं और शुभी से मिलने नहीं आते क्योंकि अगर शुभी को नये कपडे नहीं दिलवाये गये तो घर मेंविवाद खडे होने की संभावना है और इससे घर की शांति भंग होने का डर है। "एकाएक उसे लगा था, शादी के बाद भी वह बाबूजी पर भार है, कपड़ादेना पड़ता है इसलिए बाबूजी उसके आने पर खुश नहीं होते, जैसे उसके और बाबूजी के बीच में कपडे की दीवार है।"13 बेटी को ब्याह दिये जाने केबाद उसके ससुराल में उसके माता-पिता का आकर रहना बुरा माना जाता है। अगर उनके पास रहने का और कोई ठिकाना न हो तो भी वे अपनी बेटी केपास आकर नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारे संस्कार इसकी इज़ाजत नहीं देती है। "अपने-अपने लोग" कहानी में सुमन की बाई(माँ) गाँव में अकेली रहतीहै। सुमन अपनी कमाई के रूपये भी बाई को नहीं भेज पाती है। वह चाहती है कि अपनी बाई को अपने पास लाकर ठहरायें लेकिन उसके ससुरवालेसमाज और संस्कार को बीच में घसीटते हैं। "मगर बाई क्या बेटी के घर रह लेंगी? उनके इतने पुराने संस्कार, फिर समाज के लोग क्या कहेंगें?"14
ब्याहत बेटी का ससुराल छोड़कर मायके आकर रहना ठीक नहीं माना जाता है। हमारी पुरानी रीतियों के अनुसार अगर एक बार बेटी घर सेडोली में विदा होकर जाती है तो उसे वापस अर्थी पर ही ससुराल छोड़ना चाहिए। वहाँ के जुलमों और दुखों को सहना उसका नसीब माना जाता है।"अम्मा" कहानी में सुमन और उमा, माँ की इसी नज़रिए के कारण ससुराल में उम्रकैद काटने को मजबूर हो जाती है। "आकृतियाँ और दीवारें" कहानीका मुख्य नारी-पात्र तलाक-पश्चात मायके वापस आता है। आत्मनिर्भर होने पर भी उसे उपेक्षा भरी नज़रों का सामना करना पड़ता है। "कुआंरी लड़कीजीवन-भर माँ की दहलीज़ पर रह सकती है, पर ब्याही लड़की आँख में पडे बाल-सी खटकती है। उपेक्षा से भरी आँखें....और आँखों में भरा पानी,एकान्त में रो लेने को मन।"15 "बूद का हक" कहानी में जब बेटी के आत्मसम्मान को टेस पहुँचती है तब वह वापस अपने मैके लौट आती है। उसेयकीन होता है कि उसके घरवाले उसकी भावनाओं को जरूर समझेंगें और उसे सहारा देंगें लेकिन घर आकर उसे घरवालों की अवगणना का सामनाकरना पड़ता है। उसके पिता उसकी भावनाओं को समझते हैं और इस मुसीबत के वक्त वह अपनी बेटी का साथ भी देते हैं। लेकिन उन्हें भी घर के अन्यसदस्यों का ताना सुनना पड़ता है। घरवाले बेटी को दुनिया-जहान की कसम दिलाकर वापस भेजना चाहते हैं। "नहीं, उससे कह दो, वापस राहुल के घरलौट जाए। शादीशुदा लड़की का घर बैठना क्या अच्छी बात है.....कैसे बाप हो तुम! लड़की को घर पर बैठाकर खानदान में नाक नीची करवाओगे! दुनिया क्या कहेगी?"16 हमारे समाज की खोखली रूढ़ियों के कारण विवाह-पश्चात नारी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जिन सपनों कोसंजोये हुए वह ससुराल की दहलीज़ पर पहुँचती है वही सपने कुछ दिनों के पश्चात बिखरते हुए नजर आते हैं। मायका तो पराया हो ही जाता है, ससुराल भी अपना नहीं हो पाता है।
बांझपन का बोझ: हमारे समाज की नारी को बांझपन एक अभिशाप प्रतीत होता है। यह माना जाता है कि नारी अपनी पूर्णता को तभी प्राप्तकरती है जब वह माँ का दर्जा हासिल कर लेती है। बच्चों से ही उसे समाज और परिवार में प्रतिष्ठा हासिल होती है। "सूकी बयड़ी" कहानी में थोरा माँनहीं बन पाती है और इस कारण उसे पति के अत्याचारों को सहना पड़ता है। घर में सौतन लाकर पति उसका अपमान करता है लेकिन फिर भी वह चुपरहती है क्योंकि वह इसे अपना ही दोष समझती है। "भगवान ने ही जब मेरे भाग्य को सूकी बयडी बना दी, किससे कहूँ? बयडी का भाग्य जाणे नी,ऊँची रहे है, पर पानी नी ठहरे, फसल नी उगे। जाके खेत माँ बयडी होए वह किसान तो माथा फोड़े नी। उसकी जमीन तो बेकार चली जाए।"17 माँ नबन पाने के कारण उत्पन्न मानसिक द्वन्द्व से गुजरती नारी का वर्णन "बन्द कमरों की सिसकियाँ" कहानी में किया गया है। मौना को अपनी जिन्दगीबेमकसद प्रतीत होती है। जब उसे बांझपन का एहसास बार-बार दूसरों द्वारा करवाया जाता है तब उसका दुख और ज्यादा गहरा हो जाता है। मौना औरउसका पति, शंकर दोनों ही अपने चारों ओर एक दायरा बना लेते हैं। लेकिन संतान के अभाव में पति-पत्नी के बीच में भी खालीपन उत्पन्न हो जाताहै।
संतति के अभाव में स्त्री की छटपटाहट को "बंजर दोपहर" कहानी में व्यक्त किया गया है। संतान के कमी के कारण पत्नी की ओर से पतिउदासीन हो जाता है। परिणामत: पत्नी घुटन, छटपटाहट और अकेलापन से ग्रसित हो जाती है। बचपन से दिये गये संस्कारों के कारण हमारे समाज मेंनारी की यह मानसिकता है। हिन्दू धर्म के अनुसार विवाह का प्रथम लक्ष्य संतानोत्पत्ति माना गया है और नि:संतान व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वारा बन्दबताया गया है। स्त्री-पुरुष के जीवन में रिक्तता को भरने का काम संतति करती है। यह भावनात्मक आवश्यकता स्त्री-पुरुष के लिए समान है। पुरुष केलिए यह अन्य माँगों में से एक है लेकिन नारी के लिए यह जैसे अनिवार्यता ही है।
नारी के प्रति रूढ़िगत-विचार: रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ी नारी आज एक-एक करके उन्हें तोड़ने में कामयाब हो रही है। शिक्षा औरपाश्चात्य-सभ्यता के प्रभाव ने नारी को अपनी स्थिति का पूर्ण परिचय करा दिया है। लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है।इसके लिए जिम्मेदार वह खुद भी है क्योंकि वह पुरुष के अधीन रहना चाहती है। "ओढ़ना" कहानी में रानी का भाई अपने पत्नी को सिर्फ इसलिएमारता है कि उसने घर के बाहर के आदमी से बात करने की हिम्मत दिखाई। रानी अपने भाभी से कहती है कि अपनी नाराजगी ज़ाहिर करने के लिएसात रातों तक वह भी अपने पति से बात न करें। लेकिन भाभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती है। रानी रूढ़ियों में जकड़ी स्त्रियों के बारे में कहती है-"औरत की जात मार खाने के लिए ही होती है, मरद कितना भी जुल्म करें, बदले में उसे रूठना भी नहीं आता, पति मार-मारकर प्राण ले लेगा और वहउसके लिए करवाचौथा का व्रत करेगी।"18
"सोने का बेसर" कहानी में संस्कार और रीति-रिवाज के जंजीरों में जकड़ी कुमकुम दूसरों के फैसलों पर अपनी जिन्दगी जीने के लिए मजबूरहो जाती है। ऐसी स्थितियों से जूझने के लिए नारी की मानसिकता में बदलाव आना बहुत जरूरी है। इसके लिए माता-पिता, घर के अन्य सदस्यों औरपूरे समाज को अपना योगदान देना होगा। इन रूढ़िगत विश्वासों को तोड़ने का समय बीत चुका है। अगर नारी सचमुच स्वतंत्र होना चाहती है तो उसकेलिए इन बन्धनों को तोड़ना अनिवार्य है। इसके लिए उसमें आत्मविश्वास और धैर्य की जरूरत है।
अनमेल विवाह: जिस घर में बेटी को बोझ समझा जाता है, वहाँ उसका विवाह माता-पिता किसी प्रकार निपटा देना चाहते हैं। इस उधेड़-बुन में वेकभी-कभी उम्र में काफी बडे व्यक्ति से उसका विवाह करा देते हैं। भले ही इस स्थिति में आज सुधार आयी है फिर भी समाज में यत्र-तत्र यह बातकायम है। अनमेल विवाह का तात्पर्य है जिस विवाह में वर या वधू में से किसी एक का अन्य के लायक या मुताबिक होना। इसमें किसी एक का मेलठीक प्रकार नहीं हो पाता है। इससे दाम्पत्य जीवन सन्तुष्ट नहीं हो पाता है। "नंगी आँखोंवाला रेगिस्तान" कहानी में नारी का पति उससे दुगुनी उम्र काहै। अधेड़ पति से नीरा को पिता जैसा स्नेह मिलता है। नीरा अपनी ही आग में सुलगती रहती है। उसकी जरूरतों को पति समझ नहीं पाता है क्योंकिदेव का यौवन बीत चुका है। नीरा को पति जैसा प्रेम देव से कभी भी नहीं मिल पाता है। उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी- "उसे अपना जीवन पिंजरे मेंबंद तोता-मैना सा लगता, जो लोह के सींखचों में है और जिसे समय-समय पर खाना-पानी मिल जाता है और कभी-कभी मालिक की पुचकार, बस।"19
अनमेल विवाह के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से नारी पर असर पड़ता है। एक ओर वह मानसिक रूप से तालमेल नहीं बिठा पाती हैवहीं दूसरी ओर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण जिन्दगी भर तड़पती रहती है। ऐसी स्थिति में किसी तीसरे की तरफ झुकावस्वाभाविक है और इस कारणवश दाम्पत्य जीवन की नींव हिलने लगती है।
वैधव्य के अभिशाप: समाज सुधारकों एवं साहित्यकारों के सम्मिलित प्रयत्न के द्वारा समाज में विधवाओं की समस्याओं का काफी हद तकनिवारण हुआ है। लेकिन नये परिवेश में नई समस्याओं का आगमन हुआ है। अब नारी शिक्षित एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुकी है और इस कारणउससे कोई जोर-जबरदस्ती नहीं कर सकता है। विधवा-विवाह को समाज ने बहुत पहले ही स्वीकृति दे दी है। लेकिन कुछ उच्च-वर्ग के परिवारों में अबभी पुरानी रूढ़ियों के मिथ को तोड़ना मुश्किल हो गया है। "जीवनमंथन" कहानी में अमित के देहान्त के बाद नंदिता से एक-एक करके सब कुछ छिनजाता है। बेटे पर ससुरालवाले कब्जा कर लेते हैं। सारे सुखों से उसे वंचित कर दिया जाता है। शुभकार्यों में भाग लेना और श्रृंगार करना उसके लिएवर्जित हो जाता है। उसे अपशकुन माना जाता है। उसे लगता है मानो उसकी जिन्दगी में अकाल पड़ गया है। "तीसरे दिन जब उसे सफेद कोरी साडीपहनाई गई तब वह दहाड़ मारकर बिलक उठी थी। सब छिना जा रहा था.....अमित की तो लाश जलाई गई थी, पर उसे तो जीते-जी लोगों ने जलादिया था। जीते-जी सफेद कफन पहना दिया था।"20 "बौना मौन" कहानी में नीतू के पति के देहान्त के बाद वह बेसहारा हो जाती है। पति की पेंशनपाने के लिए उसे दफतरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अंत में इसके लिए उसे साहब को सन्तुष्ट करना पड़ता है। जब वह दूसरे विवाह के बारे मेंसोचती है तब उसके पिता उसे बच्चों की दुहाई देते हैं जो खुद भी पत्नी के देहान्त के बाद अकेलेपन से घबराकर दूसरा ब्याह करना चाहते थे। "नीतू, देख बच्चे हैं, कोई गलत कदम मत उठाना, बेटी! औरत के आगे उसके बच्चे लक्ष्मण-रेखा की तरह होते हैं, जिन्हें वह कभी लांघ नहीं पाती, इस बातका ध्यान हमेशा रखना।"21
"वीराने" कहानी में माँ और बेटी दोनों ही विधवा की जिन्दगी जी रहे हैं। प्रेमी के देहान्त के बाद बेटी अपने आपको विधवा समझती है औरपति के देहान्त के बाद माँ अपने आपको समाज से अलग कर लेती है। हमारे समाज में पति के देहान्त के बाद पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। उसकासजना-संवरना और शुभ कार्यों में शामिल होना सिर्फ पति के जीवित रहने तक ही सीमित है। इस कहानी में माँ ने इस ओर संकेत किया है- "छि: छि: पागल है क्या, मैं विधवा ऐसी साडी पहन सकती हूँ।"22
"आदम और हव्वा" कहानी में उमी के पति, देव की दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके बाद उमी का परिचय महिम से होता है और यह प्रेम मेंबदलने लगता है। महिम उसके भूतकाल से परिचित है और उससे विवाह करना चाहता है। लेकिन ईर्ष्यावश उमी के भूतकाल को वह भुला नहीं पाता हैऔर उस सम्बन्ध को तोड़ देता है। पुरुष हमेशा से यही चाहता आ रहा है कि वह स्त्री के जीवन में आने वाला पहला पुरुष हो।
"हत्या एक दोपहर की" कहानी में नूपुर के पति के देहान्त के बाद वह अपने मायके आ जाती है। वह आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी उसे औरउसके बेटे को मायके में सम्मान नहीं मिलता है। आज विधवा नारी की सबसे बडी समस्या असुरक्षा की भावना है। समाज में, पुरुष वर्ग मौका हाथलगते ही बेसहारा नारी पर चील की तरह झपट कर उसका चीर फाड़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्त्री को मान-मर्यादा का पाठ पढ़ाकर चुप करा देतेहैं। एक विधवा नारी को अन्य सुहागिन स्त्रियाँ अपशकुन मानती हैं। चूंकि उसे किसी का साथ नहीं प्राप्त होता, वह अपने आपको बहुत अकेली पातीहै। इस असुरक्षा और अकेलेपन को मिटाने के लिए जब वह पुनर्विवाह करती है तो वहाँ भी उसे इज्जतपूर्ण और तनावहीन जिन्दगी मिलना मुश्किल है।
परित्यक्त नारी: बदलते सामाजिक परिवेश के कारण सम्बन्धों का बिखराव आज हर कहीं नजर आ रहा है। दाम्पत्य जैसे आत्मीय सम्बन्धों का भीविघटन होने लगा है और इससे तलाक की संख्या बहुत बढ़ गयी है। नारी की शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता उसे अपनी आत्मसम्मान को दाँवपर लगाने नहीं देती है। समाज में यह भ्रम विद्यमान है कि तलाकशुदा नारी खुद अपना घर तो तोड चुकी है साथ ही दूसरे घरों को भी बर्बाद कर देनाचाहती है। पुरुष वर्ग उसे हमेशा से इस्तेमाल करने की ताक में रहता है। "नंगी आँखोंवाला रेगिस्तान" कहानी में देव से तलाक के पश्चात नीरा कीमुलाकात अमित से होती है और वह उसे ही अपनी मंजिल समझ बैठती है। लेकिन अमित कोई भी नीरा से अपने बेटे का पीछा छुडवाना चाहते हैं। इसवजह से नीरा को हर जगह अपमानित होना पड़ता है- "अपमान, लज्जा और आँसुओं से उसका चेहरा फीका पड़ गया था। अपने में और कोठे की वेश्यामें उसे कोई फर्क नहीं लग रहा था।"23 "ढ़हता कुतुबमीनार" कहानी में सपना के पति, राहुल का विवाहेतर सम्बन्ध है और इसलिए वह उससे तलाकले लेती हैं। लेकिन इस कारण उसे परिवार के लोग और समाज से अपेक्षापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वह जिन्दगी से जूझने के लिएअकेली पड़ जाती है। "साल की पहली रात"45 और "आकृतियाँ और दीवारें" कहानियों के प्रधान नारी पात्र तलाक पश्चात अपने मायके में रहते हैं।आत्मनिर्भर होने के पश्चात भी घरवालों से उन्हें उपेक्षा मिलती है।
"प्राण प्रतिष्ठा" कहानी के बेनिप्रसाद बहुत बड़े सन्त-महात्मा बन जाते हैं लेकिन उनकी पत्नी पर दुखों का पहाड-सा टूट पड़ता है। बेनिप्रसादअपनी पत्नी तुलसीबाई को पूरी तरह विस्मृत कर देते हैं। अचानक वर्षों बाद वह एक प्रश्न चिह्न बनकर उनके सम्मुख आ खड़ी होती है। लेकिन तबतक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उनकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह करके सुखी जिन्दगी व्यतीत कर रही थी। "आप सबके सुखी रहने काआशीष देते हैं, किंतु मुझे विपदा में छोड़कर आप भाग गए थे। आपके परिवारवालों ने मुझे अपमानित कर पीहर भेज दिया।"24 तलाकशुदा नारी कोउपेक्षा, अपमान और असुरक्षा का भाव जकड़ लेता है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए उसे खुद प्रयत्नशील होना चाहिए।
पर्दा-प्रथा: शहर में तो यह प्रथा अब न के बराबर देखने को मिलती है लेकिन गाँवों में अब भी स्त्रियों के मध्य यह प्रथा विद्यमान है। नारी को दासीबनाये रखने की बहुत बड़ी भूमिका इसने निभायी है। "जगार" कहानी में गोमती गाँव की महिला सरपंच बन गयी लेकिन उसकी सास उसे घूँघट मेंरखना चाहती है। राजनीतिक क्षेत्र में नारी ने प्रवेश कर लिया है, आज तैंतीस प्रतिशत संवरण पर भी विचार-विमर्श हो रहे हैं, अनेक जगहों पर चुनाव मेंउम्मीदवार के तौर पर भी वह खडी ही रही है लेकिन फिर भी समाज उसे चार दिवारी और आँचल में ढाँक कर रखना चाहता है क्योंकि औरत घर कीइज्जत मानी जाती है। "बैठ-ठाले की महाजनी हाथ लग गई। अब बहू मुँह उघाडे फिरेंगी! घूँघट में मुँह नहीं ढ़के जाते, बेटा, घूँघट में तो अपनी इज्जतढकी जाती है।"25 नारी के शिक्षित होने के कारण गाँवों से भी धीरे-धीरे यह रिवाज़ खत्म हो चली है। लेकिन इस प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म करने मेंअभी और संघर्ष करना पड़ेगा।
कामकाजी नारी की विडम्बनाएँ: बौद्धिक या शारीरिक क्षमता के उपयोग से, कुशल या अकुशल श्रम के माध्यम से, घर या घर के बाहर कार्यकरके अर्थोपार्जन करनेवाली महिलाएँ "कामकाजी महिलाएँ" हैं। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नारी ने अर्थोपार्जन के लिए घर की दहलीज़ को पारकिया है। इसका कारण आर्थिक विवशता, शिक्षा का प्रसार एवं सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव है। नारी के इस बदले हुये रूप के साथ ही अनेक नईसमस्याएँ भी सामने आई हैं। दुहरी जिम्मेदारी निभाने वाली कामकाजी नारी शारीरिक व मानसिक श्रम से काफी थक जाती है। उसकी जिन्दगी एकमशीन की तरह चलती है। नारी के अर्थोपार्जन से उसे तथा उसके परिवार को उच्च-जीवन-स्तर की प्राप्ति अवश्य होती है लेकिन फिर भी घर केअन्य-सदस्य घरेलू कामों में उसका हाथ बँटाने से कतराते हैं। "अपने अपने लोग" कहानी में सुमन सबेरे पाँच बजे से काम पर लग जाती है। नाश्ता एवंलंच तैयार करके वह सात बजे घर से निकलती है। बेटी को स्कूल छोड़ती हुई, वह दफतर जाती है। दोपहर को घर वापस आती है। घर में दो-तीनबचों को ट्यूशन पढ़ाती है। शाम को फिर रसोई का काम संभालती है। इन सारे कामों में उसे मदद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि घरेलू काम कीजिम्मेदारी सिर्फ बहू की मानी जाती है। "सारा काम कर रात जब बिस्तर पर लेटती तो लगता, जैसा सारी सृष्टि का चक्कर काटकर लौटी है.........दूसरेदिन फिर वही भागा-दौडी।"26 परिवार के आय के स्रोत एवं जीवन के स्तर में वृद्धि लाने के बावजूद भी कामकाजी नारी को अपनी कमाई पर अधिकारनहीं है। "अपने-अपने लोग" कहानी में सुमन माँ की मदद छुप-छुपकर ही कर पाती है। उसके वेतन पर उसके पति का अधिकार है। "पत्नी से काम भीकरवाते हैं और उसमें गुलामों-सा व्यवहार करते हैं। नारी को अपने कमाए रुपए पर भी उसका अपना अधिकार नहीं था...........पत्नी की कमाई परपति का अधिकार था।"27 निम्न-मध्यवर्ग में कामकाजी नारी घर के आय में वृद्धि लाती है और कभी कभी पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालती है। ऐसेमें अगर वो विवाहित न हो तो घरवाले अपने स्वार्थ के लिए उसका विवाह नहीं कराना चाहते हैं। "सज़ा" कहानी में उमा के एम.ए. कर लेने पर उसकेब्याह की बात चलने लगती है। लेकिन दहेज़ के कारण कहीं भी विवाह तय नहीं हो पाता है। घर में सभी उसके ब्याह को लेकर चिंचित हैं। इस दौरानवह किसी तरह अपने बाबूजी को मनवाकर बैंक में नौकरी करने लगती है। इसके साथ ही उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। इसके कारण किसीको भी उमा की शादी की जल्दी नहीं रहती और उसका विवाह एक गैरजरूरी मसला बनकर रह जाता है। पूरे दो साल के पश्चात उमा खुद ही अपनीशादी की बात को घर में उठाती है। इससे घर में जैसे कोहराम मच जाता है। उसके द्वारा जो एक बंधी-बंधायी रकम महीने की पहली तारीख को घरपहुँचती है उसे घरवाले खोना नहीं चाहते हैं। यही उमा के कामकाजी होने की त्रासदी है। "अकेला गुलमोहर" कहानी में सुधा का विवाह भी उसके भैयाइसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह कमाती है। इस बात को लेकर सुधा के दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। "तुम कसाई हो। तुम चाहते हो हरआदमी कमाकर लाये तो खाये। इसलिए तुमने सुधा की शादी नहीं की। सुधा दूसरे के घर चली जाएगी तो बंधे हुए दो सौ कौन लाकर देगा?"28
"विद्रोह" कहानी में नीना निम्न-मध्यवर्ग से है और घर की सारी जिम्मेदारी उस पर है। उसके विवाह के बारे में माता-पिता द्वारा न तो कभीसोचा गया और न किसी ने इस बारे में बात उठायी है। वह घर की आर्थिक-स्थिति सुधारने में ही पूरी जिन्दगी लगा देती है। इन समस्याओं के अध्ययनके पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि इसमें अधिकतर समस्याएँ नये रूप में आज हमारे सम्मुख हैं। इसका कारण भले ही रूढ़िवादी विश्वासएवं पुरुष का अहं है। बाह्य रूप में नारी ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन आज भी औसत नारी की स्थिति को देखा जाय तो निराशा ही हाथ लगती है।सौ साल पुरानी उसकी स्थिति से कुछ ज्यादा बदलाव उसमें नहीं आया है। उदाहरण स्वरूप थोड़े से लोगों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचसकते हैं कि नारी को सब कुछ हासिल हो चुका है जिसके लिए उसने संघर्ष किया था। उसका संघर्ष आज भी जारी है।
नारी शोषण: नारी के प्रति हो रहे हिंसा इस दुनिया में सबसे व्यापक स्तर पर हो रहे मानव अधिकार के दुरुपयोग का परिणाम है। इसके विषय मेंकोई भी देश अपवाद नहीं है। लड़कियों और स्त्रियों पर उसके लिंग के कारण अगर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो वह "नारी शोषण" कहलाता है।संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1993 के जनरल असम्बली में "नारी हिंसा विलोपन"की घोषणा करते हुए "अनुच्छेद-एक"में "नारी हिंसा" को परिभाषित कियाहै- "नारी के प्रति कोई भी प्रवृत्ति, जो लिंग आधारित हिंसा हो, जिसका परिणाम या संभावनीय परिणाम शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक हानी यापीड़ा हो, ऐसी प्रवृत्ति की धमकी, स्वेच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक या व्यक्तिगत जिन्दगी में हो, यह भी इसकेअन्तर्गत है।"29 इस बात की पुष्टि "अनुच्छेद-दो" में विस्तारपूर्वक दिया गया है। नैतिक मूल्यों में हो रहे गिरावट और यौन-चेतना के निरंतर बढ़ने से यहअनाचारता बढ़ती जा रही है। शोषण की प्रक्रिया इतनी प्रबल, भंयकर और व्यापक हो रही है कि आत्मविश्वास से पूर्ण सशक्त नारी भी डगमगा जातीहै। नारी का सबसे ज्यादा शोषण वह पुरुष करता है जिसे वह भली-भाँति जानती है- यह आदमी उसका पति या परिवार का ही कोई अन्य सदस्य होताहै। भारतीय स्त्रियाँ आज दोहरी शोषण का शिकार हो रही हैं। इस विषय पर प्रसिद्ध कथाकार मृदुला गर्ग ने अपने मत को स्पष्ट किया है- "स्त्री होने कीवजह से होने वाला शोषण, बलात्कार और वेश्या बनाए जाने तक सीमित नहीं है। पैदा होते ही, या बाद में पति की चिता पर उसकी हत्या होती है।खाने को उसे कम दिया जाता है और शिक्षा से वंचित रखा जाता है।"30
लड़कियों को समाज में जीने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। अगर वह जन्म ले लेती है तो उसे जिन्दा रहने का अधिकार नहीं दियाजाता है। "अपनी ज़मीन" कहानी में गोदावरी ने चार लड़कियों को जन्म दिया जिससे वह और उसकी बेटियाँ, सास के द्वारा प्रताडित होती हैं। जबउसकी तीसरी बेटी ने जन्म लिया था तब सास दो दिन तक आँचल में तंबाकू बाँधे घूमती रही थी। वह नवजात शिशु की तालु में तंबाकू रखना चाहतीथी जिससे बच्ची का देहान्त हो जाय। दाई ने गोदावरी को सतर्क कर दिया था इसलिए वह एक पल के लिए भी बच्ची को अपने से अलग नहीं करतीथी। सारी रात जागकर काटती थी। अन्त में हारकर सास ने बच्ची को मारने का इरादा छोड़ दिया लेकिन उसका क्रोध गालियों के रूप में निकलनेलगता है। चूल्हे की जलती लकडियों से वह लड़कियों को मारती है।
"अपने होने का एहसास" कहानी में एक ऐसी नारी का वर्णन है जो अपने संपूर्ण वैवाहिक जीवन में उपेक्षित और अपमानित रही। उसने अपनेपति को परमेश्वर माना लेकिन पति ने उसे अपनी वासना को तृप्त करने वाली माँस का पिंड ही समझता रहा। "साल की पहली रात" कहानी में एलमाको उसका भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है। जिन्दगी भर अपनी बहन की हिफाज़त करना जिस भाई का कर्तव्य था, वही भाई उसेभूखे भेड़िये के सामने डाल देता है। जब एलमा को इस बात की समझ आती है तब तक बात बहुत आगे बढ़ जाती है। "कयामत आ गई है" कहानी मेंआपा अपने मामा की हवस का शिकार बनती है। "शनाख्त" कहानी में बती के पिता कच्ची शराब बनाता है और खुद भी हमेशा नशे में धुत रहता है।नशे में वह लोक-लाज भूलकर बती की माँ की तरफ "भूखे शेर" की तरह झपटता है। उसकी माँ बती को पिता की नजरों से बचाये रखना चाहती हैलेकिन एक दिन उसका भी अंजाम वही हो जाता है जो माँ का रोज होता है। नशे में पिता को बेटी भी सिर्फ एक नारी देह मात्र ही लगता है। पुरुष कीनिगाह में औरत सिर्फ वासना को तृप्त करने का साधन है। "पत्थर वाली गली" कहानी में जेबा का बलात्कार होता है। वह शारीरिक और मानसिक रूपसे पीढ़ित होती है। इसी कहानी में जेबा के पिता अफीम की तस्करी करता है। शराब के नशे में वह अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ बाँटता है।लेकिन जब जेबा की माँ उसके दोस्त के बच्चे की माँ बन जाती है तब वह उसकी पिटाई करता है और घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है। "नंगीटहनियाँ" कहानी में जैतुन की माँ परिवारवालों के अत्याचार को मौन होकर सहने वाली नारी का प्रधिनिधित्व करती है। वह पत्नी और माँ होकर भीउसके सुख और अधिकार से वंचित है। पति के लिए वह वासना को तृप्त करनेवाली माँस-पिंड है तो ससुराल के अन्य सदस्यों के लिए वह नौकरानी है।"दूसरी-तीसरी रात से ही वह जान गई थी कि वह अकेली उनकी पत्नी नहीं है। बहुत-सी पत्नियों की लड़ी में उसे भी पिरो दिया गया है। यहीं आकरउसने जाना कि शारीरिक सुख ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है।"31 मध्यप्रदेश के रत्लाम से नीमच तक एक सौ पचास किलोमीटर के राज्यमार्ग मेंबाँछडा जाति के लोग रहते हैं। वे अपने परिवार की लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाते हैं। ये लोग मन्दसौर, नीमच, रत्लाम, इन्दौर, उज्जैन और राजापुरजिले में रहते हैं। वे मूलत: मन्दसौर जिले के निवासी थे जो पहले ग्वालियर राज्य में रहते थे। यहाँ के पुरुष आलसी और स्वप्नविलासी हैं। रीति केअनुसार घर की बड़ी बेटी को धंधे पर बिठाया जाता है लेकिन अब स्वार्थवश घरवाले छोटी उम्र की लड़कियों को भी इस घिनौने व्यापार में लगा देतेहैं। इन लड़कियों को "खेलावाड़ी" कहते हैं, जिसका अर्थ है "जिससे खेला जाय"। रीति-रिवाज़ और देवी के नाम पर अनेक लड़कियों का यौन-शोषणहोता है। जवान होते-होते किसी लैंगिक बीमारी के कारण इनका देहान्त हो जाता है। मेहरुन्निसा परवेज़ ने इन लड़कियों की स्थिति को अपनीकहानियों में उजागर किया है जिसका विश्लेषण आगे किया गया है।
"ओढ़ना" कहानी में रानी के माँ-बाप और भाई पैसों के लिए उसे बेच देते हैं। वह एक विवाहित जिन्दगी बिताना चाहती है लेकिन बाप औरभाई उसकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं करने देते क्योंकि वे जानते हैं कि इससे उनके कमाने का जरिया छूट जायेगा। रानी को यह कहकर बहकाते हैं किबचपन से ही उसे देवी को अर्पित करने का वादा किया गया है और अगर उसे निभाया नहीं गया तो देवी का शाप उस पर आने का भय है। वह जबअपने घर में धंधा करने से इनकार करती है तब उसे मामा के हाथों बेच दिया जाता है। रानी इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है लेकिन उसकी बात सुननेके लिए कोई तैयार नहीं होता है। "मैं कोई भैंस हूँ, जो जब जहाँ मर्जी आए बेच दी, कभी चेतन से पैसा खा लिया, अब मामा से पैसे ले रहे हैं और यहींपाँच के दस मामा मुझसे कमाएगा।"32
"खेलावड़ी" कहानी में भी लालमणि भत्तावडी(सुहागिन) बनकर जीना चाहती है। लेकिन उसका मंगेतर शंकर और उसके पिता विवाह सेमुकर जाते हैं। लालमणी के पिता और शंकर के पिता एक-साथ अफीम की तस्करी करते हैं और जब धंधे में शंकर के पिता धोखा देता है तो मंगनीतोड़ दी जाती है। लालमणी के पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लालमणी घर की सारी मर्यादा छोड़कर शंकर के घर पहुँचती है लेकिन शंकरकी बुजदिली के कारण उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है और बाप को पुलिस से बचाने के लिए उसे मामा के घर जाने को तैयार होना पड़ता है।वह रत्लाम से मंदसौर आ जाती है। वक्त और माहोल उसे खेलावड़ी बना देते हैं। बाँछडा समाज में वेश्यावृत्ति परंपरा और देवी के नाम पर हजारोंलड़कियों की जिन्दगी अंधकार से युक्त है। "जूठन" कहानी में ठाकुर तेजासिंह का दबदबा भिंड जिले के गोहद गाँव में है। उसकी दो ब्याही पत्नियाँ तोहैं ही लेकिन जब ग्वालियर के मेले में सिल्ली को देखता है तो अपने धन और वैभव के ज़ोर पर उसे भी ब्याह लाता है। सिल्ली के सारे सपने उजड़ जातेहैं। उससे दुगुनी उम्र के आदमी के साथ ब्याह हो जाता है। ठाकुर की हवेली में जो लड़कियाँ काम पर आती हैं उसे भी वह अपने हवस का शिकारबनाता है। ठाकुर की दिन-ब-दिन चढ़ती जवानी तीनों ठकुराइनों को तो दुखी करती ही है साथ में गाँव की लड़कियाँ भी ठाकुर के कारणसहमी-सहमी-सी रहती हैं। सिल्ली के लिए यह वातावरण बिल्कुल नया था। हवेली की इस हालात को देखकर वह बिल्कुल भयभीत हो जाती है।सुहागरात में ही सिल्ली के साथ ठाकुर तेजासिंह बलात्कार करता है। ठाकुर तेजासिंह के लिए हर औरत एक खिलौना मात्र है। वह अपना धन, वैभवऔर शक्ति का दुरुपयोग करता है। उसकी दहशत की वजह से कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरता है। उच्च वर्ग के पुरुष द्वारा निम्न-वर्गकी स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार का वर्णन "जुगनू" कहानी में किया गया है। तारिक शहर में पढ़ता है। उसके घर की पी डिग्री बावर्ची की बेटी, गुलशनथोड़ी पागल-सी है। जब भी तारिक छुट्टियों पर गाँव आता है, गुलशन को अपने कमरे में बुला भेजता है। जब गुलशन माँ बनने वाली थी तब बात केखुल जाने के डर से पी डिग्री बावर्ची अपने ही हाथों उसे कुएँ में ढकेल कर मार देता है। एक मजबूर, गरीब पिता की मानसिकता को लेखिका ने पाठकोंके समक्ष रखा है। पी डिग्री बावर्ची अपने और अपने जैसे दूसरे गरीबों की मजबूरी पर प्रकाश डालते हैं- "उनकी दी हुई बख्शीशों में से हमारीबहू-बेटियों की इज्जत लेना भी हम लोग अपनी खुशनसीबी और उनका करम मानते आए हैं। हम गरीबों के घर की बहू-बेटियाँ पैदा ही मालिक कोखुश करने, उनकी हवस के लिए ही जन्म लेती हैं।"33 "जगार" कहानी में ननकू, चौधरी की कोठी में नौकर है। जब वह गोमती को ब्याह कर लाता हैतब उसी रात उसका मालिक चौधरी उसे शहर भेज देता है। ननकू की गैरहाज़िरी में गोमती को कोठी पर बुलवाकर वह उसका बलात्कार करता है। सातदिन तक यह सिलसिला जारी रहता है। अपनी बेबसी और लाचारी के कारण गोमती सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। उसकी सास, बुधिया उसकेदुख और पीड़ा को समझती है क्योंकि जब वह ब्याह कर लायी गई थी तब उसे भी बड़े मालिक की हवस की पूर्ति का साधन बनना पड़ा था। पूरे गाँवकी बहुओं के साथ ऐसा होता है। उच्चवर्ग के ये लोग निम्न-वर्ग के पुरुषों का शोषण तो करते ही वे अपने हवस की तृप्ति के लिए स्त्रियों से पशुओंजैसा व्यवहार भी करते हैं। "चुटकी भर समर्पण" कहानी में मनीष अपनी विलासिता के लिए पाखी का उपयोग करता है। पाखी विश्वास, प्यार, अपनत्वऔर सुरक्षा की तलाश में थी। दो-चार मुलाकातों के बाद ही वह मनीष के बच्चे की माँ बनने वाली थी लेकिन मनीष यह जिम्मेदारी लेने से मुकर जाताहै। मनीष की जिद्द के कारण वह बच्चे को गिरवा देती है जिससे पाखी को शारीरिक और मानसिक वेदना से गुजरना पड़ता है। उसकी जिन्दगी में एकखलीपन आ जाता है और वह मनीष से दूर चली जाती है। यहाँ भी पाखी को इस्तेमाल किया जा रहा था।
नारी को निम्न-वर्ग से भी निचली श्रेणी में रखा जाता है। जहाँ निम्न-वर्ग का शोषण सिर्फ उच्च-वर्ग ही करता है वहीं नारी का शोषण उच्चवर्गके साथ-साथ पति, परिवार और समाज के लोग भी करते रहे हैं। वह हर जगह असुरक्षा की गिरफ्त में रहती है।
निष्कर्ष: मेहरुन्निसा परवेज़ ने अपने कहानी साहित्य में, नारी-जीवन में आये अनेक मोडों को, जीवन के यथार्थ पहलुओं से जोड़कर प्रस्तुत करने काप्रयास किया है। अपने कहानी-साहित्य में उन्होंने निम्न-वर्ग, निम्न-मध्य-वर्ग के नारी पात्रों का चयन किया है। नारी के शोषण, बदलते परिवेश के साथउसकी समस्याओं को वाणी दी है।
मेहरुन्निसा परवेज़ ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि शिक्षा के प्रसार के बावजूद भी अनमेल विवाह, दहेज-प्रथा, पर्दा-प्रथा, विधवासमस्या, नारी शोषण आदि से नारी मुक्त नहीं हो पायी है। इसके विरोध में समाज-सुधारकों ने पिछली सदी में ही जंग शु डिग्री कर दिया था लेकिनबदलते परिवेश के साथ समस्याओं ने अपना रूप भी बदल दिया है। नारी को भोग्या समझे जाने की मानसिकता आज पूरे शिद्दत के साथ कायम है।इसलिए नारी के प्रति शोषण घर में ही होता था लेकिन उसका कार्यक्षेत्र के बढ़ने से उसके शोषित होने की संभावनाएँ भी बढ़ गयी हैं। समाज में व्याप्तइन अनाचारों का वर्णन लेखिका ने मर्मस्पर्शी रूप में किया है।
मेहरुन्निसा परवेज़ ने विशेषकर नारी सम्बन्धी विषयों को प्रमुखता दी है। नारी की समस्या एवं शोषण को अपनी कहानियों में उद्घाटित कियाहै। नारी को हर क्षेत्र में अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। यह सिलसिला घर से शु डिग्री होकर मृत्यु तक पीछा करता है। भारतीय परिवारों में आजभी बेटों को प्रधानता दी जाती है जिसका विवरण लेखिका ने अपनी कहानियों में दिया है। दहेज़ जैसे कुप्रथा के कारण बेटी को बोझ समझा जाता है।विवाह के बाद नारी की अनेक समस्याओं को मेहरूजी ने अपनी कहानियों में अंकित किया है। जब नारी माँ बनने में असमर्थ होती है तब उसे मानसिकद्वन्द्व से गुजरना पड़ता है। उसके इस मानसिकता को लेखिका ने अपनी कहानियों में उभारा है। नारी के प्रति रूढ़िगत विचार, अनमेल विवाह से पीढ़ितनारी की व्यथा पर मेहरुन्निसा परवेज़ ने आवाज उठायी है। विधवा नारी, परित्यक्त नारी को समाज एवं परिवार से उपेक्षा मिलती है। नारी को भोग्यासमझने के कारण यौन-शोषण सर्वव्यापी हो गया है। नारी की इस दुर्गति को भी अपनी कहानियों में मेहरुन्निसा परवेज़ ने उजागर किया है।
संदर्भ संकेत:
1. Women : Tradition and Culture - Malladi Subbamma, P.47
2. जमाना बदल गया है (सोने का बेसर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.139
3. सूकी बयड़ी (समर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.111
4. बड़े लोग (धर्मयुग - 13 मार्च 1983), पृ.25
5. जाने कब (सोने का बेसर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.184
6. कयामत आ गई है (ढ़हता कुतुबमीनार-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.38
7. सोने का बेसर (सोने का बेसर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.19
8. आकाशनील (ढ़हता कुतुबमीनार-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.144
9. लौट जाओ बाबूजी(अम्मा-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.35
10. अपने-अपने लोग (अम्मा-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.139
11. अपने होने का एहसास (सोने का बेसर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.40
12. खामोशी की आवाज़ (टहनियों पर धूप-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.85
13. चमडे का खोल(एक और सैलाब-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.59
14. अपने-अपने लोग (अम्मा-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.153
15. आकृतियाँ और दीवारें (धर्मयुग - 2 जनवरी 1972) पृ.18
16. बूँद का हक (अम्मा-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.128
17. सूकी बयड़ी (समर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.143
18. ओढ़ना (सोने का बेसर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.92
19. नंगी आँखोंवाला रेगिस्तान (ढहता कुतुबमीनार-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.56
20. जीवनमंथन (समर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.72
21. बौना मौन(फालगुनी-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.97, 98
22. वीराने (एक और सैलाब-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.82
23. नंगी आँखोंवाला रेगिस्तान (ढहता कुतुबमीनार-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.60
24. प्राण प्रतिष्ठा (अम्मा-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.48
25. जगार (समर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.37
26. अपने-अपने लोग (अम्मा-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.149
27. वही, पृ.150-151
28. अकेला गुलमोहर (अयोध्या से वापसी-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.94
29. United Nations General Assembly, Declaration of elimination of violence against
women. Proceedings of the 85th plenary meeting. Geneva, 20 Dec 1993; reported
in 'Population Report' series L, Number 11, Aug 2000 P.3
30. चुकते नहीं सवाल - मृदुला गर्ग, पृ.42
31. नंगी टहनियाँ (अयोध्या से वापसी-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.134
32. ओढ़ना (सोने का बेसर-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.90
33. जुगनू (अयोध्या से वापसी-कहानी संग्रह) - मेहरुन्निसा परवेज़, पृ.159
_______________
.png)